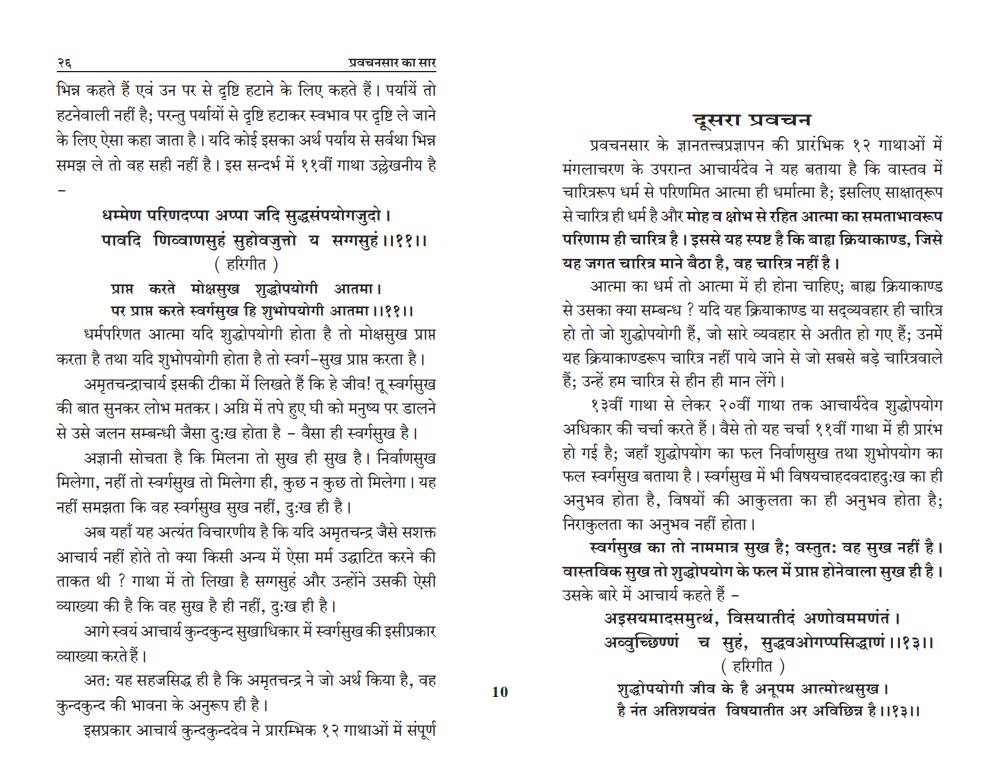________________
प्रवचनसार का सार भिन्न कहते हैं एवं उन पर से दृष्टि हटाने के लिए कहते हैं। पर्यायें तो हटनेवाली नहीं है; परन्तु पर्यायों से दृष्टि हटाकर स्वभाव पर दृष्टि ले जाने के लिए ऐसा कहा जाता है। यदि कोई इसका अर्थ पर्याय से सर्वथा भिन्न समझ ले तो वह सही नहीं है। इस सन्दर्भ में ११वीं गाथा उल्लेखनीय है
धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो। पावदि णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो य सग्गसुहं ।।११।।
(हरिगीत ) प्राप्त करते मोक्षसुख शुद्धोपयोगी आतमा।
पर प्राप्त करते स्वर्गसुख हि शुभोपयोगी आतमा ।।११।। धर्मपरिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगी होता है तो मोक्षसुख प्राप्त करता है तथा यदि शुभोपयोगी होता है तो स्वर्ग-सुख प्राप्त करता है।
अमृतचन्द्राचार्य इसकी टीका में लिखते हैं कि हे जीव! तू स्वर्गसुख की बात सुनकर लोभ मतकर । अग्नि में तपे हुए घी को मनुष्य पर डालने से उसे जलन सम्बन्धी जैसा दुःख होता है - वैसा ही स्वर्गसुख है।
अज्ञानी सोचता है कि मिलना तो सुख ही सुख है। निर्वाणसुख मिलेगा, नहीं तो स्वर्गसुख तो मिलेगा ही, कुछ न कुछ तो मिलेगा। यह नहीं समझता कि वह स्वर्गसुख सुख नहीं, दुःख ही है।
अब यहाँ यह अत्यंत विचारणीय है कि यदि अमृतचन्द्र जैसे सशक्त आचार्य नहीं होते तो क्या किसी अन्य में ऐसा मर्म उद्घाटित करने की ताकत थी ? गाथा में तो लिखा है सग्गसुहं और उन्होंने उसकी ऐसी व्याख्या की है कि वह सुख है ही नहीं, दुःख ही है।
आगे स्वयं आचार्य कुन्दकुन्द सुखाधिकार में स्वर्गसुख की इसीप्रकार व्याख्या करते हैं।
अत: यह सहजसिद्ध ही है कि अमृतचन्द्र ने जो अर्थ किया है, वह कुन्दकुन्द की भावना के अनुरूप ही है।
इसप्रकार आचार्य कुन्दकुन्ददेव ने प्रारम्भिक १२ गाथाओं में संपूर्ण
दूसरा प्रवचन प्रवचनसार के ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापन की प्रारंभिक १२ गाथाओं में मंगलाचरण के उपरान्त आचार्यदेव ने यह बताया है कि वास्तव में चारित्ररूप धर्म से परिणमित आत्मा ही धर्मात्मा है; इसलिए साक्षात्रूप से चारित्र ही धर्म है और मोह व क्षोभ से रहित आत्मा का समताभावरूप परिणाम ही चारित्र है। इससे यह स्पष्ट है कि बाह्य क्रियाकाण्ड, जिसे यह जगत चारित्र माने बैठा है, वह चारित्र नहीं है।
आत्मा का धर्म तो आत्मा में ही होना चाहिए: बाह्य क्रियाकाण्ड से उसका क्या सम्बन्ध ? यदि यह क्रियाकाण्ड या सद्व्यवहार ही चारित्र हो तो जो शुद्धोपयोगी हैं, जो सारे व्यवहार से अतीत हो गए हैं; उनमें यह क्रियाकाण्डरूप चारित्र नहीं पाये जाने से जो सबसे बड़े चारित्रवाले हैं; उन्हें हम चारित्र से हीन ही मान लेंगे।
१३वीं गाथा से लेकर २०वीं गाथा तक आचार्यदेव शुद्धोपयोग अधिकार की चर्चा करते हैं। वैसे तो यह चर्चा ११वीं गाथा में ही प्रारंभ हो गई है; जहाँ शुद्धोपयोग का फल निर्वाणसुख तथा शुभोपयोग का फल स्वर्गसुख बताया है। स्वर्गसुख में भी विषयचाहदवदाहदुःख का ही
अनुभव होता है, विषयों की आकुलता का ही अनुभव होता है; निराकुलता का अनुभव नहीं होता।
स्वर्गसुख का तो नाममात्र सुख है; वस्तुत: वह सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो शुद्धोपयोग के फल में प्राप्त होनेवाला सुख ही है। उसके बारे में आचार्य कहते हैं -
अइसयमादसमुत्थं, विसयातीदं अणोवममणंतं । अव्वुच्छिण्णं च सुहं, सुद्धवओगप्पसिद्धाणं ।।१३।।
(हरिगीत) शुद्धोपयोगी जीव के है अनूपम आत्मोत्थसुख । है नंत अतिशयवंत विषयातीत अर अविछिन्न है।।१३।।