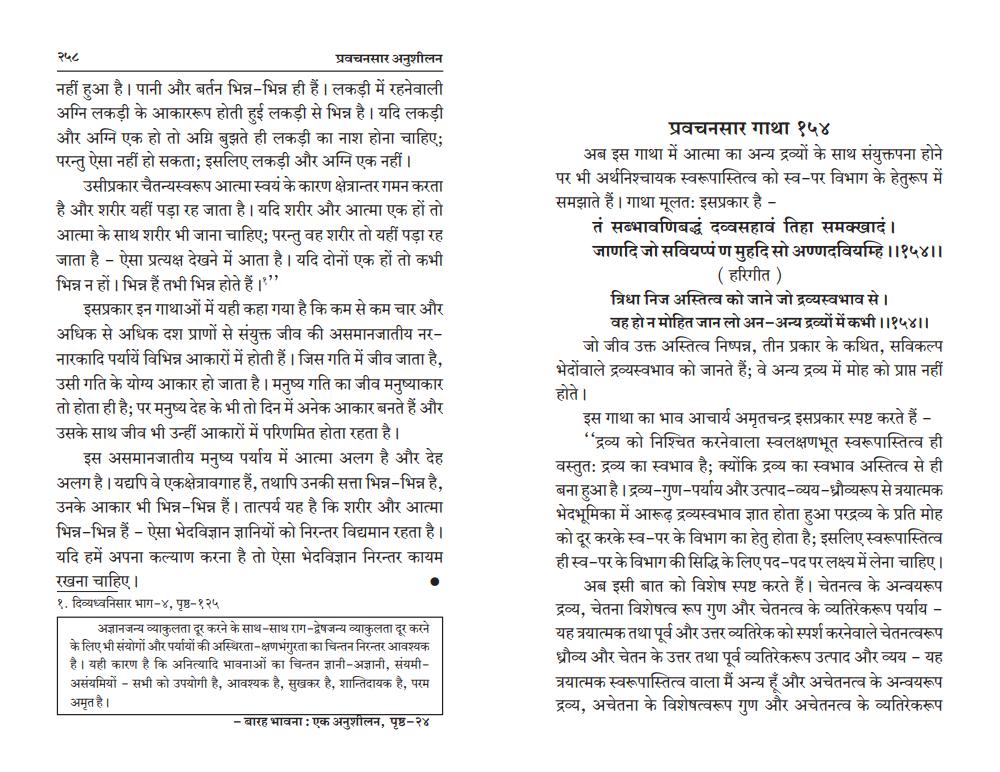________________
ર૬૮
प्रवचनसार अनुशीलन नहीं हुआ है। पानी और बर्तन भिन्न-भिन्न ही हैं। लकड़ी में रहनेवाली अग्नि लकड़ी के आकाररूप होती हुई लकड़ी से भिन्न है। यदि लकड़ी और अग्नि एक हो तो अग्नि बुझते ही लकड़ी का नाश होना चाहिए; परन्तु ऐसा नहीं हो सकता; इसलिए लकड़ी और अग्नि एक नहीं।
उसीप्रकार चैतन्यस्वरूप आत्मा स्वयं के कारण क्षेत्रान्तर गमन करता है और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। यदि शरीर और आत्मा एक हों तो आत्मा के साथ शरीर भी जाना चाहिए; परन्तु वह शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है - ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। यदि दोनों एक हों तो कभी भिन्न न हों। भिन्न हैं तभी भिन्न होते हैं।"
इसप्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि कम से कम चार और अधिक से अधिक दश प्राणों से संयुक्त जीव की असमानजातीय नरनारकादि पर्यायें विभिन्न आकारों में होती हैं। जिस गति में जीव जाता है, उसी गति के योग्य आकार हो जाता है। मनुष्य गति का जीव मनुष्याकार तो होता ही है; पर मनुष्य देह के भी तो दिन में अनेक आकार बनते हैं और उसके साथ जीव भी उन्हीं आकारों में परिणमित होता रहता है।
इस असमानजातीय मनुष्य पर्याय में आत्मा अलग है और देह अलग है। यद्यपि वे एकक्षेत्रावगाह हैं, तथापि उनकी सत्ता भिन्न-भिन्न है, उनके आकार भी भिन्न-भिन्न हैं। तात्पर्य यह है कि शरीर और आत्मा भिन्न-भिन्न हैं - ऐसा भेदविज्ञान ज्ञानियों को निरन्तर विद्यमान रहता है। यदि हमें अपना कल्याण करना है तो ऐसा भेदविज्ञान निरन्तर कायम रखना चाहिए। १. दिव्यध्वनिसार भाग-४, पृष्ठ-१२५
अज्ञानजन्य व्याकुलता दूर करने के साथ-साथ राग-द्वेषजन्य व्याकुलता दूर करने के लिए भी संयोगों और पर्यायों की अस्थिरता-क्षणभंगुरता का चिन्तन निरन्तर आवश्यक है। यही कारण है कि अनित्यादि भावनाओं का चिन्तन ज्ञानी-अज्ञानी, संयमीअसंयमियों - सभी को उपयोगी है, आवश्यक है, सुखकर है, शान्तिदायक है, परम अमृत है।
- बारह भावना : एक अनुशीलन, पृष्ठ-२४
प्रवचनसार गाथा १५४ अब इस गाथा में आत्मा का अन्य द्रव्यों के साथ संयुक्तपना होने पर भी अर्थनिश्चायक स्वरूपास्तित्व को स्व-पर विभाग के हेतुरूप में समझाते हैं। गाथा मूलत: इसप्रकार है -
तं सब्भावणिबद्धं दव्वसहावं तिहा समक्खादं । जाणदिजो सवियप्पंण मुहदि सो अण्णदवियम्हि ।।१५४।।
(हरिगीत ) त्रिधा निज अस्तित्व को जाने जो द्रव्यस्वभाव से।
वह हो न मोहित जान लो अन-अन्य द्रव्यों में कभी ।।१५४।। जो जीव उक्त अस्तित्व निष्पन्न, तीन प्रकार के कथित, सविकल्प भेदोंवाले द्रव्यस्वभाव को जानते हैं; वे अन्य द्रव्य में मोह को प्राप्त नहीं होते।
इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचन्द्र इसप्रकार स्पष्ट करते हैं
"द्रव्य को निश्चित करनेवाला स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्व ही वस्तुतः द्रव्य का स्वभाव है; क्योंकि द्रव्य का स्वभाव अस्तित्व से ही बना हुआ है। द्रव्य-गुण-पर्याय और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप से त्रयात्मक भेदभूमिका में आरूढ़ द्रव्यस्वभाव ज्ञात होता हुआ परद्रव्य के प्रति मोह को दूर करके स्व-पर के विभाग का हेतु होता है; इसलिए स्वरूपास्तित्व ही स्व-पर के विभाग की सिद्धि के लिए पद-पद पर लक्ष्य में लेना चाहिए।
अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। चेतनत्व के अन्वयरूप द्रव्य, चेतना विशेषत्व रूप गुण और चेतनत्व के व्यतिरेकरूप पर्याय - यह त्रयात्मक तथा पूर्व और उत्तर व्यतिरेक को स्पर्श करनेवाले चेतनत्वरूप ध्रौव्य और चेतन के उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूप उत्पाद और व्यय - यह त्रयात्मक स्वरूपास्तित्व वाला मैं अन्य हैं और अचेतनत्व के अन्वयरूप द्रव्य, अचेतना के विशेषत्वरूप गुण और अचेतनत्व के व्यतिरेकरूप