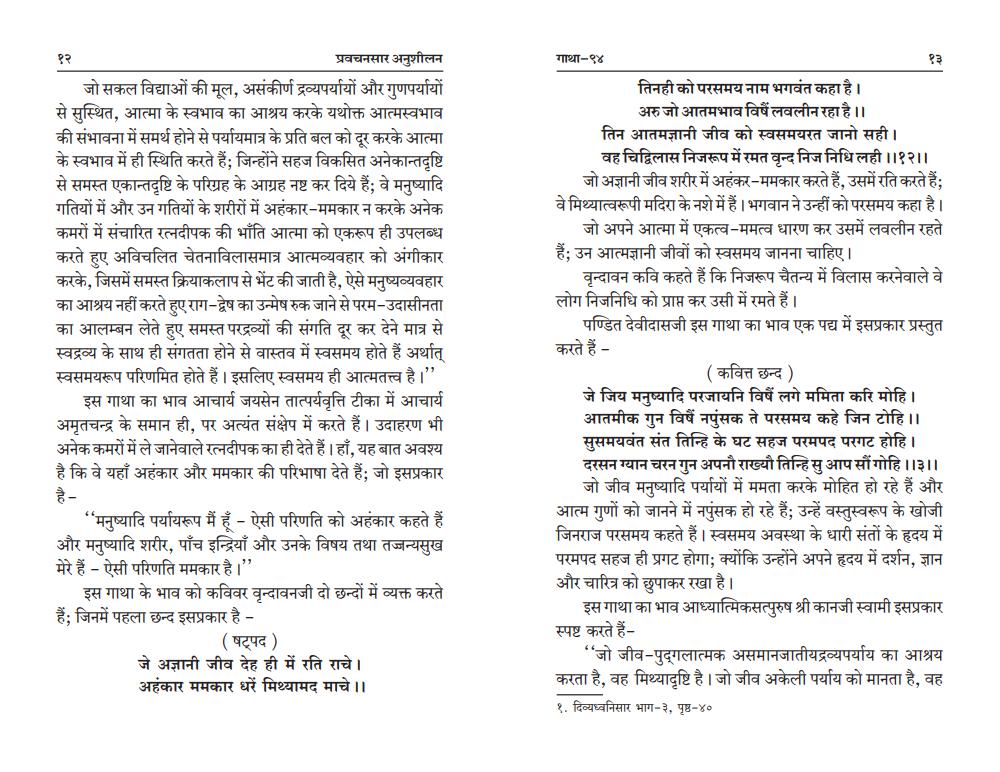________________
प्रवचनसार अनुशीलन
जो सकल विद्याओं की मूल, असंकीर्ण द्रव्यपर्यायों और गुणपर्यायों से सुस्थित, आत्मा के स्वभाव का आश्रय करके यथोक्त आत्मस्वभाव की संभावना में समर्थ होने से पर्यायमात्र के प्रति बल को दूर करके आत्मा के स्वभाव में ही स्थिति करते हैं; जिन्होंने सहज विकसित अनेकान्तदृष्टि से समस्त एकान्तदृष्टि के परिग्रह के आग्रह नष्ट कर दिये हैं; वे मनुष्यादि गतियों में और उन गतियों के शरीरों में अहंकार-ममकार न करके अनेक कमरों में संचारित रत्नदीपक की भाँति आत्मा को एकरूप ही उपलब्ध करते हुए अविचलित चेतनाविलासमात्र आत्मव्यवहार को अंगीकार करके, जिसमें समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है, ऐसे मनुष्यव्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए राग-द्वेष का उन्मेष रुक जाने से परम उदासीनता का आलम्बन लेते हुए समस्त परद्रव्यों की संगति दूर कर देने मात्र से स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से वास्तव में स्वसमय होते हैं अर्थात् स्वसमयरूप परिणमित होते हैं। इसलिए स्वसमय ही आत्मतत्त्व है।"
इस गाथा का भाव आचार्य जयसेन तात्पर्यवृत्ति टीका में आचार्य अमृतचन्द्र के समान ही, पर अत्यंत संक्षेप में करते हैं। उदाहरण भी अनेक कमरों में ले जानेवाले रत्नदीपक का ही देते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि वे यहाँ अहंकार और ममकार की परिभाषा देते हैं; जो इसप्रकार हैं
१२
"मनुष्यादि पर्यायरूप मैं हूँ ऐसी परिणति को अहंकार कहते हैं। और मनुष्यादि शरीर, पाँच इन्द्रियाँ और उनके विषय तथा तज्जन्यसुख मेरे हैं- ऐसी परिणति ममकार है।"
इस गाथा के भाव को कविवर वृन्दावनजी दो छन्दों में व्यक्त करते हैं; जिनमें पहला छन्द इसप्रकार है -
( षट्पद )
जे अज्ञानी जीव देह ही में रति राचे। अहंकार ममकार धरें मिथ्यामद माचे ॥
गाथा - ९४
१३
तिनही को परसमय नाम भगवंत कहा है । अरु जो आतमभाव विषै लवलीन रहा है । तिन आत्मज्ञानी जीव को स्वसमयरत जानो सही ।
वह चिद्विलास निजरूप में रमत वृन्द निज निधि लही ।। १२ ।। जो अज्ञानी जीव शरीर में अहंकर-ममकार करते हैं, उसमें रति करते हैं; वे मिथ्यात्वरूपी मदिरा के नशे में हैं। भगवान ने उन्हीं को परसमय कहा है। जो अपने आत्मा में एकत्व - ममत्व धारण कर उसमें लवलीन रहते हैं; उन आत्मज्ञानी जीवों को स्वसमय जानना चाहिए।
वृन्दावन कवि कहते हैं कि निजरूप चैतन्य में विलास करनेवाले वे लोग निजनिधि को प्राप्त कर उसी में रमते हैं ।
पण्डित देवीदासजी इस गाथा का भाव एक पद्य में इसप्रकार प्रस्तुत करते हैं
( कवित्त छन्द )
जे जिय मनुष्यादि परजायनि विषै लगे ममिता करि मोहि । आतमीक गुन विषै नपुंसक ते परसमय कहे जिन टोहि ।। सुसमयवंत संत तिन्हि के घट सहज परमपद परगट होहि । दरसन ग्यान चरन गुन अपनौ राख्यौ तिन्हि सु आप सौं गोहि । । ३ । । जो जीव मनुष्यादि पर्यायों में ममता करके मोहित हो रहे हैं और आत्म गुणों को जानने में नपुंसक हो रहे हैं; उन्हें वस्तुस्वरूप के खोजी जिनराज परसमय कहते हैं। स्वसमय अवस्था के धारी संतों के हृदय में परमपद सहज ही प्रगट होगा; क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में दर्शन, ज्ञान और चारित्र को छुपाकर रखा है।
इस गाथा का भाव आध्यात्मिकसत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इसप्रकार स्पष्ट करते हैं
"जो जीव- पुद्गलात्मक असमानजातीयद्रव्यपर्याय का आश्रय करता है, वह मिथ्यादृष्टि है। जो जीव अकेली पर्याय को मानता है, वह १. दिव्यध्वनिसार भाग-३, पृष्ठ ४०