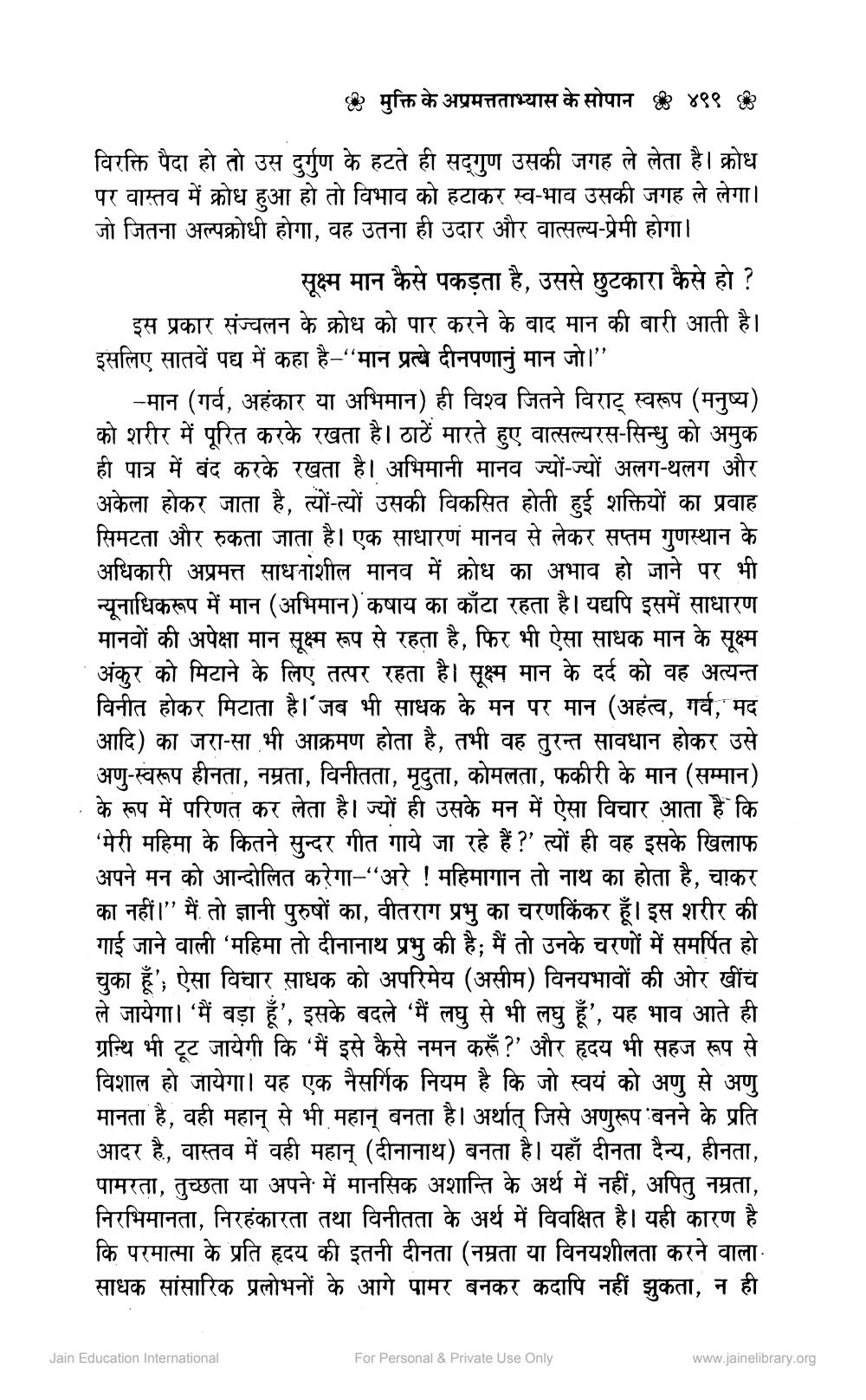________________
* मुक्ति के अप्रमत्तताभ्यास के सोपान ७ ४९९
विरक्ति पैदा हो तो उस दुर्गुण के हटते ही सद्गुण उसकी जगह ले लेता है। क्रोध पर वास्तव में क्रोध हुआ हो तो विभाव को हटाकर स्व-भाव उसकी जगह ले लेगा। जो जितना अल्पक्रोधी होगा, वह उतना ही उदार और वात्सल्य-प्रेमी होगा।
सूक्ष्म मान कैसे पकड़ता है, उससे छुटकारा कैसे हो ? इस प्रकार संज्वलन के क्रोध को पार करने के बाद मान की बारी आती है। इसलिए सातवें पद्य में कहा है-“मान प्रत्ये दीनपणानुं मान जो।" ___-मान (गर्व, अहंकार या अभिमान) ही विश्व जितने विराट स्वरूप (मनुष्य) को शरीर में पूरित करके रखता है। ठाठे मारते हुए वात्सल्यरस-सिन्धु को अमुक ही पात्र में बंद करके रखता है। अभिमानी मानव ज्यों-ज्यों अलग-थलग और अकेला होकर जाता है, त्यों-त्यों उसकी विकसित होती हुई शक्तियों का प्रवाह सिमटता और रुकता जाता है। एक साधारणं मानव से लेकर सप्तम गुणस्थान के अधिकारी अप्रमत्त साधनाशील मानव में क्रोध का अभाव हो जाने पर भी न्यूनाधिकरूप में मान (अभिमान) कषाय का काँटा रहता है। यद्यपि इसमें साधारण मानवों की अपेक्षा मान सूक्ष्म रूप से रहता है, फिर भी ऐसा साधक मान के सूक्ष्म अंकुर को मिटाने के लिए तत्पर रहता है। सूक्ष्म मान के दर्द को वह अत्यन्त विनीत होकर मिटाता है। जब भी साधक के मन पर मान (अहंत्व, गर्व, मद आदि) का जरा-सा भी आक्रमण होता है, तभी वह तुरन्त सावधान होकर उसे अणु-स्वरूप हीनता, नम्रता, विनीतता, मृदुता, कोमलता, फकीरी के मान (सम्मान) के रूप में परिणत कर लेता है। ज्यों ही उसके मन में ऐसा विचार आता है कि 'मेरी महिमा के कितने सुन्दर गीत गाये जा रहे हैं ?' त्यों ही वह इसके खिलाफ अपने मन को आन्दोलित करेगा-“अरे ! महिमागान तो नाथ का होता है, चाकर का नहीं।" मैं तो ज्ञानी पुरुषों का, वीतराग प्रभु का चरणकिंकर हूँ। इस शरीर की गाई जाने वाली 'महिमा तो दीनानाथ प्रभु की है; मैं तो उनके चरणों में समर्पित हो चुका हूँ', ऐसा विचार साधक को अपरिमेय (असीम) विनयभावों की ओर खींच ले जायेगा। 'मैं बड़ा हूँ', इसके बदले 'मैं लघु से भी लघु हूँ', यह भाव आते ही ग्रन्थि भी टूट जायेगी कि 'मैं इसे कैसे नमन करूँ?' और हृदय भी सहज रूप से विशाल हो जायेगा। यह एक नैसर्गिक नियम है कि जो स्वयं को अणु से अणु मानता है, वही महान् से भी महान् बनता है। अर्थात् जिसे अणुरूप बनने के प्रति आदर है, वास्तव में वही महान् (दीनानाथ) बनता है। यहाँ दीनता दैन्य, हीनता, पामरता, तुच्छता या अपने में मानसिक अशान्ति के अर्थ में नहीं, अपितु नम्रता, निरभिमानता, निरहंकारता तथा विनीतता के अर्थ में विवक्षित है। यही कारण है कि परमात्मा के प्रति हृदय की इतनी दीनता (नम्रता या विनयशीलता करने वाला साधक सांसारिक प्रलोभनों के आगे पामर बनकर कदापि नहीं झुकता, न ही
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org