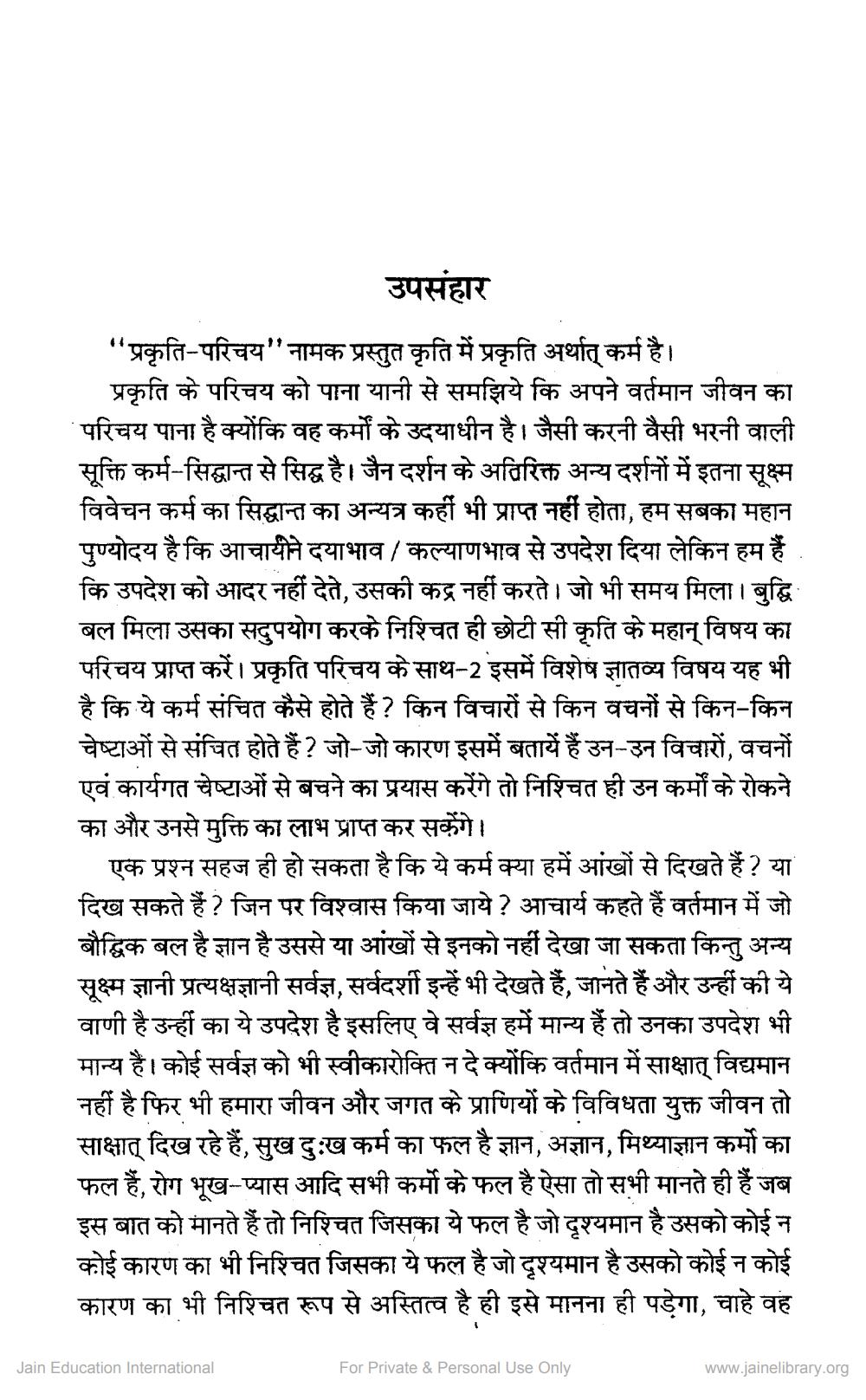Book Title: Prakruti Parichaya Author(s): Vinod Jain, Anil Jain Publisher: Digambar Sahitya Prakashan View full book textPage 9
________________ उपसंहार "प्रकृति-परिचय" नामक प्रस्तुत कृति में प्रकृति अर्थात् कर्म है। प्रकृति के परिचय को पाना यानी से समझिये कि अपने वर्तमान जीवन का परिचय पाना है क्योंकि वह कर्मों के उदयाधीन है। जैसी करनी वैसी भरनी वाली सूक्ति कर्म-सिद्धान्त से सिद्ध है। जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शनों में इतना सूक्ष्म विवेचन कर्म का सिद्धान्त का अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता, हम सबका महान पुण्योदय है कि आचायीने दयाभाव / कल्याणभाव से उपदेश दिया लेकिन हम हैं कि उपदेश को आदर नहीं देते, उसकी कद्र नहीं करते। जो भी समय मिला। बुद्धि बल मिला उसका सदुपयोग करके निश्चित ही छोटी सी कृति के महान् विषय का परिचय प्राप्त करें। प्रकृति परिचय के साथ-2 इसमें विशेष ज्ञातव्य विषय यह भी है कि ये कर्म संचित कैसे होते हैं ? किन विचारों से किन वचनों से किन-किन चेष्टाओं से संचित होते हैं? जो-जो कारण इसमें बतायें हैं उन-उन विचारों, वचनों एवं कार्यगत चेष्टाओं से बचने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही उन कर्मों के रोकने का और उनसे मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ___ एक प्रश्न सहज ही हो सकता है कि ये कर्म क्या हमें आंखों से दिखते हैं? या दिख सकते हैं? जिन पर विश्वास किया जाये? आचार्य कहते हैं वर्तमान में जो बौद्धिक बल है ज्ञान है उससे या आंखों से इनको नहीं देखा जा सकता किन्तु अन्य सूक्ष्म ज्ञानी प्रत्यक्षज्ञानी सर्वज्ञ, सर्वदर्शी इन्हें भी देखते हैं, जानते हैं और उन्हीं की ये वाणी है उन्हीं का ये उपदेश है इसलिए वे सर्वज्ञ हमें मान्य हैं तो उनका उपदेश भी मान्य है। कोई सर्वज्ञ को भी स्वीकारोक्ति न दे क्योंकि वर्तमान में साक्षात् विद्यमान नहीं है फिर भी हमारा जीवन और जगत के प्राणियों के विविधता युक्त जीवन तो साक्षात् दिख रहे हैं, सुख दुःख कर्म का फल है ज्ञान, अज्ञान, मिथ्याज्ञान कर्मो का फल हैं, रोग भूख-प्यास आदि सभी कर्मो के फल है ऐसा तो सभी मानते ही हैं जब इस बात को मानते हैं तो निश्चित जिसका ये फल है जो दृश्यमान है उसको कोई न कोई कारण का भी निश्चित जिसका ये फल है जो दृश्यमान है उसको कोई न कोई कारण का भी निश्चित रूप से अस्तित्व है ही इसे मानना ही पड़ेगा, चाहे वह Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 134