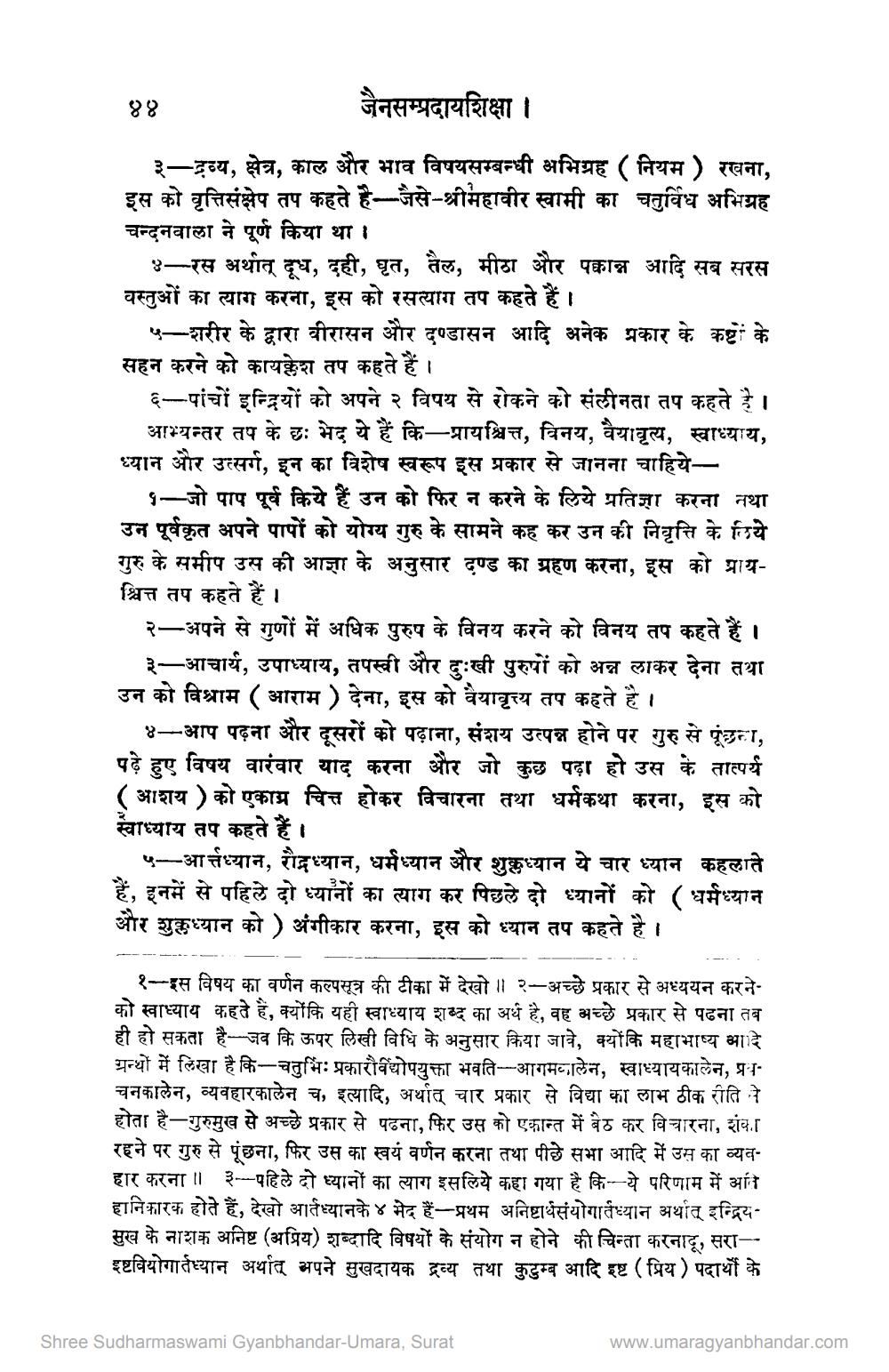________________
जैनसम्प्रदायशिक्षा |
३ – द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव विषयसम्बन्धी अभिग्रह ( नियम ) रखना, इस को वृत्तिसंक्षेप तप कहते है - जैसे- श्रीमहावीर स्वामी का चतुर्विध अभिग्रह चन्दनवाला ने पूर्ण किया था ।
४४
— रस अर्थात् दूध, दही, घृत, तैल, मीठा और पक्वान्न आदि सब सरस वस्तुओं का त्याग करना, इस को रसत्याग तप कहते हैं ।
५ - शरीर के द्वारा वीरासन और दण्डासन आदि अनेक प्रकार के कष्टों के सहन करने को कायक्लेश तप कहते हैं ।
६ - पांचों इन्द्रियों को अपने २ विषय से रोकने को संलीनता तप कहते है । आभ्यन्तर तप के छः भेद ये हैं कि - प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और उत्सर्ग, इन का विशेष स्वरूप इस प्रकार से जानना चाहिये
१ - जो पाप पूर्व किये हैं उन को फिर न करने के लिये प्रतिज्ञा करना तथा उन पूर्वकृत अपने पापों को योग्य गुरु के सामने कह कर उन की निवृत्ति के लिये गुरु के समीप उस की आज्ञा के अनुसार दण्ड का ग्रहण करना, इस को प्रायवित्त तप कहते हैं ।
२- अपने से गुणों में अधिक पुरुष के विनय करने को विनय तप कहते हैं ।
३ – आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी और दुःखी पुरुषों को अन्न लाकर देना तथा उनको विश्राम ( आराम ) देना, इस को वैयावृत्त्य तप कहते है ।
४ - आप पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, संशय उत्पन्न होने पर गुरु से पूंछ, पढ़े हुए विषय वारंवार याद करना और जो कुछ पढ़ा हो उस के तात्पर्य आशय ) को एकाग्र चित्त होकर विचारना तथा धर्मकथा करना, इस को स्वाध्याय तप कहते हैं ।
५- आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान ये चार ध्यान कहलाते हैं, इनमें से पहिले दो ध्यानों का त्याग कर पिछले दो ध्यानों को ( धर्मध्यान और शुकुध्यान को ) अंगीकार करना, इस को ध्यान तप कहते है ।
१ -- इस विषय का वर्णन कल्पसूत्र की टीका में देखो ॥ २- अच्छे प्रकार से अध्ययन करने को स्वाध्याय कहते हैं, क्योंकि यही स्वाध्याय शब्द का अर्थ है, वह अच्छे प्रकार से पढना तब ही हो सकता है-जब कि ऊपर लिखी विधि के अनुसार किया जावे, क्योंकि महाभाष्य आदि ग्रन्थों में लिखा है कि- चतुर्भिः प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति - आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन प्रव चनकालेन, व्यवहारकालेन च, इत्यादि, अर्थात् चार प्रकार से विद्या का लाभ ठीक रीति ने होता है - गुरुमुख से अच्छे प्रकार से पढना, फिर उस को एकान्त में बैठ कर विचारना, शंका रहने पर गुरु से पूंछना, फिर उस का स्वयं वर्णन करना तथा पीछे सभा आदि में उस का व्यव हार करना ॥ ३- पहिले दो ध्यानों का त्याग इसलिये कहा गया है कि- परिणाम में अति हानिकारक होते हैं, देखो आर्तध्यानके ४ भेद हैं- प्रथम अनिष्टार्थसंयोगार्तध्यान अर्थात् इन्द्रियसुख के नाशक अनिष्ट (अप्रिय) शब्दादि विषयों के संयोग न होने की चिन्ता करनादू, सरा-इष्टवियोगार्तध्यान अर्थात् अपने सुखदायक द्रव्य तथा कुटुम्ब आदि इष्ट (प्रिय) पदार्थों के
Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat
www.umaragyanbhandar.com