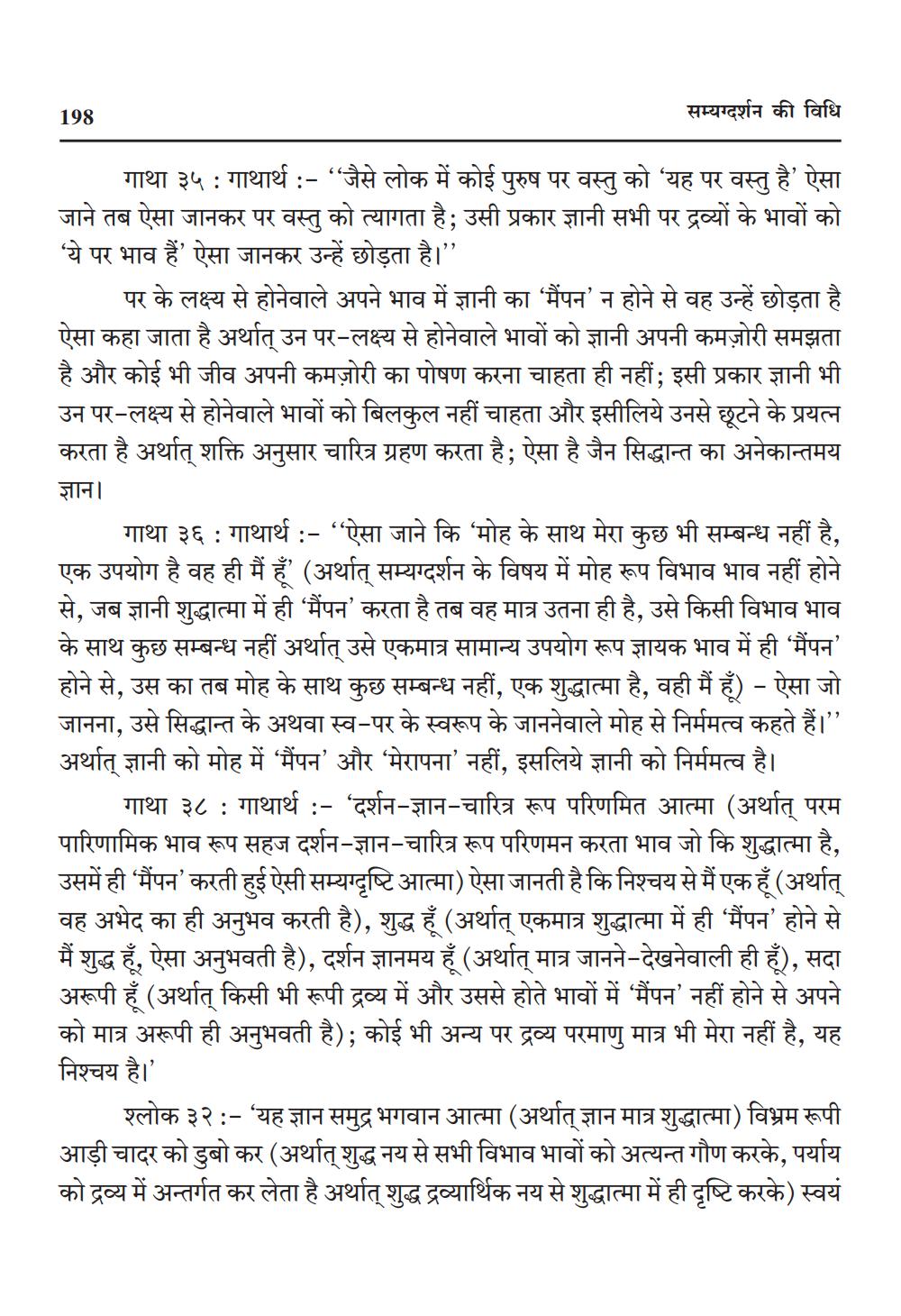________________
198
सम्यग्दर्शन की विधि
गाथा ३५ : गाथार्थ :- "जैसे लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को 'यह पर वस्तु है' ऐसा जाने तब ऐसा जानकर पर वस्तु को त्यागता है; उसी प्रकार ज्ञानी सभी पर द्रव्यों के भावों को 'ये पर भाव हैं' ऐसा जानकर उन्हें छोड़ता है।"
पर के लक्ष्य से होनेवाले अपने भाव में ज्ञानी का 'मैंपन' न होने से वह उन्हें छोड़ता है ऐसा कहा जाता है अर्थात् उन पर-लक्ष्य से होनेवाले भावों को ज्ञानी अपनी कमज़ोरी समझता है और कोई भी जीव अपनी कमज़ोरी का पोषण करना चाहता ही नहीं; इसी प्रकार ज्ञानी भी उन पर-लक्ष्य से होनेवाले भावों को बिलकुल नहीं चाहता और इसीलिये उनसे छूटने के प्रयत्न करता है अर्थात् शक्ति अनुसार चारित्र ग्रहण करता है; ऐसा है जैन सिद्धान्त का अनेकान्तमय ज्ञान।
गाथा ३६ : गाथार्थ :- “ऐसा जाने कि 'मोह के साथ मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, एक उपयोग है वह ही मैं हूँ' (अर्थात् सम्यग्दर्शन के विषय में मोह रूप विभाव भाव नहीं होने से, जब ज्ञानी शुद्धात्मा में ही 'मैंपन' करता है तब वह मात्र उतना ही है, उसे किसी विभाव भाव के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं अर्थात् उसे एकमात्र सामान्य उपयोग रूप ज्ञायक भाव में ही 'मैंपन' होने से, उस का तब मोह के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं, एक शुद्धात्मा है, वही मैं हँ) - ऐसा जो जानना, उसे सिद्धान्त के अथवा स्व-पर के स्वरूप के जाननेवाले मोह से निर्ममत्व कहते हैं।" अर्थात् ज्ञानी को मोह में 'मैंपन' और 'मेरापना' नहीं, इसलिये ज्ञानी को निर्ममत्व है।
___ गाथा ३८ : गाथार्थ :- ‘दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप परिणमित आत्मा (अर्थात् परम पारिणामिक भाव रूप सहज दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप परिणमन करता भाव जो कि शुद्धात्मा है, उसमें ही 'मैंपन' करती हई ऐसी सम्यग्दृष्टि आत्मा) ऐसा जानती है कि निश्चय से मैं एक हँ (अर्थात वह अभेद का ही अनुभव करती है), शुद्ध हूँ (अर्थात् एकमात्र शुद्धात्मा में ही 'मैंपन' होने से मैं शुद्ध हूँ, ऐसा अनुभवती है), दर्शन ज्ञानमय हूँ (अर्थात् मात्र जानने-देखनेवाली ही हूँ), सदा अरूपी हूँ (अर्थात् किसी भी रूपी द्रव्य में और उससे होते भावों में 'मैंपन' नहीं होने से अपने को मात्र अरूपी ही अनुभवती है); कोई भी अन्य पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह निश्चय है।'
__ श्लोक ३२ :- 'यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा (अर्थात् ज्ञान मात्र शुद्धात्मा) विभ्रम रूपी आड़ी चादर को डुबो कर (अर्थात् शुद्ध नय से सभी विभाव भावों को अत्यन्त गौण करके, पर्याय को द्रव्य में अन्तर्गत कर लेता है अर्थात् शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से शुद्धात्मा में ही दृष्टि करके) स्वयं