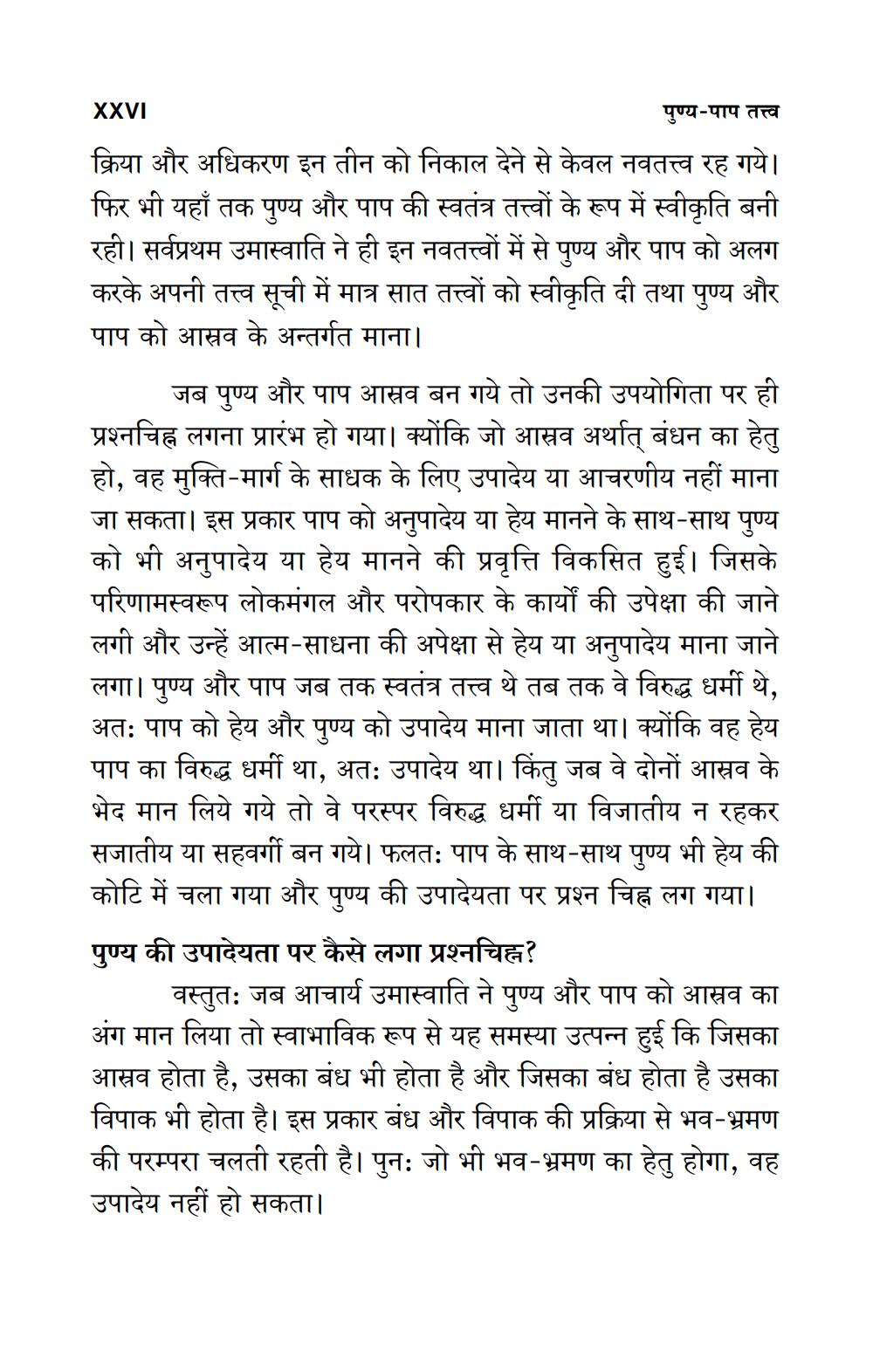________________
XXVI
पुण्य-पाप तत्त्व
क्रिया और अधिकरण इन तीन को निकाल देने से केवल नवतत्त्व रह गये। फिर भी यहाँ तक पुण्य और पाप की स्वतंत्र तत्त्वों के रूप में स्वीकृति बनी रही। सर्वप्रथम उमास्वाति ने ही इन नवतत्त्वों में से पुण्य और पाप को अलग करके अपनी तत्त्व सूची में मात्र सात तत्त्वों को स्वीकृति दी तथा पुण्य और पाप को आस्रव के अन्तर्गत माना।
जब पुण्य और पाप आस्रव बन गये तो उनकी उपयोगिता पर ही प्रश्नचिह्न लगना प्रारंभ हो गया। क्योंकि जो आस्रव अर्थात् बंधन का हेतु हो, वह मुक्ति-मार्ग के साधक के लिए उपादेय या आचरणीय नहीं माना जा सकता। इस प्रकार पाप को अनुपादेय या हेय मानने के साथ-साथ पुण्य को भी अनुपादेय या हेय मानने की प्रवृत्ति विकसित हुई। जिसके परिणामस्वरूप लोकमंगल और परोपकार के कार्यों की उपेक्षा की जाने लगी और उन्हें आत्म-साधना की अपेक्षा से हेय या अनुपादेय माना जाने लगा। पुण्य और पाप जब तक स्वतंत्र तत्त्व थे तब तक वे विरुद्ध धर्मी थे, अतः पाप को हेय और पुण्य को उपादेय माना जाता था। क्योंकि वह हेय पाप का विरुद्ध धर्मी था, अतः उपादेय था। किंतु जब वे दोनों आस्रव के भेद मान लिये गये तो वे परस्पर विरुद्ध धर्मी या विजातीय न रहकर सजातीय या सहवर्गी बन गये। फलतः पाप के साथ-साथ पुण्य भी हेय की कोटि में चला गया और पुण्य की उपादेयता पर प्रश्न चिह्न लग गया। पुण्य की उपादेयता पर कैसे लगा प्रश्नचिह्न?
वस्तुतः जब आचार्य उमास्वाति ने पुण्य और पाप को आस्रव का अंग मान लिया तो स्वाभाविक रूप से यह समस्या उत्पन्न हुई कि जिसका आस्रव होता है, उसका बंध भी होता है और जिसका बंध होता है उसका विपाक भी होता है। इस प्रकार बंध और विपाक की प्रक्रिया से भव-भ्रमण की परम्परा चलती रहती है। पुनः जो भी भव-भ्रमण का हेतु होगा, वह उपादेय नहीं हो सकता।