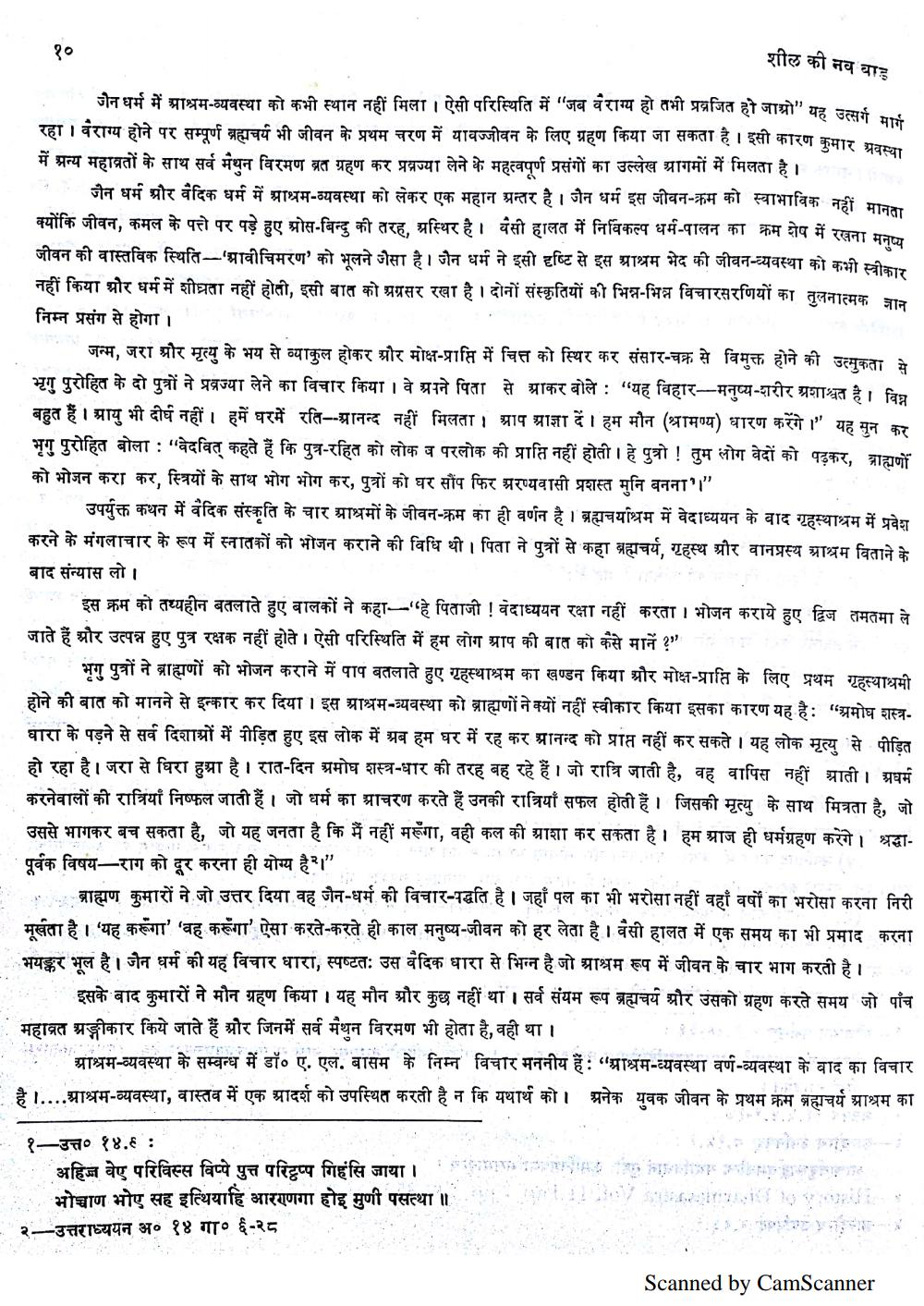________________
१०
शील की नव वाद
. जैन धर्म में पाश्रम-व्यवस्था को कभी स्थान नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में "जब वैराग्य हो तभी प्रवजित हो जायो" या रहा । वैराग्य होने पर सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य भी जीवन के प्रथम चरण में यावज्जीवन के लिए ग्रहण किया जा सकता है । इसी कारण कुमार में अन्य महावतों के साथ सर्व मैथन विरमण ब्रत ग्रहण कर प्रव्रज्या लेने के महत्वपूर्ण प्रसंगों का उल्लेख पागमों में मिलता है।।
जैन धर्म और वैदिक धर्म में प्राथम-व्यवस्था को लेकर एक महान अन्तर है। जैन धर्म इस जीवन-क्रम को स्वाभाविक नहीं पर क्योंकि जीवन, कमल के पत्ते पर पड़े हुए प्रोस-बिन्दु की तरह, अस्थिर है। वैसी हालत में निर्विकल्प धर्म-पालन का क्रम शेष में रखना मना जीवन की वास्तविक स्थिति-'पावीचिमरण' को भूलने जैसा है। जैन धर्म ने इसी दृष्टि से इस आश्रम भेद की जीवन-व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं किया और धर्म में शीघ्रता नहीं होती, इसी बात को अग्रसर रखा है। दोनों संस्कृतियों की भिन्न-भिन्न विचारसरणियों का तुलनात्मक हो निम्न प्रसंग से होगा।
जन्म, जरा और मृत्यु के भय से व्याकुल होकर और मोक्ष-प्राप्ति में चित्त को स्थिर कर संसार-चक्र से विमुक्त होने की उत्सुकता से भृगु पुरोहित के दो पुत्रों ने प्रव्रज्या लेने का विचार किया । वे अपने पिता से आकर बोले : “यह विहार-मनुष्य-शरीर अशाश्वत है। विघ्न बहुत हैं । आयु भी दीर्घ नहीं। हमें घरमें रति--प्रानन्द नहीं मिलता। आप आज्ञा दें। हम मौन (श्रामण्य) धारण करेंगे।" यह सुन कर भग पुरोहित बोला: "वेदवित कहते हैं कि पूत्र-रहित को लोक व परलोक की प्राप्ति नहीं होती। हे पुत्रो ! तुम लोग वेदों को पढकर. बाटा को भोजन करा कर, स्त्रियों के साथ भोग भोग कर, पुत्रों को घर सौंप फिर अरण्यवासी प्रशस्त मुनि बनना'।"
उपर्युक्त कथन में वैदिक संस्कृति के चार आश्रमों के जीवन-क्रम का ही वर्णन है । ब्रह्मचर्याश्रम में वेदाध्ययन के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के मंगलाचार के रूप में स्नातकों को भोजन कराने की विधि थी। पिता ने पुत्रों से कहा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम विताने के। बाद संन्यास लो।
इस क्रम को तथ्यहीन बतलाते हुए बालकों ने कहा-'हे पिताजी ! वेदाध्ययन रक्षा नहीं करता। भोजन कराये हुए द्विज तमतमा ले। जाते हैं और उत्पन्न हुए पुत्र रक्षक नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में हम लोग आप की बात को कैसे मानें ?"
भृगु पुत्रों ने ब्राह्मणों को भोजन कराने में पाप बतलाते हुए गृहस्थाश्रम का खण्डन किया और मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रथम गृहस्थाश्रमी होने की बात को मानने से इन्कार कर दिया। इस आश्रम-व्यवस्था को ब्राह्मणों ने क्यों नहीं स्वीकार किया इसका कारण यह है : "अमोघ शस्त्रधारा के पड़ने से सर्व दिशाओं में पीडित हए इस लोक में अब हम घर में रह कर प्रानन्द को प्राप्त नहीं कर सकते । यह लोक मृत्यु से पीडित हो रहा है। जरा से घिरा हुआ है। रात-दिन अमोघ शस्त्र-धार की तरह बह रहे हैं। जो रात्रि जाती है, वह वापिस नहीं आती। अधर्म करनेवालों की रात्रियां निष्फल जाती हैं। जो धर्म का आचरण करते हैं उनकी रात्रियाँ सफल होती हैं । जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता है, जो उससे भागकर बच सकता है, जो यह जनता है कि मैं नहीं मरूँगा, वही कल की आशा कर सकता है। हम आज ही धर्मग्रहण करेंगे। श्रद्धापूर्वक विषय-राग को दूर करना ही योग्य है।"
ब्राह्मण कुमारों ने जो उत्तर दिया वह जैन-धर्म की विचार-पद्धति है । जहाँ पल का भी भरोसा नहीं वहाँ वर्षों का भरोसा करना निरी मूर्खता है । 'यह करूंगा' 'वह करूंगा' ऐसा करते-करते ही काल मनुष्य-जीवन को हर लेता है । वैसी हालत में एक समय का भी प्रमाद करना भयङ्कर भूल है। जैन धर्म की यह विचार धारा, स्पष्टतः उस वैदिक धारा से भिन्न है जो पाश्रम रूप में जीवन के चार भाग करती है।
इसके बाद कुमारों ने मौन ग्रहण किया। यह मौन और कुछ नहीं था । सर्व संयम रूप ब्रह्मचर्य और उसको ग्रहण करते समय जो पाँच महाव्रत अङ्गीकार किये जाते हैं और जिनमें सर्व मैथुन विरमण भी होता है, वही था।
आश्रम-व्यवस्था के सम्बन्ध में डॉ. ए. एल. बासम के निम्न विचार मननीय हैं : "पाश्रम-व्यवस्था वर्ण-व्यवस्था के बाद का विचार है।....आश्रम-व्यवस्था, वास्तव में एक आदर्श को उपस्थित करती है न कि यथार्थ को। अनेक युवक जीवन के प्रथम क्रम ब्रह्मचर्य आश्रम का
१-उत्त० १४.६ :
अहिज वेए परिविस्स विप्पे पुत्त परिठ्ठप्प गिहंसि जाया।
भोच्चाण भोए सह इत्थियाहि आरएणगा होइ मुणी पसत्था ॥ २-उत्तराध्ययन अ० १४ गा०६-२८
VARTAananesade
S HIY
.
Scanned by CamScanner