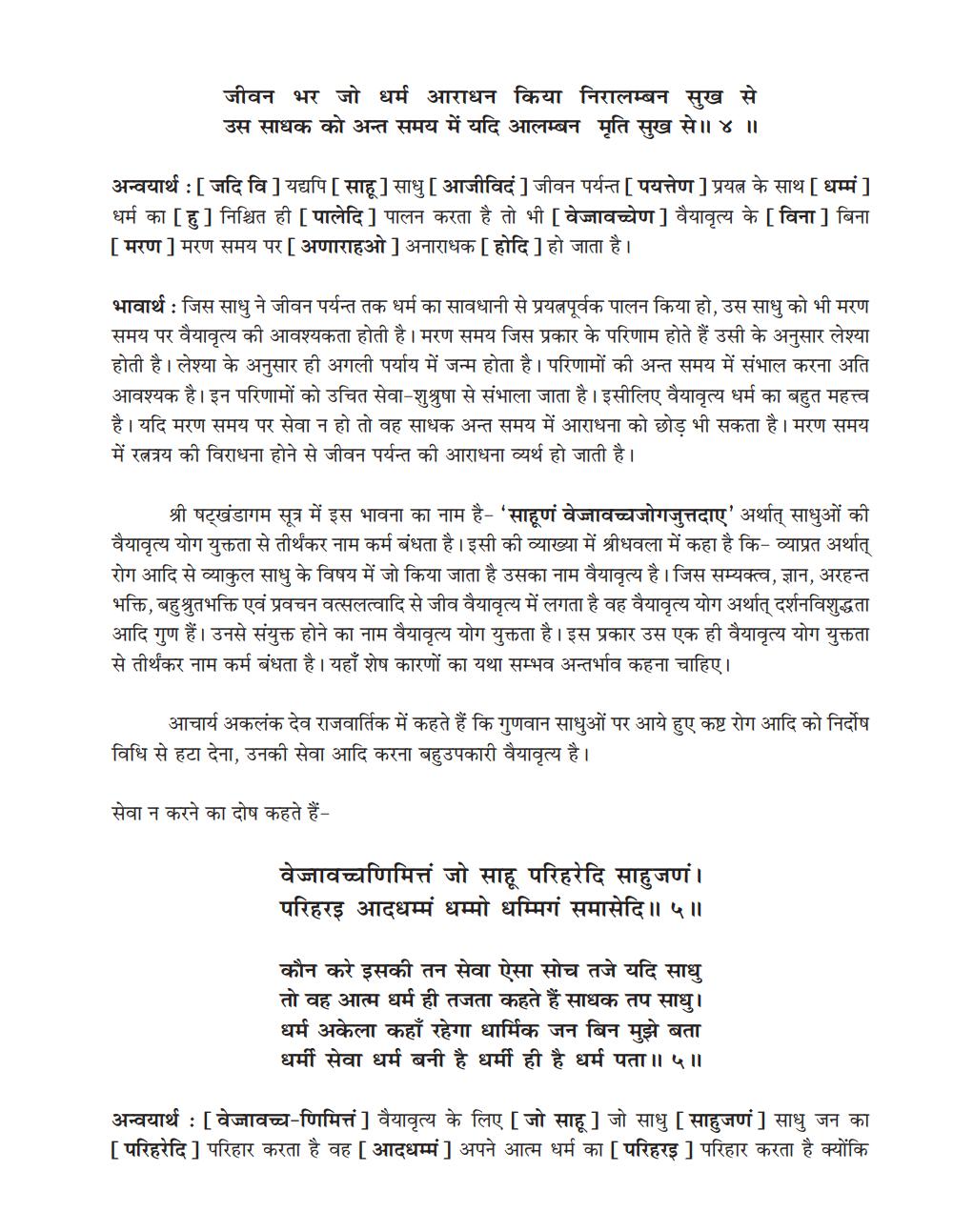________________
जीवन भर जो धर्म आराधन किया निरालम्बन सुख से उस साधक को अन्त समय में यदि आलम्बन मृति सुख से॥ ४ ॥
अन्वयार्थ : [जदि वि] यद्यपि [साहू] साधु [आजीविदं] जीवन पर्यन्त [पयत्तेण] प्रयत्न के साथ [धम्म] धर्म का [हु ] निश्चित ही [ पालेदि ] पालन करता है तो भी [ वेज्जावच्चेण ] वैयावृत्य के [विना ] बिना [मरण] मरण समय पर [अणाराहओ] अनाराधक [होदि] हो जाता है।
भावार्थ : जिस साधु ने जीवन पर्यन्त तक धर्म का सावधानी से प्रयत्नपूर्वक पालन किया हो, उस साधु को भी मरण समय पर वैयावृत्य की आवश्यकता होती है। मरण समय जिस प्रकार के परिणाम होते हैं उसी के अनुसार लेश्या होती है। लेश्या के अनुसार ही अगली पर्याय में जन्म होता है। परिणामों की अन्त समय में संभाल करना अति आवश्यक है। इन परिणामों को उचित सेवा-शुश्रुषा से संभाला जाता है। इसीलिए वैयावृत्य धर्म का बहुत महत्त्व है। यदि मरण समय पर सेवा न हो तो वह साधक अन्त समय में आराधना को छोड़ भी सकता है। मरण समय में रत्नत्रय की विराधना होने से जीवन पर्यन्त की आराधना व्यर्थ हो जाती है।
श्री षट्खंडागम सूत्र में इस भावना का नाम है- 'साहूणं वेजावच्चजोगजुत्तदाए' अर्थात् साधुओं की वैयावृत्य योग युक्तता से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है। इसी की व्याख्या में श्रीधवला में कहा है कि- व्याप्रत अर्थात् रोग आदि से व्याकुल साधु के विषय में जो किया जाता है उसका नाम वैयावृत्य है। जिस सम्यक्त्व, ज्ञान, अरहन्त भक्ति, बहुश्रुतभक्ति एवं प्रवचन वत्सलत्वादि से जीव वैयावृत्य में लगता है वह वैयावृत्य योग अर्थात् दर्शनविशुद्धता आदि गुण हैं। उनसे संयुक्त होने का नाम वैयावृत्य योग युक्तता है। इस प्रकार उस एक ही वैयावृत्य योग युक्तता से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है। यहाँ शेष कारणों का यथा सम्भव अन्तर्भाव कहना चाहिए।
आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में कहते हैं कि गुणवान साधुओं पर आये हुए कष्ट रोग आदि को निर्दोष विधि से हटा देना, उनकी सेवा आदि करना बहुउपकारी वैयावृत्य है।
सेवा न करने का दोष कहते हैं
वेजावच्चणिमित्तं जो साहू परिहरेदि साहुजणं। परिहरइ आदधम्मं धम्मो धम्मिगं समासेदि॥ ५॥
कौन करे इसकी तन सेवा ऐसा सोच तजे यदि साधु तो वह आत्म धर्म ही तजता कहते हैं साधक तप साधु। धर्म अकेला कहाँ रहेगा धार्मिक जन बिन मुझे बता धर्मी सेवा धर्म बनी है धर्मी ही है धर्म पता॥५॥
अन्वयार्थ : [वेज्जावच्च-णिमित्तं] वैयावृत्य के लिए [जो साह] जो साधु [साहजणं] साधु जन का [परिहरेदि] परिहार करता है वह [आदधम्म ] अपने आत्म धर्म का [ परिहरइ ] परिहार करता है क्योंकि