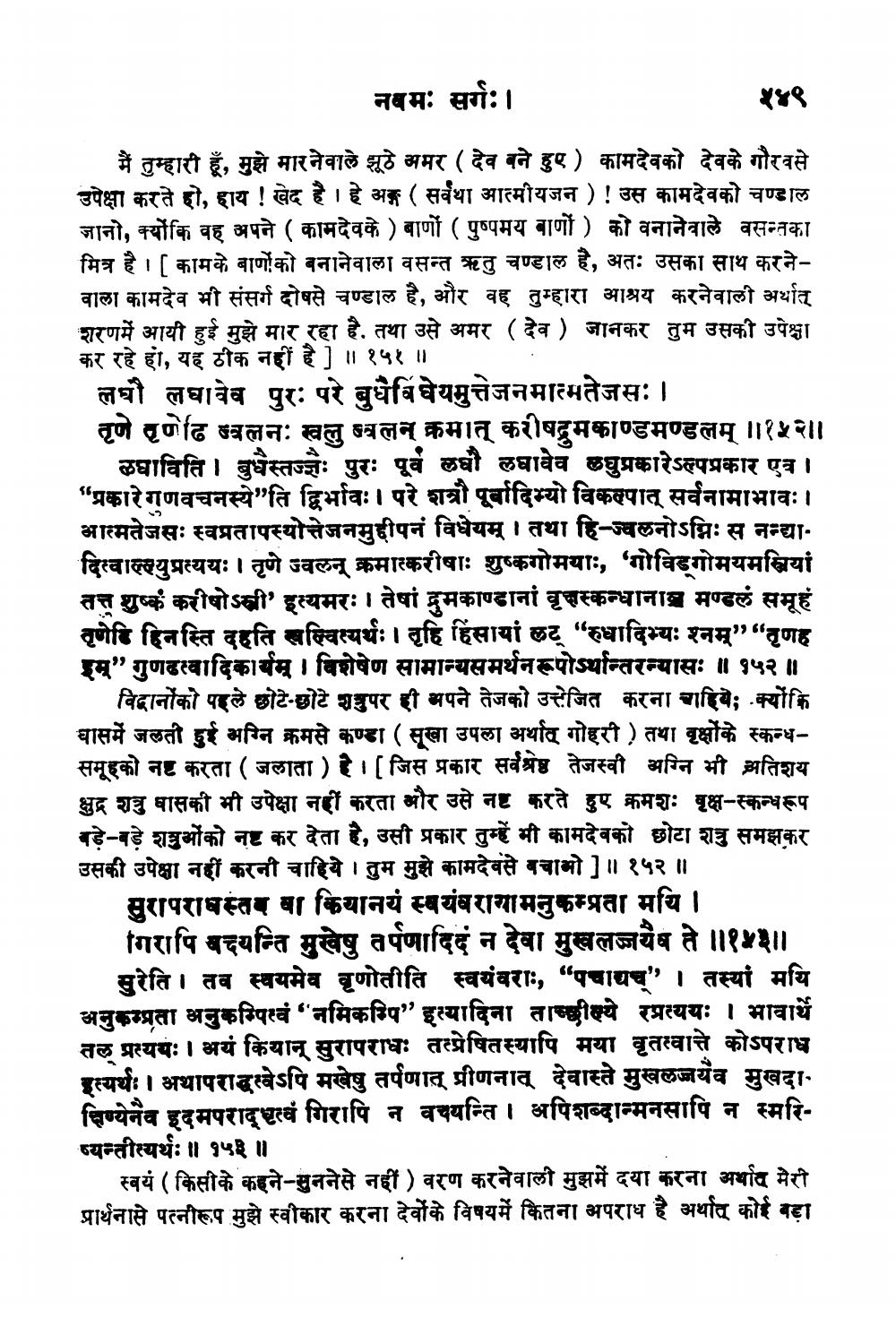________________ नवमः सर्गः। मैं तुम्हारी हूँ, मुझे मारनेवाले झूठे अमर ( देव बने हुए ) कामदेवको देवके गौरवसे उपेक्षा करते हो, हाय ! खेद है / हे अङ्ग ( सर्वथा आत्मीयजन ) ! उस कामदेवको चण्डाल जानो, क्योंकि वह अपने ( कामदेवके ) बाणों ( पुष्पमय बाणों ) को वनानेवाले वसन्तका मित्र है। [ कामके बाणों को बनानेवाला वसन्त ऋतु चण्डाल है, अतः उसका साथ करनेवाला कामदेव भी संसर्ग दोषसे चण्डाल है, और वह तुम्हारा आश्रय करनेवाली अर्थात् शरणमें आयी हुई मुझे मार रहा है. तथा उसे अमर ( देव ) जानकर तुम उसकी उपेक्षा कर रहे हो, यह ठीक नहीं है ] // 15 // लघौ लघावेव पुरः परे बुधैविधेयमुत्तेजनमात्मतेजसः / तृणे तृणेढि ज्वलनः खलु ज्वलन क्रमात् करीषद्मकाण्डमण्डलम् // 152 / / लघाविति / बुधैस्तज्ज्ञः पुरः पूर्व लघी लघावेव लघुप्रकारेऽल्पप्रकार एव / "प्रकारेगणवचनस्ये"ति द्विर्भावः / परे शत्रौ पूर्वादिभ्यो विकल्पात् सर्वनामाभावः। आत्मतेजसः स्वप्रतापस्योत्तेजनमुद्दीपनं विधेयम् / तथा हि-ज्वलनोऽग्निः स नन्द्या. दिवाल्ल्युप्रत्ययः / तृणे ज्वलन् क्रमारकरीषाः शुष्कगोमयाः, 'गोविड्गोमयमस्त्रियां तत्त शुष्कं करीषोऽत्री' इत्यमरः / तेषां दुमकाण्डानां वृक्षस्कन्धानाश मण्डलं समूह तृणेति हिनस्ति दहति खस्वित्यर्थः / तृहि हिंसायां लट् “रुधादिभ्यः श्नम्" "तृणह इम" गुणढत्वादिकार्यम् / विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः // 152 / / विदानोंको पहले छोटे-छोटे शत्रुपर ही अपने तेजको उत्तेजित करना चाहिये। क्योंकि वासमें जलती हुई अग्नि क्रमसे कण्डा (सूखा उपला अर्थात् गोहरी) तथा वृक्षोंके स्कन्धसमूहको नष्ट करता ( जलाता) है। [जिस प्रकार सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी अग्नि भी अतिशय क्षुद्र शत्रु घासकी भी उपेक्षा नहीं करता और उसे नष्ट करते हुए क्रमशः वृक्ष-स्कन्धरूप बड़े-बड़े शत्रुओंको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तुम्हें भी कामदेवको छोटा शत्रु समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये / तुम मुझे कामदेवसे बचामो ] // 152 // सुरापराषस्तव वा कियानयं स्वयंवरायामनुकम्प्रता मयि / गिरापि वक्ष्यन्ति मुखेषु तर्पणादिदं न देवा मुखलजयैष ते // 15 // सुरेति / तव स्वयमेव वृणोतीति स्वयंवराः, “पचायच्" / तस्यां मयि अनुकम्प्रता अनुकम्पित्वं "नमिकम्पि" इत्यादिना ताच्छील्ये रप्रत्ययः / भावार्थे तल प्रत्ययः / अयं कियान् सुरापराधः तत्प्रेषितस्यापि मया वृतत्वात्ते कोऽपराध इत्यर्थः / अथापरास्वेऽपि मखेषु तर्पणात् प्रीणनात् देवास्ते मुखलजयैव मुखदा. क्षिण्येनैव इदमपराद्धवं गिरापि न वचयन्ति / अपिशब्दान्मनसापि न स्मरिप्यन्तीत्यर्थः॥ 153 // ___ स्वयं ( किसीके कहने-सुननेसे नहीं) वरण करनेवाली मुझमें दया करना अर्थात मेरी प्रार्थनासे पत्नीरूप मुझे स्वीकार करना देवों के विषयमें कितना अपराध है अर्थात् कोई बड़ा