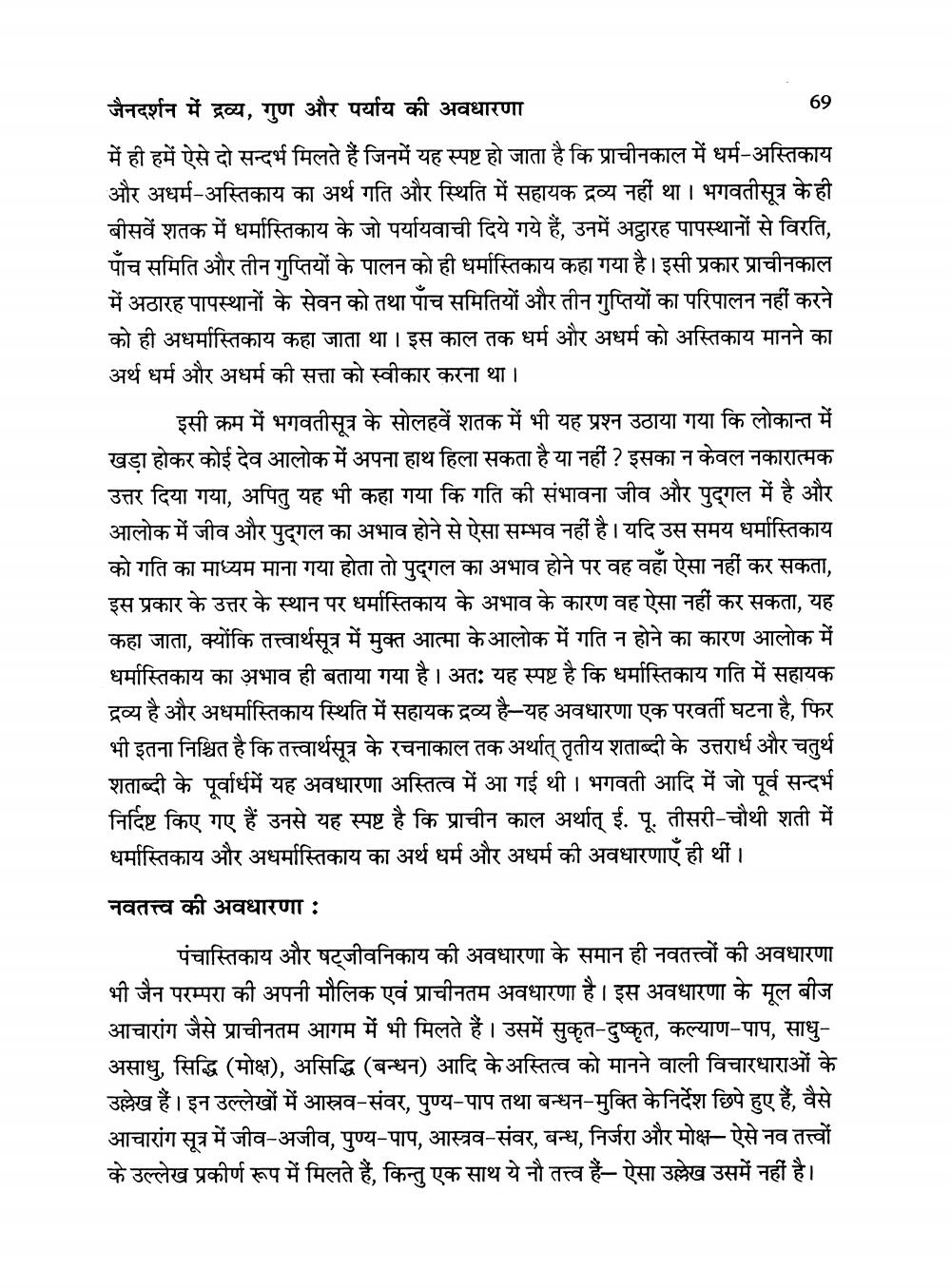________________ जैनदर्शन में द्रव्य, गुण और पर्याय की अवधारणा में ही हमें ऐसे दो सन्दर्भ मिलते हैं जिनमें यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीनकाल में धर्म-अस्तिकाय और अधर्म-अस्तिकाय का अर्थ गति और स्थिति में सहायक द्रव्य नहीं था। भगवतीसूत्र के ही बीसवें शतक में धर्मास्तिकाय के जो पर्यायवाची दिये गये हैं, उनमें अट्ठारह पापस्थानों से विरति, पाँच समिति और तीन गुप्तियों के पालन को ही धर्मास्तिकाय कहा गया है। इसी प्रकार प्राचीनकाल में अठारह पापस्थानों के सेवन को तथा पाँच समितियों और तीन गुप्तियों का परिपालन नहीं करने को ही अधर्मास्तिकाय कहा जाता था। इस काल तक धर्म और अधर्म को अस्तिकाय मानने का अर्थ धर्म और अधर्म की सत्ता को स्वीकार करना था। इसी क्रम में भगवतीसूत्र के सोलहवें शतक में भी यह प्रश्न उठाया गया कि लोकान्त में खड़ा होकर कोई देव आलोक में अपना हाथ हिला सकता है या नहीं ? इसका न केवल नकारात्मक उत्तर दिया गया, अपितु यह भी कहा गया कि गति की संभावना जीव और पुद्गल में है और आलोक में जीव और पुद्गल का अभाव होने से ऐसा सम्भव नहीं है। यदि उस समय धर्मास्तिकाय को गति का माध्यम माना गया होता तो पुद्गल का अभाव होने पर वह वहाँ ऐसा नहीं कर सकता, इस प्रकार के उत्तर के स्थान पर धर्मास्तिकाय के अभाव के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता, यह कहा जाता, क्योंकि तत्त्वार्थसूत्र में मुक्त आत्मा के आलोक में गति न होने का कारण आलोक में धर्मास्तिकाय का अभाव ही बताया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि धर्मास्तिकाय गति में सहायक द्रव्य है और अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक द्रव्य है-यह अवधारणा एक परवर्ती घटना है, फिर भी इतना निश्चित है कि तत्त्वार्थसूत्र के रचनाकाल तक अर्थात् तृतीय शताब्दी के उत्तरार्ध और चतुर्थ शताब्दी के पूर्वार्धमें यह अवधारणा अस्तित्व में आ गई थी। भगवती आदि में जो पूर्व सन्दर्भ निर्दिष्ट किए गए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल अर्थात् ई. पू. तीसरी-चौथी शती में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का अर्थ धर्म और अधर्म की अवधारणाएँ ही थीं। नवतत्त्व की अवधारणा : पंचास्तिकाय और षट्जीवनिकाय की अवधारणा के समान ही नवतत्त्वों की अवधारणा भी जैन परम्परा की अपनी मौलिक एवं प्राचीनतम अवधारणा है। इस अवधारणा के मूल बीज आचारांग जैसे प्राचीनतम आगम में भी मिलते हैं। उसमें सुकृत-दुष्कृत, कल्याण-पाप, साधुअसाधु, सिद्धि (मोक्ष), असिद्धि (बन्धन) आदि के अस्तित्व को मानने वाली विचारधाराओं के उल्लेख हैं। इन उल्लेखों में आस्रव-संवर, पुण्य-पाप तथा बन्धन-मुक्ति केनिर्देश छिपे हुए हैं, वैसे आचारांग सूत्र में जीव-अजीव, पुण्य-पाप, आस्त्रव-संवर, बन्ध, निर्जरा और मोक्ष- ऐसे नव तत्त्वों के उल्लेख प्रकीर्ण रूप में मिलते हैं, किन्तु एक साथ ये नौ तत्त्व हैं- ऐसा उल्लेख उसमें नहीं है।