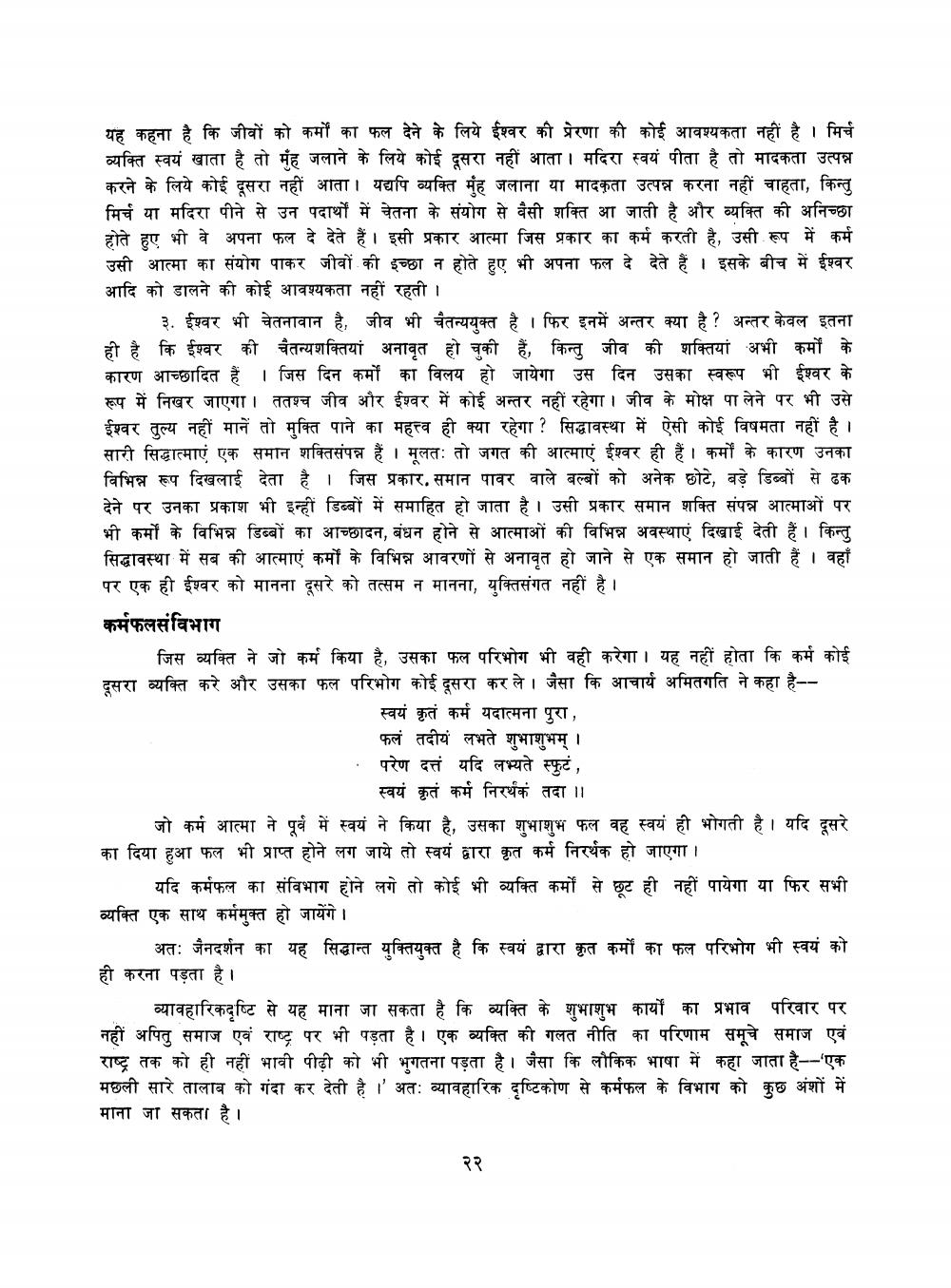________________
यह कहना है कि जीवों को कर्मों का फल देने के लिये ईश्वर की प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं है। मिर्च व्यक्ति स्वयं खाता है तो मुँह जलाने के लिये कोई दूसरा नहीं आता । मदिरा स्वयं पीता है तो मादकता उत्पन्न करने के लिये कोई दूसरा नहीं आता। यद्यपि व्यक्ति मुंह जलाना या मादकता उत्पन्न करना नहीं चाहता, किन्तु मिर्च या मदिरा पीने से उन पदार्थों में चेतना के संयोग से वैसी शक्ति आ जाती है और व्यक्ति की अनिच्छा होते हुए भी वे अपना फल दे देते हैं। इसी प्रकार आत्मा जिस प्रकार का कर्म करती है, उसी रूप में कर्म उसी आत्मा का संयोग पाकर जीवों की इच्छा न होते हुए भी अपना फल दे देते हैं । इसके बीच में ईश्वर आदि को डालने की कोई आवश्यकता नहीं रहती ।
३. ईश्वर भी चेतनावान है, जीव भी चैतन्ययुक्त है । फिर इनमें अन्तर क्या है ? अन्तर केवल इतना ही है कि ईश्वर की चैतन्यशक्तियां अनावृत हो चुकी हैं, किन्तु जीव की शक्तियां अभी कर्मों के कारण आच्छादित हैं । जिस दिन कमों का विलय हो जायेगा उस दिन उसका स्वरूप भी ईश्वर के रूप में निखर जाएगा ततश्च जीव और ईश्वर में कोई अन्तर नहीं रहेगा। जीव के मोक्ष पा लेने पर भी उसे
ईश्वर तुल्य नहीं मानें तो मुक्ति पाने का महत्त्व ही क्या रहेगा ? सिद्धावस्था में ऐसी कोई विषमता नहीं है । सारी सिद्धात्माएं एक समान शक्तिसंपन्न हैं। मूलतः तो जगत की आत्माएं ईश्वर ही हैं। कर्मों के कारण उनका विभिन्न रूप दिखलाई देता है। जिस प्रकार, समान पावर वाले बल्बों को अनेक छोटे बड़े डिब्बों से क देने पर उनका प्रकाण भी इन्हीं डिब्बों में समाहित हो जाता है। उसी प्रकार समान शक्ति संपन्न आत्माओं पर भी कर्मों के विभिन्न डिब्बों का आच्छादन, बंधन होने से आत्माओं की विभिन्न अवस्थाएं दिखाई देती हैं । किन्तु सिद्धावस्था में सब की आत्माएं कर्मों के विभिन्न आवरणों से अनावृत हो जाने से एक समान हो जाती हैं । वहाँ पर एक ही ईश्वर को मानना दूसरे को तत्सम न मानना, युक्तिसंगत नहीं है।
कर्मफलसंविभाग
जिस व्यक्ति ने जो कर्म किया है, उसका फल परिभोग भी वही करेगा। यह नहीं होता कि कर्म कोई दूसरा व्यक्ति करे और उसका फल परिभोग कोई दूसरा कर ले। जैसा कि आचार्य अमितगति ने कहा है-
1
स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् । परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ।।
जो कर्म आत्मा ने पूर्व में स्वयं ने किया है, उसका शुभाशुभ फल वह स्वयं ही भोगती है । यदि दूसरे का दिया हुआ फल भी प्राप्त होने लग जाये तो स्वयं द्वारा कृत कर्म निरर्थक हो जाएगा ।
यदि कर्मफल का संविभाग होने लगे तो कोई भी व्यक्ति कर्मों से छूट ही नहीं पायेगा या फिर सभी व्यक्ति एक साथ कर्ममुक्त हो जायेंगे।
अत: जैनदर्शन का यह सिद्धान्त युक्तियुक्त है कि स्वयं द्वारा कृत कमों का फल परिभोग भी स्वयं को ही करना पड़ता है ।
व्यावहारिकदृष्टि से यह माना जा सकता है कि व्यक्ति के शुभाशुभ कार्यों का प्रभाव परिवार पर नहीं अपितु समाज एवं राष्ट्र पर भी पड़ता है। एक व्यक्ति की गलत नीति का परिणाम समूचे समाज एवं राष्ट्र तक को ही नहीं भावी पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता है। जैसा कि लौकिक भाषा में कहा जाता है— एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ।' अतः व्यावहारिक दृष्टिकोण से कर्मफल के विभाग को कुछ अंशों में माना जा सकता है ।
२२