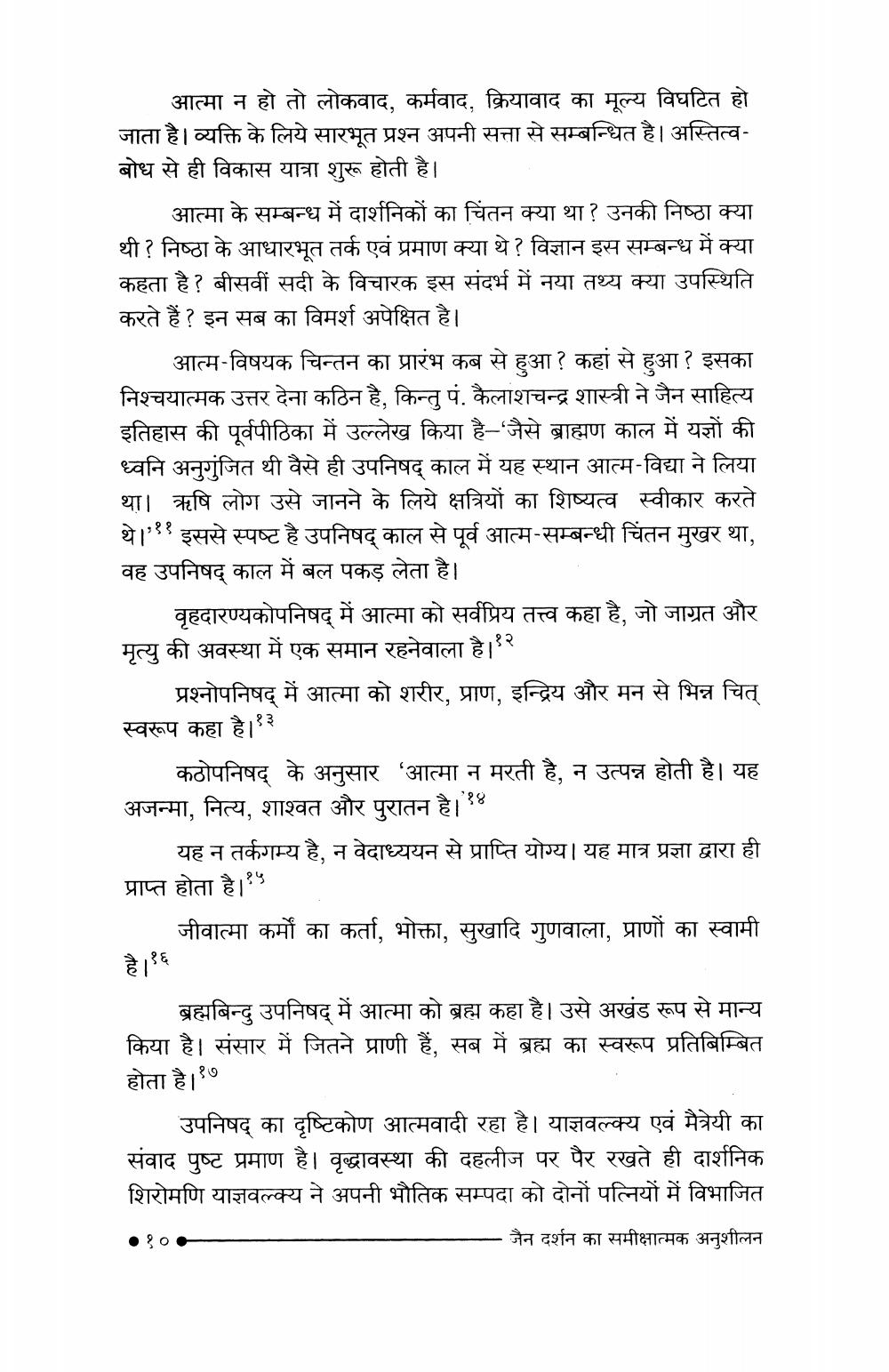________________
आत्मा न हो तो लोकवाद, कर्मवाद, क्रियावाद का मूल्य विघटित हो ता है। व्यक्ति के लिये सारभूत प्रश्न अपनी सत्ता से सम्बन्धित है। अस्तित्वबोध से ही विकास यात्रा शुरू होती है।
आत्मा के सम्बन्ध में दार्शनिकों का चिंतन क्या था ? उनकी निष्ठा क्या थी? निष्ठा के आधारभूत तर्क एवं प्रमाण क्या थे ? विज्ञान इस सम्बन्ध में क्या कहता है ? बीसवीं सदी के विचारक इस संदर्भ में नया तथ्य क्या उपस्थिति करते हैं ? इन सब का विमर्श अपेक्षित है।
आत्म-विषयक चिन्तन का प्रारंभ कब से हुआ ? कहां से हुआ? इसका निश्चयात्मक उत्तर देना कठिन है, किन्तु पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री ने जैन साहित्य इतिहास की पूर्वपीठिका में उल्लेख किया है- 'जैसे ब्राह्मण काल में यज्ञों की ध्वनि अनुगुंजित थी वैसे ही उपनिषद् काल में यह स्थान आत्म-विद्या ने लिया था। ऋषि लोग उसे जानने के लिये क्षत्रियों का शिष्यत्व स्वीकार करते थे।”” इससे स्पष्ट है उपनिषद् काल से पूर्व आत्म-सम्बन्धी चिंतन मुखर था, वह उपनिषद् काल में बल पकड़ लेता है।
वृहदारण्यकोपनिषद् में आत्मा को सर्वप्रिय तत्त्व कहा है, जो जाग्रत और मृत्यु की अवस्था में एक समान रहनेवाला है । १२
प्रश्नोपनिषद् में आत्मा को शरीर, प्राण, इन्द्रिय और मन से भिन्न चित् स्वरूप कहा है । १३
कठोपनिषद् के अनुसार 'आत्मा न मरती है, न उत्पन्न होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है ।"
१४
यह न तर्कगम्य है, न वेदाध्ययन से प्राप्ति योग्य । यह मात्र प्रज्ञा द्वारा ही प्राप्त होता है । १५
जीवात्मा कर्मों का कर्ता, भोक्ता, सुखादि गुणवाला, प्राणों का स्वामी
है । १६
ब्रह्मबिन्दु उपनिषद् में आत्मा को ब्रह्म कहा है। उसे अखंड रूप से मान्य किया है। संसार में जितने प्राणी हैं, सब में ब्रह्म का स्वरूप प्रतिबिम्बित होता है।
उपनिषद् का दृष्टिकोण आत्मवादी रहा है। याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी का संवाद पुष्ट प्रमाण है । वृद्धावस्था की दहलीज पर पैर रखते ही दार्शनिक शिरोमणि याज्ञवल्क्य ने अपनी भौतिक सम्पदा को दोनों पत्नियों में विभाजित
१०
जैन दर्शन का समीक्षात्मक अनुशीलन