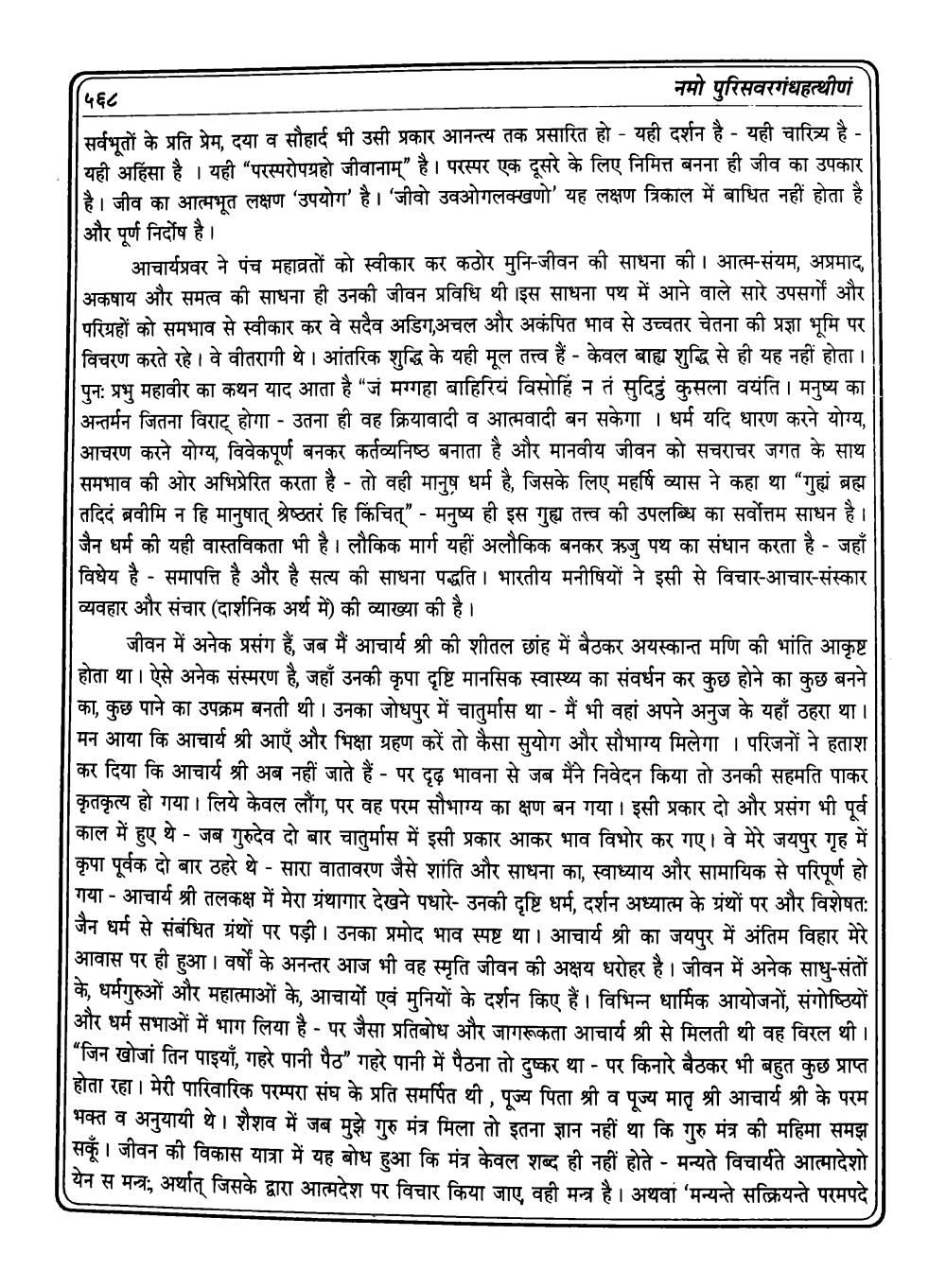________________
नमो पुरिसवरगंधहत्थीणं ५६८ सर्वभूतों के प्रति प्रेम, दया व सौहार्द भी उसी प्रकार आनन्त्य तक प्रसारित हो - यही दर्शन है - यही चारित्र्य है - यही अहिंसा है । यही “परस्परोपग्रहो जीवानाम्” है। परस्पर एक दूसरे के लिए निमित्त बनना ही जीव का उपकार है। जीव का आत्मभूत लक्षण 'उपयोग' है। 'जीवो उवओगलक्खणो' यह लक्षण त्रिकाल में बाधित नहीं होता है और पूर्ण निर्दोष है।
आचार्यप्रवर ने पंच महाव्रतों को स्वीकार कर कठोर मुनि-जीवन की साधना की। आत्म-संयम, अप्रमाद, अकषाय और समत्व की साधना ही उनकी जीवन प्रविधि थी ।इस साधना पथ में आने वाले सारे उपसर्गों और परिग्रहों को समभाव से स्वीकार कर वे सदैव अडिग,अचल और अकंपित भाव से उच्चतर चेतना की प्रज्ञा भूमि पर विचरण करते रहे। वे वीतरागी थे। आंतरिक शुद्धि के यही मूल तत्त्व हैं - केवल बाह्य शुद्धि से ही यह नहीं होता।। पुन: प्रभु महावीर का कथन याद आता है "जं मग्गहा बाहिरियं विसोहिं न तं सुदिटुं कुसला वयंति । मनुष्य का अन्तर्मन जितना विराट् होगा - उतना ही वह क्रियावादी व आत्मवादी बन सकेगा । धर्म यदि धारण करने योग्य, आचरण करने योग्य, विवेकपूर्ण बनकर कर्तव्यनिष्ठ बनाता है और मानवीय जीवन को सचराचर जगत के साथ समभाव की ओर अभिप्रेरित करता है - तो वही मानुष धर्म है, जिसके लिए महर्षि व्यास ने कहा था “गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्” - मनुष्य ही इस गुह्य तत्त्व की उपलब्धि का सर्वोत्तम साधन है। जैन धर्म की यही वास्तविकता भी है। लौकिक मार्ग यहीं अलौकिक बनकर ऋजु पथ का संधान करता है - जहाँ विधेय है - समापत्ति है और है सत्य की साधना पद्धति । भारतीय मनीषियों ने इसी से विचार-आचार-संस्कार व्यवहार और संचार (दार्शनिक अर्थ में) की व्याख्या की है।
जीवन में अनेक प्रसंग हैं, जब मैं आचार्य श्री की शीतल छांह में बैठकर अयस्कान्त मणि की भांति आकृष्ट होता था। ऐसे अनेक संस्मरण है, जहाँ उनकी कृपा दृष्टि मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन कर कुछ होने का कुछ बनने का, कुछ पाने का उपक्रम बनती थी। उनका जोधपुर में चातुर्मास था - मैं भी वहां अपने अनुज के यहाँ ठहरा था। मन आया कि आचार्य श्री आएँ और भिक्षा ग्रहण करें तो कैसा सुयोग और सौभाग्य मिलेगा । परिजनों ने हताश कर दिया कि आचार्य श्री अब नहीं जाते हैं - पर दृढ़ भावना से जब मैंने निवेदन किया तो उनकी सहमति पाकर कृतकृत्य हो गया। लिये केवल लौंग, पर वह परम सौभाग्य का क्षण बन गया। इसी प्रकार दो और प्रसंग भी पूर्व काल में हुए थे - जब गुरुदेव दो बार चातुर्मास में इसी प्रकार आकर भाव विभोर कर गए। वे मेरे जयपुर गृह में कृपा पूर्वक दो बार ठहरे थे - सारा वातावरण जैसे शांति और साधना का, स्वाध्याय और सामायिक से परिपूर्ण हो गया - आचार्य श्री तलकक्ष में मेरा ग्रंथागार देखने पधारे- उनकी दृष्टि धर्म, दर्शन अध्यात्म के ग्रंथों पर और विशेषत: जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों पर पड़ी। उनका प्रमोद भाव स्पष्ट था। आचार्य श्री का जयपुर में अंतिम विहार मेरे आवास पर ही हुआ। वर्षों के अनन्तर आज भी वह स्मृति जीवन की अक्षय धरोहर है। जीवन में अनेक साधु-संतों के, धर्मगुरुओं और महात्माओं के, आचार्यों एवं मुनियों के दर्शन किए हैं। विभिन्न धार्मिक आयोजनों, संगोष्ठियों
और धर्म सभाओं में भाग लिया है - पर जैसा प्रतिबोध और जागरूकता आचार्य श्री से मिलती थी वह विरल थी। "जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ” गहरे पानी में पैठना तो दष्कर था - पर किनारे बैठकर भी बहुत कुछ प्राप्त होता रहा। मेरी पारिवारिक परम्परा संघ के प्रति समर्पित थी , पूज्य पिता श्री व पूज्य मातृ श्री आचार्य श्री के परम भक्त व अनुयायी थे। शैशव में जब मुझे गुरु मंत्र मिला तो इतना ज्ञान नहीं था कि गुरु मंत्र की महिमा समझ सकू। जीवन की विकास यात्रा में यह बोध हुआ कि मंत्र केवल शब्द ही नहीं होते - मन्यते विचार्यते आत्मादेशो येन स मन्त्र; अर्थात् जिसके द्वारा आत्मदेश पर विचार किया जाए, वही मन्त्र है। अथवा 'मन्यन्ते सक्रियन्ते परमपदे