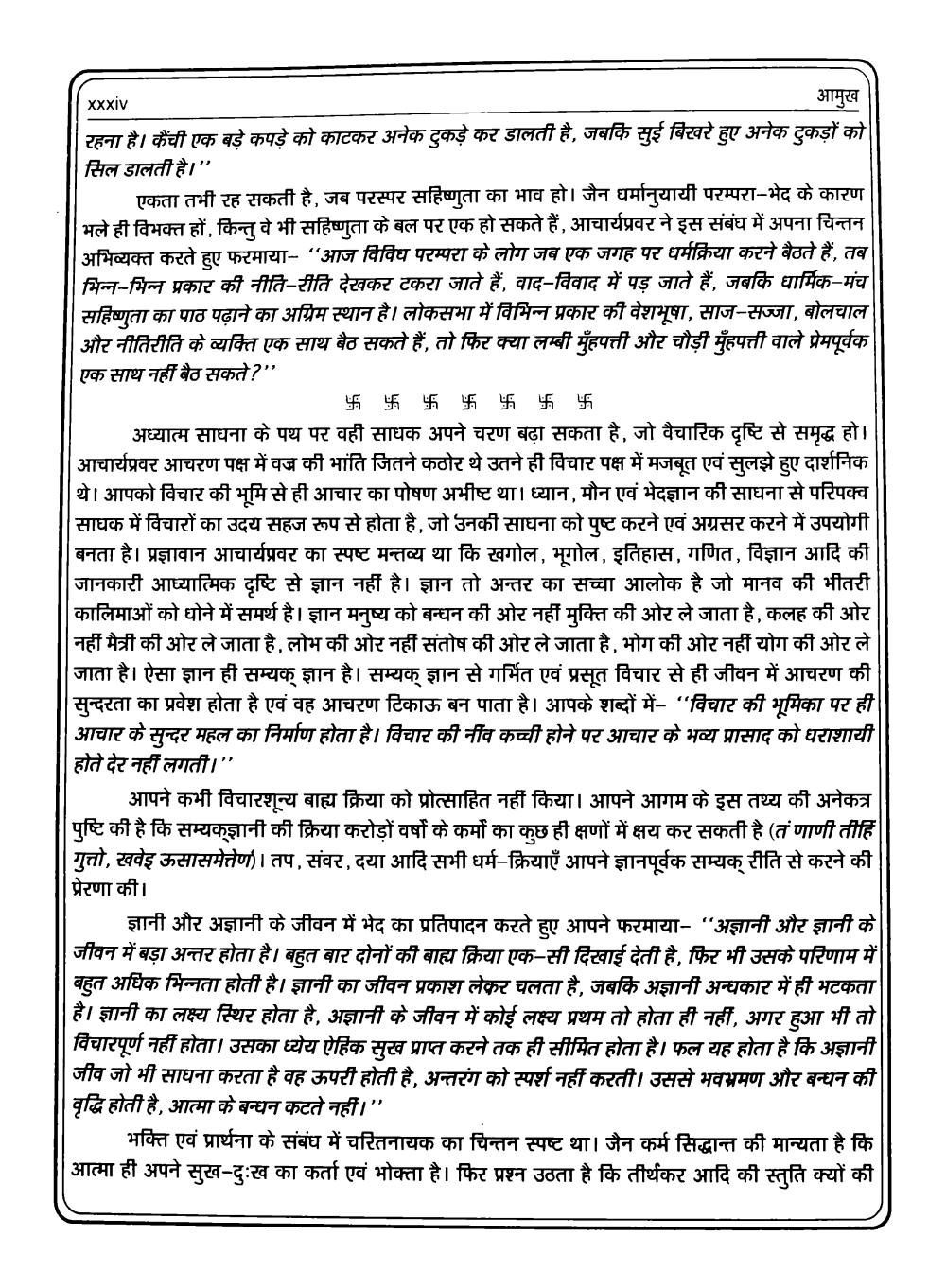________________
xxxiv
आमुख रहना है। कैंची एक बड़े कपड़े को काटकर अनेक टुकड़े कर डालती है, जबकि सुई बिखरे हुए अनेक टुकड़ों को सिल डालती है।"
एकता तभी रह सकती है, जब परस्पर सहिष्णुता का भाव हो। जैन धर्मानुयायी परम्परा-भेद के कारण भले ही विभक्त हों, किन्त वे भी सहिष्णता के बल पर एक हो सकते हैं, आचार्यप्रवर ने इस संबंध में अपना चिन्तन अभिव्यक्त करते हुए फरमाया- “आज विविध परम्परा के लोग जब एक जगह पर धर्मक्रिया करने बैठते हैं, तब भिन्न-भिन्न प्रकार की नीति-रीति देखकर टकरा जाते हैं, वाद-विवाद में पड़ जाते हैं, जबकि धार्मिक-मंच सहिष्णता का पाठ पढ़ाने का अग्रिम स्थान है। लोकसभा में विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, साज-सज्जा, बोलचाल और नीतिरीति के व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं, तो फिर क्या लम्बी मुँहपत्ती और चौड़ी मुँहपत्ती वाले प्रेमपूर्वक एक साथ नहीं बैठ सकते?"
__ अध्यात्म साधना के पथ पर वहीं साधक अपने चरण बढ़ा सकता है, जो वैचारिक दृष्टि से समृद्ध हो। आचार्यप्रवर आचरण पक्ष में वज की भांति जितने कठोर थे उतने ही विचार पक्ष में मजबूत एवं सुलझे हुए दार्शनिक थे। आपको विचार की भूमि से ही आचार का पोषण अभीष्ट था। ध्यान, मौन एवं भेदज्ञान की साधना से परिपक्व साधक में विचारों का उदय सहज रूप से होता है, जो उनकी साधना को पुष्ट करने एवं अग्रसर करने में उपयोगी बनता है। प्रज्ञावान आचार्यप्रवर का स्पष्ट मन्तव्य था कि खगोल, भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान आदि की जानकारी आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो अन्तर का सच्चा आलोक है जो मानव की भीतरी कालिमाओं को धोने में समर्थ है। ज्ञान मनुष्य को बन्धन की ओर नहीं मुक्ति की ओर ले जाता है, कलह की ओर नहीं मैत्री की ओर ले जाता है.लोभ की ओर नहीं संतोष की ओर ले जाता है, भोग की ओर नहीं योग की ओर ले जाता है। ऐसा ज्ञान ही सम्यक् ज्ञान है। सम्यक् ज्ञान से गर्मित एवं प्रसूत विचार से ही जीवन में आचरण की सुन्दरता का प्रवेश होता है एवं वह आचरण टिकाऊ बन पाता है। आपके शब्दों में- "विचार की भूमिका पर ही आचार के सुन्दर महल का निर्माण होता है। विचार की नींव कच्ची होने पर आचार के भव्य प्रासाद को धराशायी होते देर नहीं लगती।"
आपने कभी विचारशून्य बाह्य क्रिया को प्रोत्साहित नहीं किया। आपने आगम के इस तथ्य की अनेकत्र | पुष्टि की है कि सम्यक्ज्ञानी की क्रिया करोड़ों वर्षों के कर्मों का कुछ ही क्षणों में क्षय कर सकती है (तंणाणी तीहि
गुत्तो, खवेइ ऊसासमेत्ते)। तप, संवर, दया आदि सभी धर्म-क्रियाएँ आपने ज्ञानपूर्वक सम्यक् रीति से करने की प्रेरणा की।
ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में भेद का प्रतिपादन करते हुए आपने फरमाया- "अज्ञानी और ज्ञानी के | जीवन में बड़ा अन्तर होता है। बहुत बार दोनों की बाह्य क्रिया एक-सी दिखाई देती है, फिर भी उसके परिणाम में बहुत अधिक भिन्नता होती है। ज्ञानी का जीवन प्रकाश लेकर चलता है, जबकि अज्ञानी अन्धकार में ही भटकता है। ज्ञानी का लक्ष्य स्थिर होता है, अज्ञानी के जीवन में कोई लक्ष्य प्रथम तो होता ही नहीं, अगर हुआ भी तो विचारपूर्ण नहीं होता। उसका ध्येय ऐहिक सुख प्राप्त करने तक ही सीमित होता है। फल यह होता है कि अज्ञानी जीव जो भी साधना करता है वह ऊपरी होती है. अन्तरंग को स्पर्श नहीं करती। उससे भवभ्रमण और बन्धन की वृद्धि होती है, आत्मा के बन्धन कटते नहीं।"
भक्ति एवं प्रार्थना के संबंध में चरितनायक का चिन्तन स्पष्ट था। जैन कर्म सिद्धान्त की मान्यता है कि आत्मा ही अपने सुख-दुःख का कर्ता एवं भोक्ता है। फिर प्रश्न उठता है कि तीर्थकर आदि की स्तुति क्यों की