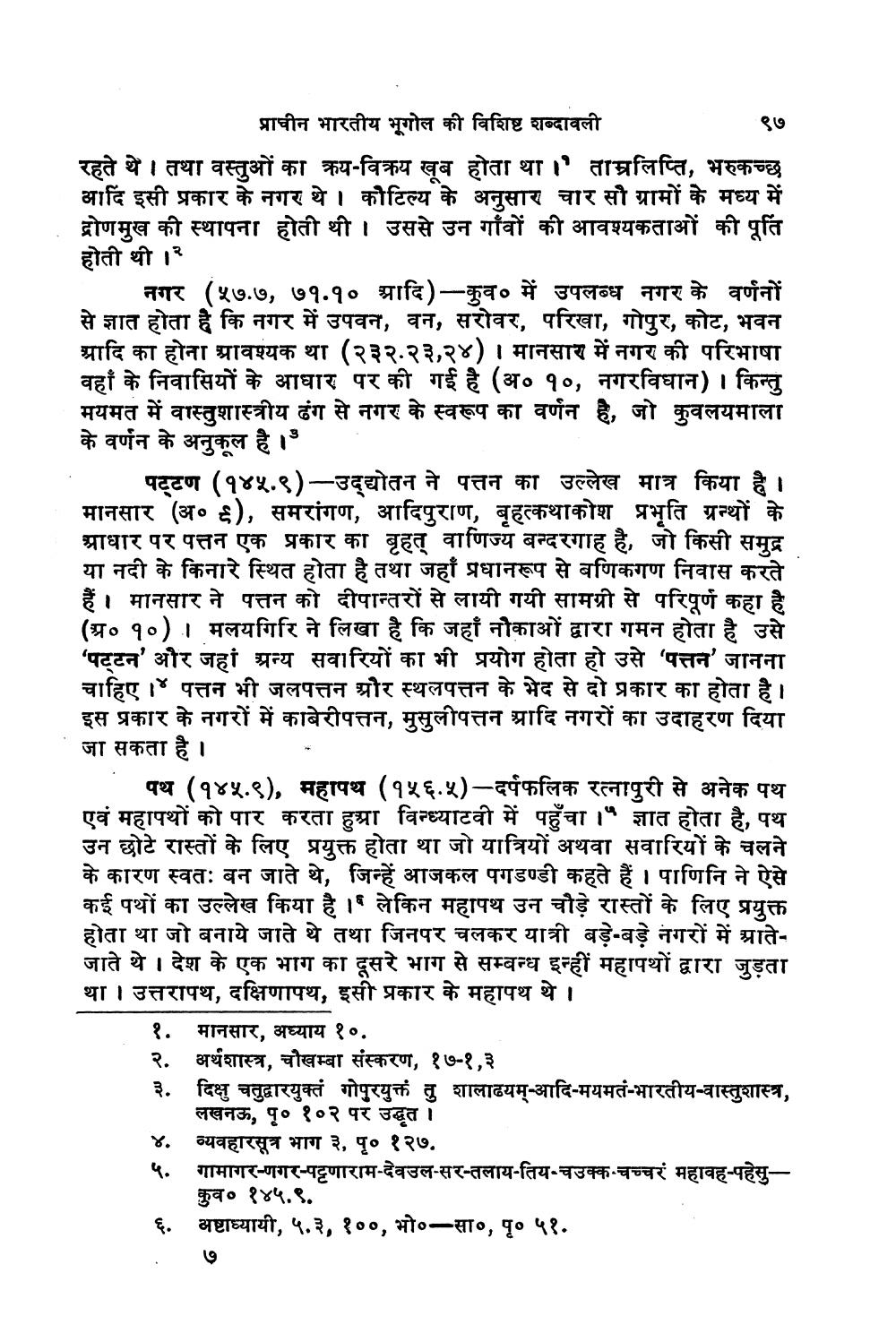________________
प्राचीन भारतीय भूगोल की विशिष्ट शब्दावली
९७ रहते थे। तथा वस्तुओं का क्रय-विक्रय खूब होता था।' ताम्रलिप्ति, भरुकच्छ
आदि इसी प्रकार के नगर थे। कौटिल्य के अनुसार चार सौ ग्रामों के मध्य में द्रोणमुख की स्थापना होती थी। उससे उन गांवों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी।
नगर (५७.७, ७१.१० आदि)-कुव० में उपलब्ध नगर के वर्णनों से ज्ञात होता है कि नगर में उपवन, वन, सरोवर, परिखा, गोपुर, कोट, भवन आदि का होना आवश्यक था (२३२.२३,२४) । मानसार में नगर की परिभाषा वहाँ के निवासियों के आधार पर की गई है (अ० १०, नगरविधान)। किन्तु मयमत में वास्तुशास्त्रीय ढंग से नगर के स्वरूप का वर्णन है, जो कुवलयमाला के वर्णन के अनुकूल है।'
पट्टण (१४५.९)-उद्योतन ने पत्तन का उल्लेख मात्र किया है। मानसार (अ०६), समरांगण, आदिपुराण, बृहत्कथाकोश प्रभृति ग्रन्थों के आधार पर पत्तन एक प्रकार का बृहत् वाणिज्य बन्दरगाह है, जो किसी समुद्र या नदी के किनारे स्थित होता है तथा जहाँ प्रधानरूप से बणिकगण निवास करते हैं। मानसार ने पत्तन को दीपान्तरों से लायी गयी सामग्री से परिपूर्ण कहा है (अ० १०)। मलयगिरि ने लिखा है कि जहाँ नौकाओं द्वारा गमन होता है उसे 'पट्टन' और जहां अन्य सवारियों का भी प्रयोग होता हो उसे 'पत्तन' जानना चाहिए। पत्तन भी जलपत्तन और स्थलपत्तन के भेद से दो प्रकार का होता है। इस प्रकार के नगरों में काबेरीपत्तन, मुसुलीपत्तन आदि नगरों का उदाहरण दिया जा सकता है।
- पथ (१४५.९), महापथ (१५६.५)-दर्पफलिक रत्नापुरी से अनेक पथ एवं महापथों को पार करता हुआ विन्ध्याटवी में पहुँचा। ज्ञात होता है, पथ उन छोटे रास्तों के लिए प्रयुक्त होता था जो यात्रियों अथवा सवारियों के चलने के कारण स्वतः बन जाते थे, जिन्हें आजकल पगडण्डी कहते हैं। पाणिनि ने ऐसे कई पथों का उल्लेख किया है। लेकिन महापथ उन चौड़े रास्तों के लिए प्रयुक्त होता था जो बनाये जाते थे तथा जिनपर चलकर यात्री बड़े-बड़े नगरों में आतेजाते थे। देश के एक भाग का दूसरे भाग से सम्बन्ध इन्हीं महापथों द्वारा जुड़ता था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, इसी प्रकार के महापथ थे।
१. मानसार, अध्याय १०. २. अर्थशास्त्र, चौखम्बा संस्करण, १७-१,३ ३. दिक्षु चतुद्वारयुक्तं गोपुरयुक्तं तु शालाढयम्-आदि-मयमतं-भारतीय-वास्तुशास्त्र,
लखनऊ, पृ० १०२ पर उद्धृत । ४. व्यवहारसूत्र भाग ३, पृ० १२७.
गामागर-णगर-पट्टणाराम-देवउल-सर-तलाय-तिय चउक्क-चच्चरं महावह-पहेसु
कुव० १४५.९. ६. अष्टाध्यायी, ५.३, १००, भो०-सा०, पृ० ५१.