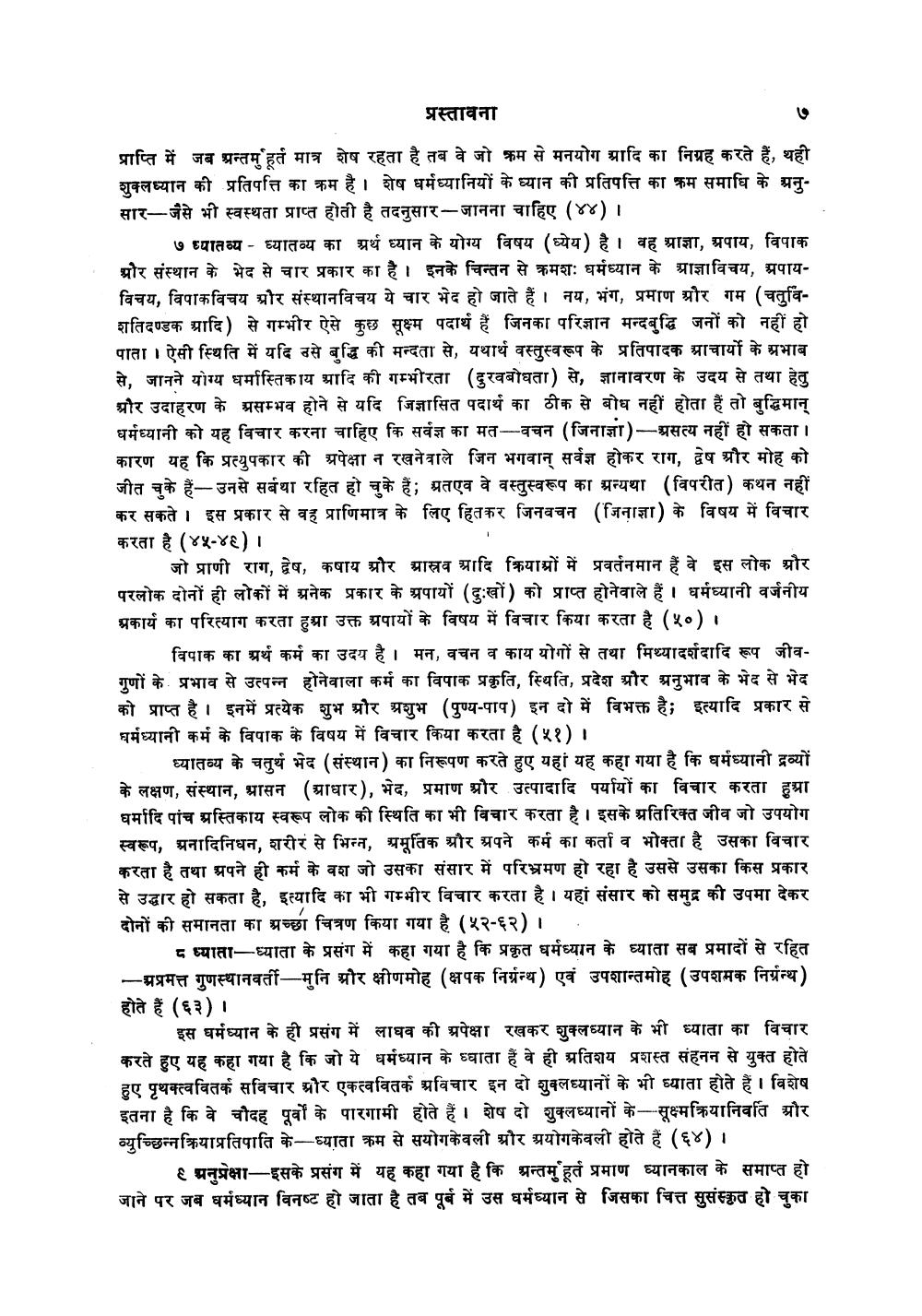________________
प्रस्तावना
प्राप्ति में जब अन्तमुहूर्त मात्र शेष रहता है तब वे जो क्रम से मनयोग आदि का निग्रह करते हैं, थही शुक्लध्यान की प्रतिपत्ति का क्रम है। शेष धर्मध्यानियों के ध्यान की प्रतिपत्ति का क्रम समाधि के अनुसार-जैसे भी स्वस्थता प्राप्त होती है तदनुसार-जानना चाहिए (४४) ।
७ ध्यातव्य - ध्यातव्य का अर्थ ध्यान के योग्य विषय (ध्येय) है। वह आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान के भेद से चार प्रकार का है। इनके चिन्तन से क्रमशः धर्मध्यान के आज्ञा विचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय ये चार भेद हो जाते हैं। नय, भंग, प्रमाण और गम (चतुर्विशतिदण्डक आदि) से गम्भीर ऐसे कुछ सूक्ष्म पदार्थ हैं जिनका परिज्ञान मन्दबुद्धि जनों को नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में यदि उसे बुद्धि की मन्दता से, यथार्थ वस्तुस्वरूप के प्रतिपादक आचार्यों के अभाब से, जानने योग्य धर्मास्तिकाय आदि की गम्भीरता (दुरवबोधता) से, ज्ञानावरण के उदय से तथा हेतु
और उदाहरण के असम्भव होने से यदि जिज्ञासित पदार्थ का ठीक से बोध नहीं होता हैं तो बद्धिमान धर्मध्यानी को यह विचार करना चाहिए कि सर्वज्ञ का मत-वचन (जिनाज्ञा)-असत्य नहीं हो सकता। कारण यह कि प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखनेवाले जिन भगवान् सर्वज्ञ होकर राग, द्वेष और मोह को जीत चुके हैं-उनसे सर्वथा रहित हो चुके हैं। प्रतएव वे वस्तुस्वरूप का अन्यथा (विपरीत) कथन नहीं कर सकते। इस प्रकार से वह प्राणिमात्र के लिए हितकर जिनवचन (जिनाज्ञा) के विषय में विचार करता है (४५-४६)।
जो प्राणी राग, द्वेष, कषाय और आस्रव आदि क्रियानों में प्रवर्तनमान हैं वे इस लोक और परलोक दोनों ही लोकों में अनेक प्रकार के अपायों (दुःखों) को प्राप्त होनेवाले हैं। धर्मध्यानी वर्जनीय अकार्य का परित्याग करता हुआ उक्त अपायों के विषय में विचार किया करता है (५०)।
विपाक का अर्थ कर्म का उदय है। मन, वचन व काय योगों से तथा मिथ्यादर्शदादि रूप जीवगुणों के प्रभाव से उत्पन्न होनेवाला कर्म का विपाक प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाव के भेद से भेद को प्राप्त है। इनमें प्रत्येक शुभ और अशुभ (पुण्य-पाप) इन दो में विभक्त है। इत्यादि प्रकार से धर्मध्यानी कर्म के विपाक के विषय में विचार किया करता है (५१)।
ध्यातव्य के चतुर्थ भेद (संस्थान) का निरूपण करते हुए यहां यह कहा गया है कि धर्मध्यानी द्रव्यों के लक्षण, संस्थान, प्रासन (आधार), भेद, प्रमाण और उत्पादादि पर्यायों का विचार करता हमा धर्मादि पांच अस्तिकाय स्वरूप लोक की स्थिति का भी विचार करता है। इसके अतिरिक्त जीव जो उपयोग स्वरूप, अनादिनिधन, शरीर से भिन्न, अमूर्तिक और अपने कर्म का कर्ता व भोक्ता है उसका विचार करता है तथा अपने ही कर्म के वश जो उसका संसार में परिभ्रमण हो रहा है उससे उसका किस प्रकार से उद्धार हो सकता है, इत्यादि का भी गम्भीर विचार करता है। यहां संसार को समुद्र की उपमा देकर दोनों की समानता का अच्छा चित्रण किया गया है (५२-६२)। .
८ ध्याता-ध्याता के प्रसंग में कहा गया है कि प्रकृत धर्मध्यान के ध्याता सब प्रमादों से रहित -अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती-मुनि और क्षीणमोह (क्षपक निर्ग्रन्थ) एवं उपशान्तमोह (उपशमक निर्ग्रन्थ) होते हैं (६३)।
इस धर्मध्यान के ही प्रसंग में लाघव की अपेक्षा रखकर शुक्लध्यान के भी ध्याता का विचार करते हुए यह कहा गया है कि जो ये धर्मध्यान के ध्याता हैं वे ही अतिशय प्रशस्त संहनन से युक्त होते हुए पृथक्त्ववितर्क सविचार और एकत्ववितर्क अविचार इन दो शुक्लध्यानों के भी ध्याता होते हैं । विशेष इतना है कि वे चौदह पूर्वो के पारगामी होते हैं। शेष दो शुक्लध्यानों के-सूक्ष्मक्रियानिवर्ति और व्युच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति के-ध्याता क्रम से सयोगकेवली और प्रयोगकेवली होते हैं (६४)।
अनुप्रेक्षा-इसके प्रसंग में यह कहा गया है कि अन्तमुहूर्त प्रमाण ध्यानकाल के समाप्त हो जाने पर जब धर्मध्यान विनष्ट हो जाता है तब पूर्व में उस धर्मध्यान से जिसका चित्त सुसंस्कृत हो चुका