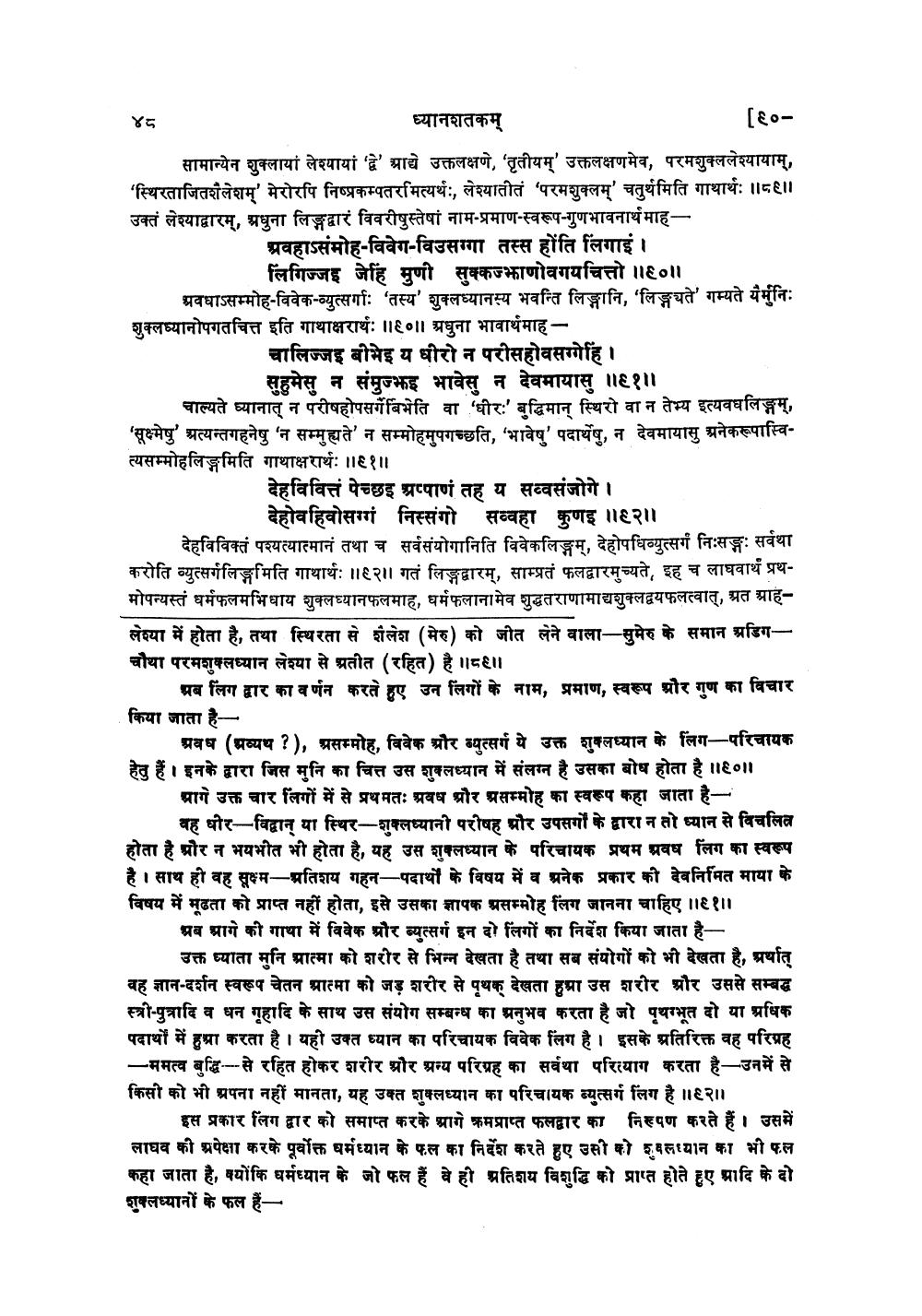________________
४८
ध्यानशतकम्
[६०
.
सामान्येन शुक्लायां लेश्यायां 'द्वे' आद्ये उक्तलक्षणे, 'तृतीयम्' उक्तलक्षणमेव, परमशुक्ललेश्यायाम्, 'स्थिरताजितशैलेशम्' मेरोरपि निष्प्रकम्पतरमित्यर्थः, लेश्यातीतं 'परमशुक्लम्' चतुर्थमिति गाथार्थः ।।६।। उक्तं लेश्याद्वारम्, अधुना लिङ्गद्वारं विवरीषुस्तेषां नाम-प्रमाण-स्वरूप-गुणभावनार्थमाह
प्रवहाऽसंमोह-विवेग-विउसग्गा तस्स होंति लिंगाई।
लिगिज्जइ जेहिं मुणी सुक्कज्झाणोवगयचित्तो ॥१०॥ अवधाऽसम्मोह-विवेक-व्युत्सर्गाः 'तस्य' शुक्लध्यानस्य भवन्ति लिङ्गानि, 'लिङ्गयते' गम्यते यैर्मुनिः शुक्लध्यानोपगतचित्त इति गाथाक्षरार्थः ॥१०॥ अधुना भावार्थमाह
चालिज्जइ बीभेइ य धीरो न परीसहोवसग्गेहिं ।
सुहुमेसु न संमुज्झइ भावेसु न देवमायासु ॥१॥ चाल्यते ध्यानात् न परीषहोपसर्गबिभेति वा 'धीरः' बुद्धिमान स्थिरो वा न तेभ्य इत्यवधलिङ्गम्, 'सूक्ष्मेषु' अत्यन्तगहनेषु 'न सम्मुह्यते' न सम्मोहमुपगच्छति, 'भावेषु' पदार्थेषु, न देवमायासु अनेकरूपास्वित्यसम्मोहलिङ्गमिति गाथाक्षरार्थः ॥११॥
देहविवित्तं पेच्छइ अप्पाणं तह य सव्वसंजोगे।
देहोवहिवोसग्गं निस्संगो सव्वहा कुणइ ॥२॥ देहविविक्तं पश्यत्यात्मानं तथा च सर्वसंयोगानिति विवेकलिङ्गम, देहोपधिव्युत्सर्ग निःसङ्गः सर्वथा करोति व्युत्सर्गलिङ्गमिति गाथार्थः ॥१२॥ गतं लिङ्गद्वारम, साम्प्रतं फलद्वारमुच्यते, इह च लाघवार्थं प्रथमोपन्यस्तं धर्मफलमभिधाय शुक्लध्यानफलमाह, धर्मफलानामेव शुद्धतराणामाद्यशुक्लद्वयफलत्वात्, अत आहलेश्या में होता है, तथा स्थिरता से शैलेश (मेरु) को जीत लेने वाला-सुमेरु के समान अडिगचौथा परमशुक्लध्यान लेश्या से अतीत (रहित) है ॥८६॥
अब लिंग द्वार का वर्णन करते हए उन लिंगों के नाम, प्रमाण, स्वरूप और गुण का विचार किया जाता है
अवध (भव्यथ ?), सम्मोह, विवेक और व्युत्सर्ग ये उक्त शुक्लध्यान के लिंग-परिचायक हेतु हैं। इनके द्वारा जिस मुनि का चित्त उस शुक्लध्यान में संलग्न है उसका बोष होता है ॥१०॥
मागे उक्त चार लिंगों में से प्रथमतः अवध और असम्मोह का स्वरूप कहा जाता है
वह धोर-विद्वान् या स्थिर-शुक्लध्यानी परीषह और उपसर्गों के द्वारा न तो ध्यान से विचलित होता है और न भयभीत भी होता है, यह उस शुक्लध्यान के परिचायक प्रथम अवध लिंग का स्वरूप है। साथ ही वह सूक्ष्म-अतिशय गहन-पदार्थों के विषय में व अनेक प्रकार की देवनिर्मित माया के विषय में मूढता को प्राप्त नहीं होता, इसे उसका ज्ञापक असम्मोह लिंग जानना चाहिए ॥१॥
अब आगे की गाथा में विवेक और व्युत्सर्ग इन दो लिगों का निर्देश किया जाता है
उक्त ध्याता मुनि प्रात्मा को शरीर से भिन्न देखता है तथा सब संयोगों को भी देखता है, अर्थात् वह ज्ञान-दर्शन स्वरूप चेतन प्रात्मा को जड़ शरीर से पृथक देखता हुमा उस शरीर और उससे सम्बद्ध स्त्री-पुत्रादि व धन गुहादि के साथ उस संयोग सम्बन्ध का अनुभव करता है जो पृथग्भूत दो या अधिक पदार्थों में हुआ करता है। यही उक्त ध्यान का परिचायक विवेक लिंग है। इसके अतिरिक्त वह परिग्रह
-ममत्व बुद्धि---से रहित होकर शरीर और अन्य परिग्रह का सर्वथा परित्याग करता है उनमें से किसी को भी अपना नहीं मानता, यह उक्त शुक्लध्यान का परिचायक व्युत्सर्ग लिंग है ॥२॥
इस प्रकार लिंग द्वार को समाप्त करके आगे क्रमप्राप्त फलद्वार का निरूपण करते हैं। उसमें लाघव की अपेक्षा करके पूर्वोक्त धर्मध्यान के फल का निर्देश करते हुए उसी को इपलध्यान का भी फल कहा जाता है, क्योंकि धर्मध्यान के जो फल हैं वे ही अतिशय विशद्धि को प्राप्त होते हुए प्रादि के दो शुक्लध्यानों के फल हैं