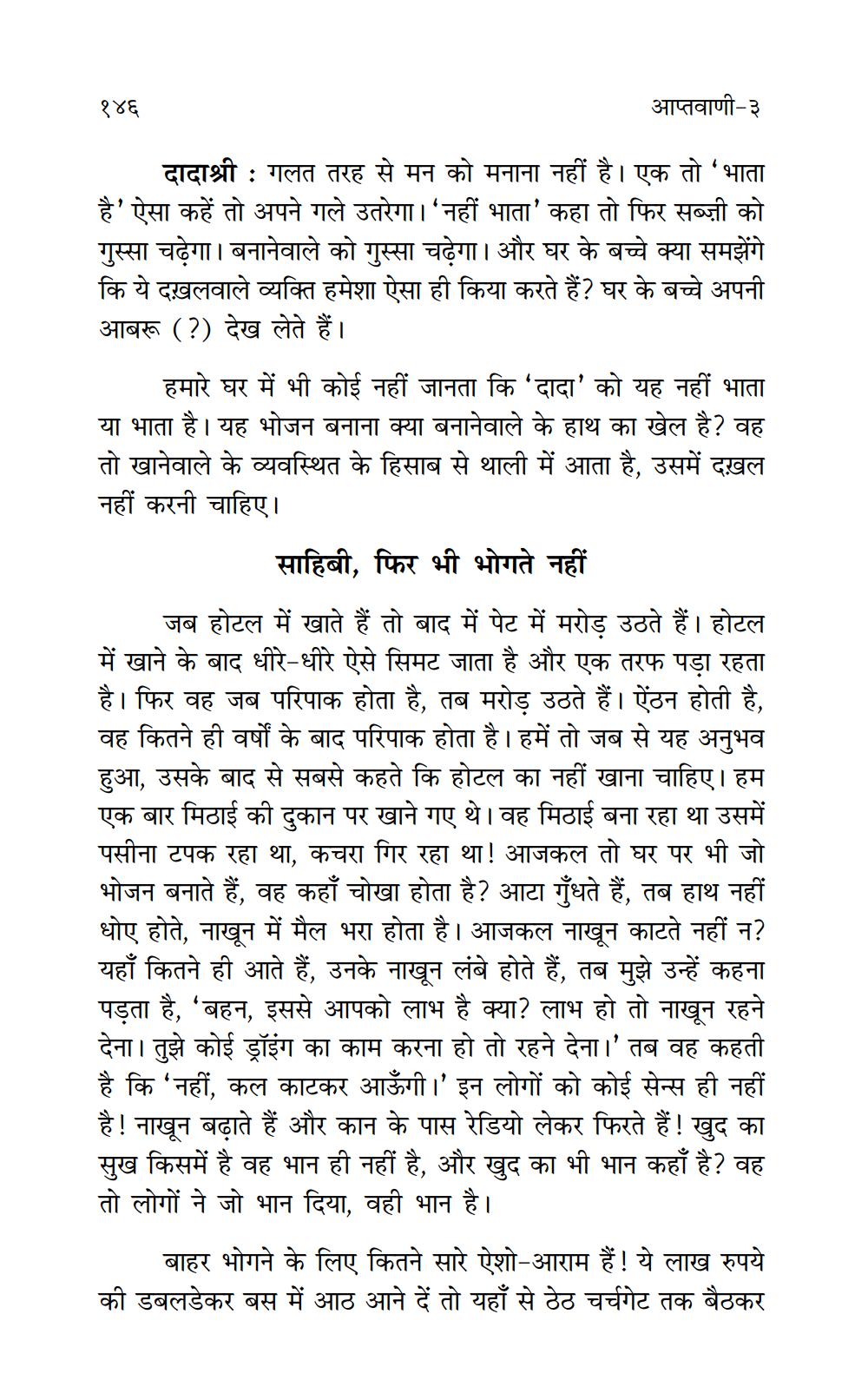________________
१४६
आप्तवाणी-३
दादाश्री : गलत तरह से मन को मनाना नहीं है। एक तो 'भाता है' ऐसा कहें तो अपने गले उतरेगा। 'नहीं भाता' कहा तो फिर सब्जी को गुस्सा चढ़ेगा। बनानेवाले को गुस्सा चढ़ेगा। और घर के बच्चे क्या समझेंगे कि ये दख़लवाले व्यक्ति हमेशा ऐसा ही किया करते हैं? घर के बच्चे अपनी आबरू (?) देख लेते हैं।
हमारे घर में भी कोई नहीं जानता कि 'दादा' को यह नहीं भाता या भाता है। यह भोजन बनाना क्या बनानेवाले के हाथ का खेल है? वह तो खानेवाले के व्यवस्थित के हिसाब से थाली में आता है, उसमें दख़ल नहीं करनी चाहिए।
साहिबी, फिर भी भोगते नहीं जब होटल में खाते हैं तो बाद में पेट में मरोड़ उठते हैं। होटल में खाने के बाद धीरे-धीरे ऐसे सिमट जाता है और एक तरफ पड़ा रहता है। फिर वह जब परिपाक होता है, तब मरोड़ उठते हैं। ऐंठन होती है, वह कितने ही वर्षों के बाद परिपाक होता है। हमें तो जब से यह अनुभव हुआ, उसके बाद से सबसे कहते कि होटल का नहीं खाना चाहिए। हम एक बार मिठाई की दुकान पर खाने गए थे। वह मिठाई बना रहा था उसमें पसीना टपक रहा था, कचरा गिर रहा था! आजकल तो घर पर भी जो भोजन बनाते हैं, वह कहाँ चोखा होता है? आटा गूंधते हैं, तब हाथ नहीं धोए होते, नाखून में मैल भरा होता है। आजकल नाखून काटते नहीं न? यहाँ कितने ही आते हैं, उनके नाखून लंबे होते हैं, तब मुझे उन्हें कहना पड़ता है, 'बहन, इससे आपको लाभ है क्या? लाभ हो तो नाखून रहने देना। तुझे कोई ड्रॉइंग का काम करना हो तो रहने देना।' तब वह कहती है कि 'नहीं, कल काटकर आऊँगी।' इन लोगों को कोई सेन्स ही नहीं है! नाखून बढ़ाते हैं और कान के पास रेडियो लेकर फिरते हैं! खुद का सुख किसमें है वह भान ही नहीं है, और खुद का भी भान कहाँ है? वह तो लोगों ने जो भान दिया, वही भान है।
बाहर भोगने के लिए कितने सारे ऐशो-आराम हैं! ये लाख रुपये की डबलडेकर बस में आठ आने दें तो यहाँ से ठेठ चर्चगेट तक बैठकर