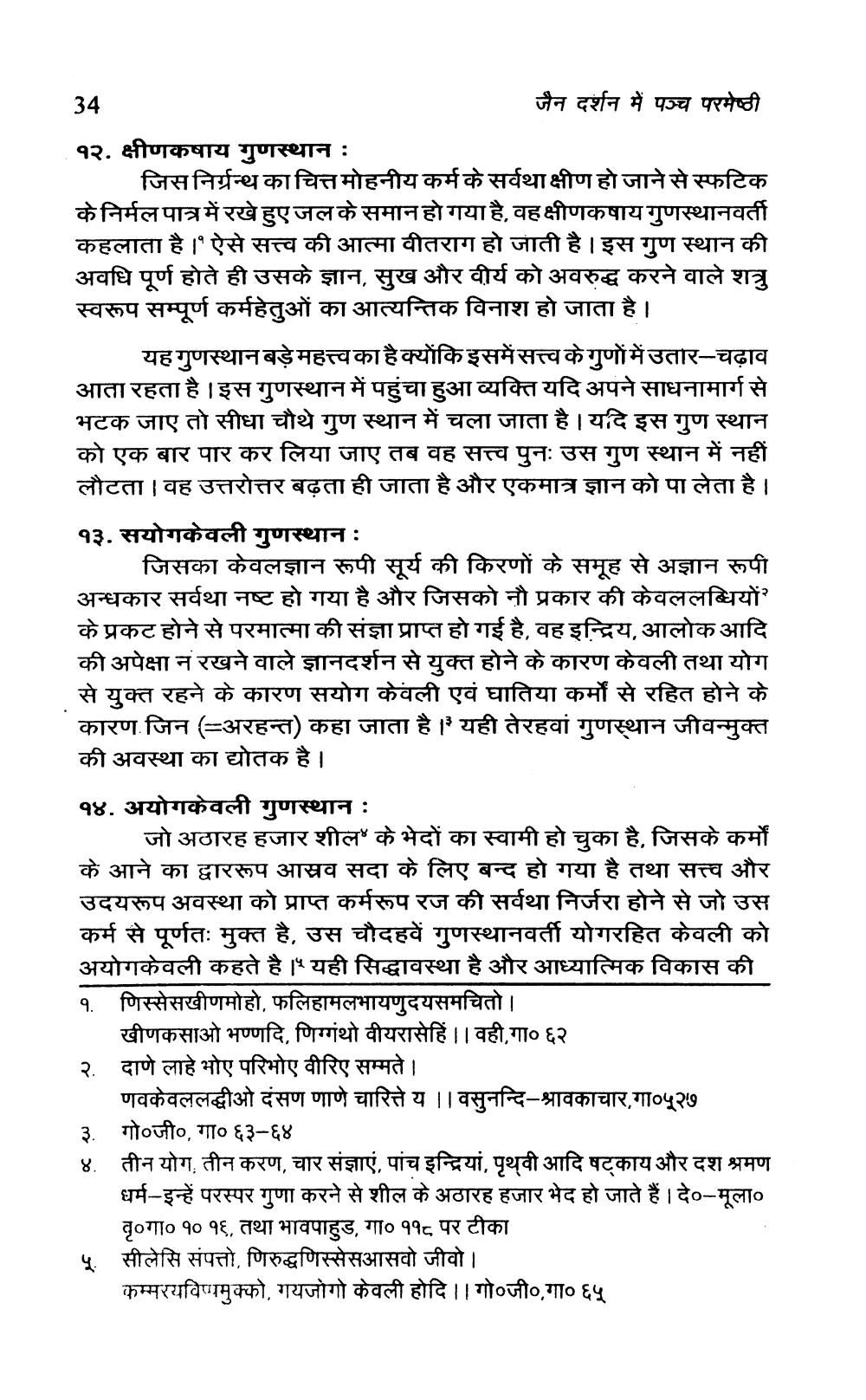________________ 34 जैन दर्शन में पञ्च परमेष्ठी 12. क्षीणकषाय गुणस्थान : जिस निर्ग्रन्थ का चित्तमोहनीय कर्म के सर्वथाक्षीण हो जाने से स्फटिक के निर्मलपात्र में रखे हुए जल के समान हो गया है, वह क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती कहलाता है। ऐसे सत्त्व की आत्मा वीतराग हो जाती है। इस गुण स्थान की अवधि पूर्ण होते ही उसके ज्ञान, सुख और वीर्य को अवरुद्ध करने वाले शत्रु स्वरूप सम्पूर्ण कर्महेतुओं का आत्यन्तिक विनाश हो जाता है। यहगुणस्थानबड़े महत्त्वका है क्योंकि इसमें सत्त्वके गुणों में उतार-चढ़ाव आता रहता है / इस गुणस्थान में पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि अपने साधनामार्ग से भटक जाए तो सीधा चौथे गुण स्थान में चला जाता है। यदि इस गुण स्थान को एक बार पार कर लिया जाए तब वह सत्त्व पुनः उस गुण स्थान में नहीं लौटता / वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है और एकमात्र ज्ञान को पा लेता है। 13. सयोगकेवली गुणस्थान : जिसका केवलज्ञान रूपी सूर्य की किरणों के समूह से अज्ञान रूपी अन्धकार सर्वथा नष्ट हो गया है और जिसको नौ प्रकार की केवललब्धियों' के प्रकट होने से परमात्मा की संज्ञा प्राप्त हो गई है, वह इन्द्रिय, आलोक आदि की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञानदर्शन से युक्त होने के कारण केवली तथा योग से युक्त रहने के कारण सयोग केवली एवं घातिया कर्मों से रहित होने के कारण जिन (अरहन्त) कहा जाता है। यही तेरहवां गुणस्थान जीवन्मुक्त की अवस्था का द्योतक है। 14. अयोगकेवली गुणस्थान : जो अठारह हजार शील के भेदों का स्वामी हो चुका है, जिसके कर्मों के आने का द्वाररूप आस्रव सदा के लिए बन्द हो गया है तथा सत्त्व और उदयरूप अवस्था को प्राप्त कर्मरूप रज की सर्वथा निर्जरा होने से जो उस कर्म से पूर्णतः मुक्त है, उस चौदहवें गुणस्थानवर्ती योगरहित केवली को अयोगकेवली कहते है। यही सिद्धावस्था है और आध्यात्मिक विकास की 1. णिस्सेसखीणमोहो, फलिहामलभायणुदयसमचितो। खीणकसाओ भण्णदि, णिग्गंथो वीयरासेहिं / / वही,गा०६२ 2. दाणे लाहे भोए परिभोए वीरिए सम्मते। णवकेवललद्धीओ देसण णाणे चारित्ते य / / वसुनन्दि-श्रावकाचार,गा०५२७ 3. गो०जी०, गा०६३-६४ 4. तीन योग, तीन करण, चार संज्ञाएं, पांच इन्द्रियां, पृथ्वी आदि षट्काय और दश श्रमण धर्म-इन्हें परस्पर गुणा करने से शील के अठारह हजार भेद हो जाते हैं / दे०-मूला० तृ०गा० 10 16, तथा भावपाहुड, गा० 118 पर टीका / 5. सीलेसि संपत्तो, णिरुद्धणिस्सेसआसवो जीवो। कम्मरयविष्पमुक्को, गयजोगो केवली होदि / / गो०जी०,गा० 65