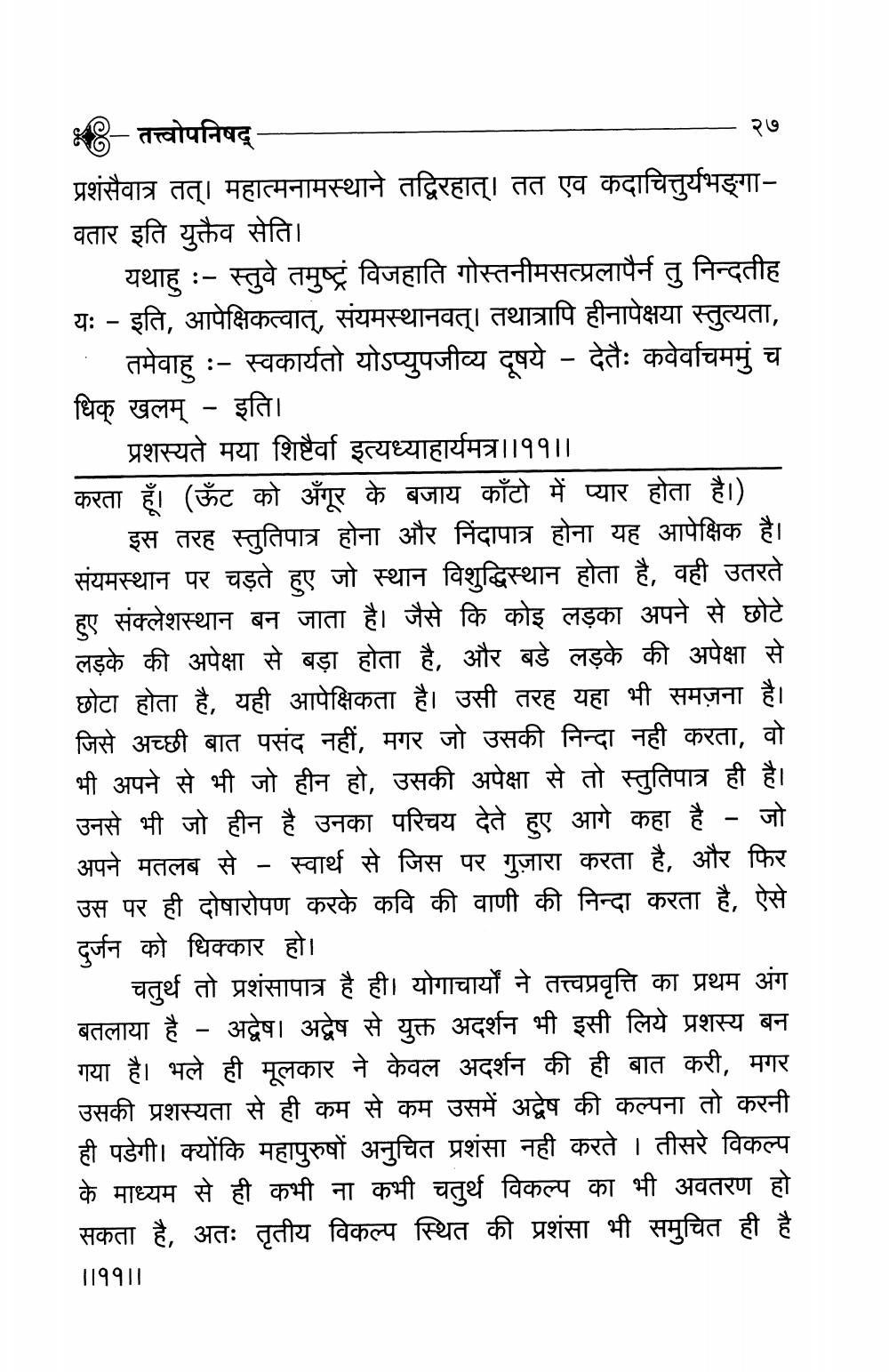________________
- तत्त्वोपनिषद्
- २७ प्रशंसैवात्र तत्। महात्मनामस्थाने तद्विरहात्। तत एव कदाचित्तुर्यभङ्गावतार इति युक्तैव सेति।
यथाहु :- स्तुवे तमुष्टं विजहाति गोस्तनीमसत्प्रलापैर्न तु निन्दतीह यः - इति, आपेक्षिकत्वात्, संयमस्थानवत्। तथात्रापि हीनापेक्षया स्तुत्यता, - तमेवाहु :- स्वकार्यतो योऽप्युपजीव्य दूषये - देतैः कवेर्वाचममुं च धिक् खलम् - इति।
प्रशस्यते मया शिष्टैर्वा इत्यध्याहार्यमत्र।।११।। करता हूँ। (ऊँट को अंगूर के बजाय काँटो में प्यार होता है।)
इस तरह स्तुतिपात्र होना और निंदापात्र होना यह आपेक्षिक है। संयमस्थान पर चड़ते हुए जो स्थान विशुद्धिस्थान होता है, वही उतरते हए संक्लेशस्थान बन जाता है। जैसे कि कोइ लड़का अपने से छोटे लड़के की अपेक्षा से बड़ा होता है, और बड़े लड़के की अपेक्षा से छोटा होता है, यही आपेक्षिकता है। उसी तरह यहा भी समज़ना है। जिसे अच्छी बात पसंद नहीं, मगर जो उसकी निन्दा नहीं करता, वो भी अपने से भी जो हीन हो, उसकी अपेक्षा से तो स्तुतिपात्र ही है। उनसे भी जो हीन है उनका परिचय देते हुए आगे कहा है - जो अपने मतलब से - स्वार्थ से जिस पर गुज़ारा करता है, और फिर उस पर ही दोषारोपण करके कवि की वाणी की निन्दा करता है, ऐसे दुर्जन को धिक्कार हो।
चतुर्थ तो प्रशंसापात्र है ही। योगाचार्यों ने तत्त्वप्रवृत्ति का प्रथम अंग बतलाया है - अद्वेष। अद्वेष से युक्त अदर्शन भी इसी लिये प्रशस्य बन गया है। भले ही मूलकार ने केवल अदर्शन की ही बात करी, मगर उसकी प्रशस्यता से ही कम से कम उसमें अद्वेष की कल्पना तो करनी ही पडेगी। क्योंकि महापुरुषों अनुचित प्रशंसा नही करते । तीसरे विकल्प के माध्यम से ही कभी ना कभी चतुर्थ विकल्प का भी अवतरण हो सकता है, अतः तृतीय विकल्प स्थित की प्रशंसा भी समुचित ही है
||११||