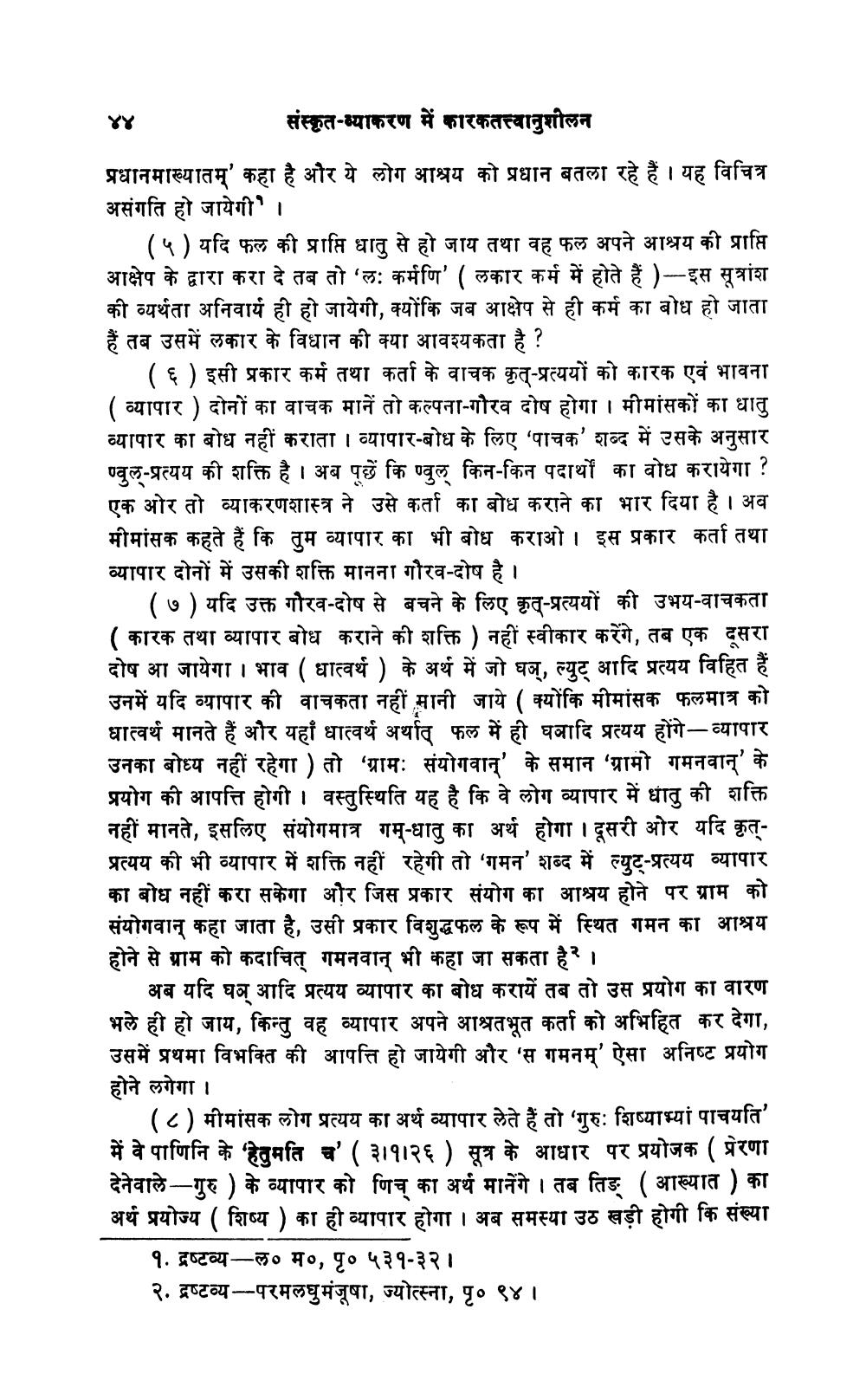________________
संस्कृत-व्याकरण में कारकतत्त्वानुशीलन प्रधानमाख्यातम्' कहा है और ये लोग आश्रय को प्रधान बतला रहे हैं । यह विचित्र असंगति हो जायेगी।
(५) यदि फल की प्राप्ति धातु से हो जाय तथा वह फल अपने आश्रय की प्राप्ति आक्षेप के द्वारा करा दे तब तो 'लः कर्मणि' ( लकार कर्म में होते हैं )-इस सूत्रांश की व्यर्थता अनिवार्य ही हो जायेगी, क्योंकि जब आक्षेप से ही कर्म का बोध हो जाता हैं तब उसमें लकार के विधान की क्या आवश्यकता है ?
(६) इसी प्रकार कर्म तथा कर्ता के वाचक कृत्-प्रत्ययों को कारक एवं भावना ( व्यापार ) दोनों का वाचक मानें तो कल्पना-गौरव दोष होगा । मीमांसकों का धातु व्यापार का बोध नहीं कराता । व्यापार-बोध के लिए 'पाचक' शब्द में उसके अनुसार ण्वुल-प्रत्यय की शक्ति है । अब पूछे कि ण्वुल किन-किन पदार्थों का बोध करायेगा ? एक ओर तो व्याकरणशास्त्र ने उसे कर्ता का बोध कराने का भार दिया है । अब मीमांसक कहते हैं कि तुम व्यापार का भी बोध कराओ। इस प्रकार कर्ता तथा व्यापार दोनों में उसकी शक्ति मानना गौरव-दोष है।
(७) यदि उक्त गौरव-दोष से बचने के लिए कृत्-प्रत्ययों की उभय-वाचकता ( कारक तथा व्यापार बोध कराने की शक्ति ) नहीं स्वीकार करेंगे, तब एक दूसरा दोष आ जायेगा । भाव ( धात्वर्थ ) के अर्थ में जो घञ्, ल्युट आदि प्रत्यय विहित हैं उनमें यदि व्यापार की वाचकता नहीं मानी जाये ( क्योंकि मीमांसक फलमात्र को धात्वर्थ मानते हैं और यहाँ धात्वर्थ अर्थात् फल में ही घनादि प्रत्यय होंगे-व्यापार उनका बोध्य नहीं रहेगा ) तो 'ग्रामः संयोगवान्' के समान 'ग्रामो गमनवान्' के प्रयोग की आपत्ति होगी। वस्तुस्थिति यह है कि वे लोग व्यापार में धातु की शक्ति नहीं मानते, इसलिए संयोगमात्र गम्-धातु का अर्थ होगा । दूसरी ओर यदि कृत्प्रत्यय की भी व्यापार में शक्ति नहीं रहेगी तो 'गमन' शब्द में ल्युट्-प्रत्यय व्यापार का बोध नहीं करा सकेगा और जिस प्रकार संयोग का आश्रय होने पर ग्राम को संयोगवान् कहा जाता है, उसी प्रकार विशुद्धफल के रूप में स्थित गमन का आश्रय होने से ग्राम को कदाचित् गमनवान् भी कहा जा सकता है।
अब यदि घञ् आदि प्रत्यय व्यापार का बोध करायें तब तो उस प्रयोग का वारण भले ही हो जाय, किन्तु वह व्यापार अपने आश्रतभूत कर्ता को अभिहित कर देगा, उसमें प्रथमा विभक्ति की आपत्ति हो जायेगी और 'स गमनम्' ऐसा अनिष्ट प्रयोग होने लगेगा।
(८) मीमांसक लोग प्रत्यय का अर्थ व्यापार लेते हैं तो 'गुरुः शिष्याभ्यां पाचयति' में वे पाणिनि के 'हेतुमति च' ( ३।१।२६ ) सूत्र के आधार पर प्रयोजक ( प्रेरणा देनेवाले–गुरु ) के व्यापार को णिच का अर्थ मानेंगे । तब तिङ् ( आख्यात ) का अर्थ प्रयोज्य ( शिष्य ) का ही व्यापार होगा। अब समस्या उठ खड़ी होगी कि संख्या
१. द्रष्टव्य-ल० म०, पृ० ५३१-३२ । २. द्रष्टव्य-परमलघुमंजूषा, ज्योत्स्ना, पृ० ९४ ।