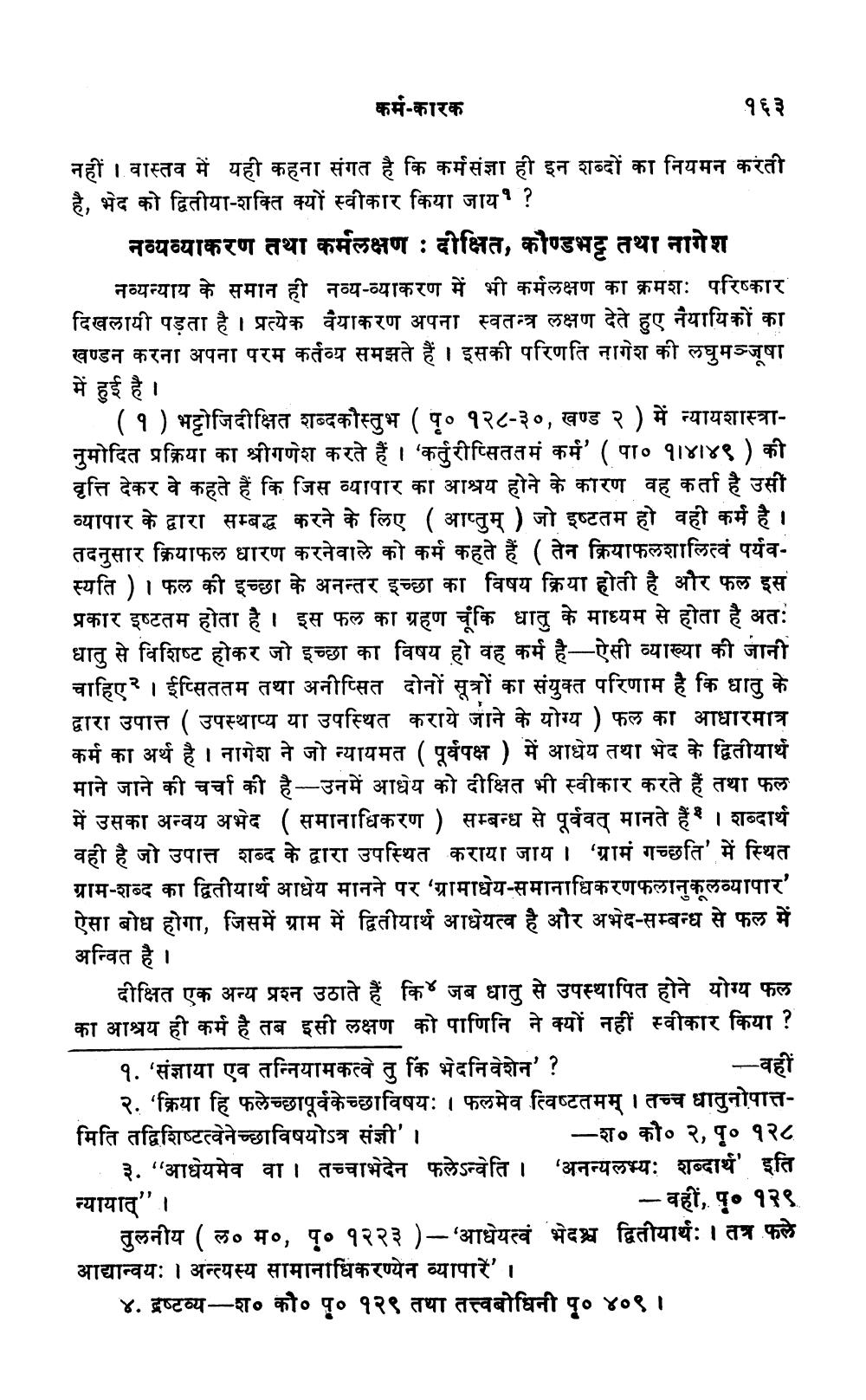________________
कर्म-कारक
१६३
नहीं । वास्तव में यही कहना संगत है कि कर्मसंज्ञा ही इन शब्दों का नियमन करती है, भेद को द्वितीया-शक्ति क्यों स्वीकार किया जाय' ?
नव्यव्याकरण तथा कर्मलक्षण : दीक्षित, कौण्डभट्ट तथा नागेश
नव्यन्याय के समान ही नव्य-व्याकरण में भी कर्मलक्षण का क्रमशः परिष्कार दिखलायी पड़ता है । प्रत्येक वैयाकरण अपना स्वतन्त्र लक्षण देते हुए नैयायिकों का खण्डन करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं । इसकी परिणति नागेश की लघुमञ्जूषा
(१) भट्टोजिदीक्षित शब्दकौस्तुभ ( पृ० १२८-३०, खण्ड २ ) में न्यायशास्त्रानुमोदित प्रक्रिया का श्रीगणेश करते हैं । 'कर्तुरीप्सिततमं कर्म' ( पा० १।४।४९ ) की वृत्ति देकर वे कहते हैं कि जिस व्यापार का आश्रय होने के कारण वह कर्ता है उसी व्यापार के द्वारा सम्बद्ध करने के लिए ( आप्तुम् ) जो इष्टतम हो वही कर्म है। तदनुसार क्रियाफल धारण करनेवाले को कर्म कहते हैं ( तेन क्रियाफलशालित्वं पर्यवस्यति )। फल की इच्छा के अनन्तर इच्छा का विषय क्रिया होती है और फल इस प्रकार इष्टतम होता है। इस फल का ग्रहण चूंकि धातु के माध्यम से होता है अतः धातु से विशिष्ट होकर जो इच्छा का विषय हो वह कर्म है-ऐसी व्याख्या की जानी चाहिए । ईप्सिततम तथा अनीप्सित दोनों सूत्रों का संयुक्त परिणाम है कि धातु के द्वारा उपात्त ( उपस्थाप्य या उपस्थित कराये जाने के योग्य ) फल का आधारमात्र कर्म का अर्थ है । नागेश ने जो न्यायमत (पूर्वपक्ष ) में आधेय तथा भेद के द्वितीयार्थ माने जाने की चर्चा की है-उनमें आधेय को दीक्षित भी स्वीकार करते हैं तथा फल में उसका अन्वय अभेद ( समानाधिकरण ) सम्बन्ध से पूर्ववत् मानते हैं ३ । शब्दार्थ वही है जो उपात्त शब्द के द्वारा उपस्थित कराया जाय । 'ग्रामं गच्छति' में स्थित ग्राम-शब्द का द्वितीयार्थ आधेय मानने पर 'ग्रामाधेय-समानाधिकरणफलानुकलव्यापार' ऐसा बोध होगा, जिसमें ग्राम में द्वितीयार्थ आधेयत्व है और अभेद-सम्बन्ध से फल में अन्वित है।
दीक्षित एक अन्य प्रश्न उठाते हैं कि जब धातु से उपस्थापित होने योग्य फल का आश्रय ही कर्म है तब इसी लक्षण को पाणिनि ने क्यों नहीं स्वीकार किया? १. 'संज्ञाया एव तन्नियामकत्वे तु किं भेदनिवेशेन' ?
-वहीं २. 'क्रिया हि फलेच्छापूर्वकेच्छाविषयः । फलमेव त्विष्टतमम् । तच्च धातुनोपात्तमिति तद्विशिष्टत्वेनेच्छाविषयोऽत्र संज्ञी' ।
-श० को० २, पृ० १२८ . ३. "आधेयमेव वा। तच्चाभेदेन फलेऽन्वेति । 'अनन्यलभ्यः शब्दार्थ' इति न्यायात्"।
- वहीं, पृ. १२९ तुलनीय ( ल० म०, पृ० १२२३ )- 'आधेयत्वं भेदश्च द्वितीयार्थः । तत्र फले आद्यान्वयः । अन्त्यस्य सामानाधिकरण्येन व्यापारे'।
४. द्रष्टव्य-श० को० पृ० १२९ तथा तत्त्वबोधिनी पृ० ४०९ ।