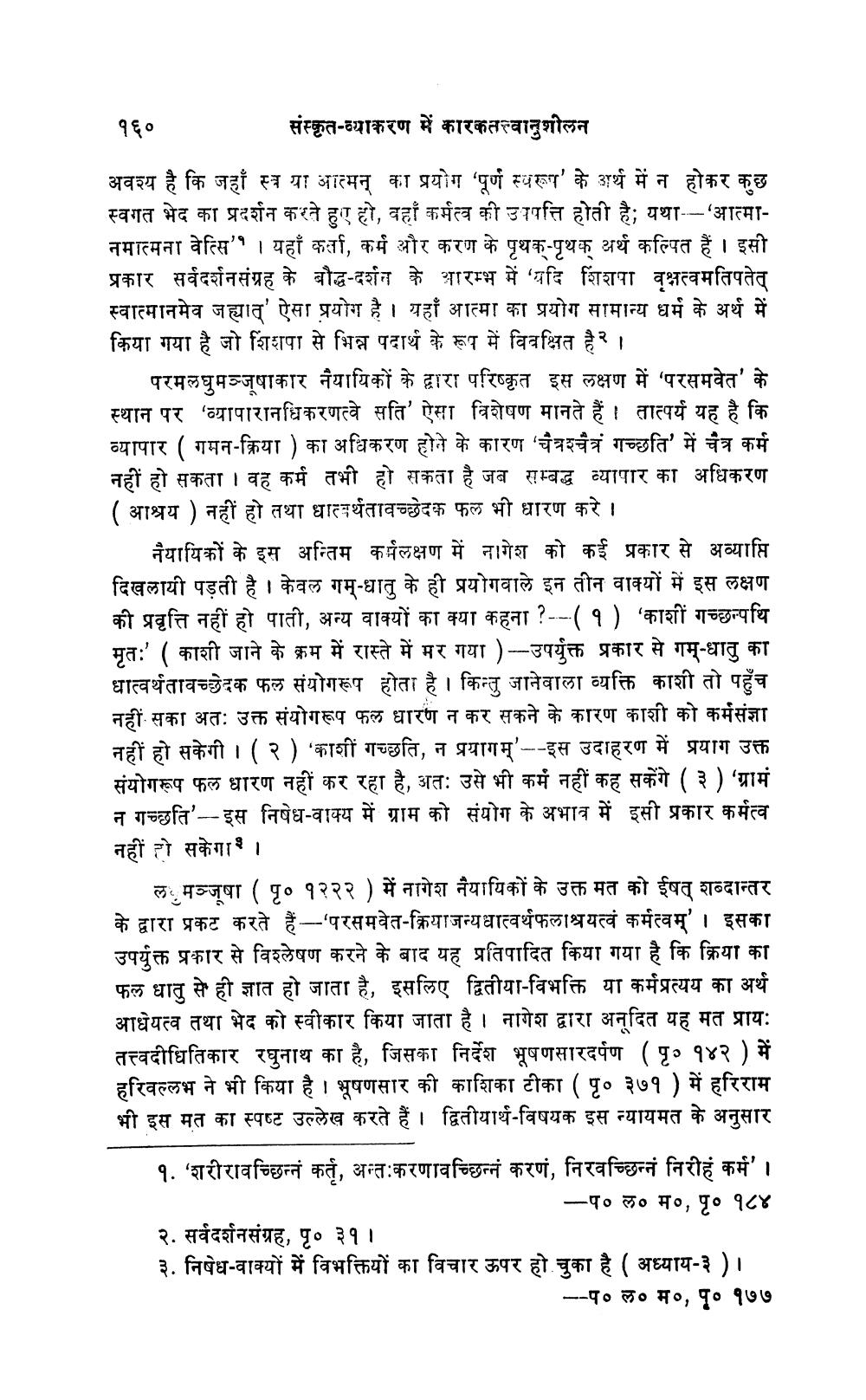________________
१६०
संस्कृत-व्याकरण में कारकतत्त्वानुशीलन अवश्य है कि जहाँ स्त्र या आत्मन् का प्रयोग 'पूर्ण स्वरूप' के अर्थ में न होकर कुछ स्वगत भेद का प्रदर्शन करते हुए हो, वहाँ कर्मत्व की अपत्ति होती है; यथा--- 'आत्मानमात्मना वेत्सि'' । यहाँ कर्ता, कर्म और करण के पृथक्-पृथक् अर्थ कल्पित हैं । इसी प्रकार सर्वदर्शनसंग्रह के बौद्ध-दर्शन के आरम्भ में 'यदि शिंशपा वृक्षत्वमतिपतेत् स्वात्मानमेव जह्यात्' ऐसा प्रयोग है। यहाँ आत्मा का प्रयोग सामान्य धर्म के अर्थ में किया गया है जो शिशपा से भिन्न पदार्थ के रूप में विवक्षित है ।
परमल घुमञ्जूषाकार नैयायिकों के द्वारा परिष्कृत इस लक्षण में 'परसमवेत' के स्थान पर 'व्यापारानधिकरणत्वे सति' ऐसा विशेषण मानते हैं। तात्पर्य यह है कि व्यापार ( गमन-क्रिया ) का अधिकरण होने के कारण 'चैत्रश्चैत्रं गच्छति' में चैत्र कर्म नहीं हो सकता । वह कर्म तभी हो सकता है जब सम्बद्ध व्यापार का अधिकरण ( आश्रय ) नहीं हो तथा धात्वर्थतावच्छेदक फल भी धारण करे ।
नैयायिकों के इस अन्तिम कर्मलक्षण में नागेश को कई प्रकार से अव्याप्ति दिखलायी पड़ती है । केवल गम्-धातु के ही प्रयोगवाले इन तीन वाक्यों में इस लक्षण की प्रवृत्ति नहीं हो पाती, अन्य वाक्यों का क्या कहना ?--(१) 'काशी गच्छन्पथि मृतः' ( काशी जाने के क्रम में रास्ते में मर गया )-उपर्युक्त प्रकार से गम्-धातु का धात्वर्थतावच्छेदक फल संयोगरूप होता है। किन्तु जानेवाला व्यक्ति काशी तो पहुँच नहीं सका अत: उक्त संयोगरूप फल धारण न कर सकने के कारण काशी को कर्मसंज्ञा नहीं हो सकेगी। ( २ ) 'काशीं गच्छति, न प्रयागम्'--इस उदाहरण में प्रयाग उक्त संयोगरूप फल धारण नहीं कर रहा है, अत: उसे भी कम नहीं कह सकेंगे ( ३ ) 'ग्राम न गच्छति'- इस निषेध-वाक्य में ग्राम को संयोग के अभाव में इसी प्रकार कर्मत्व नहीं हो सकेगा।
लमषा ( पृ० १२२२ ) में नागेश नैयायिकों के उक्त मत को ईषत् शब्दान्तर के द्वारा प्रकट करते हैं -'परसमवेत-क्रियाजन्यधात्वर्थफलाश्रयत्वं कर्मत्वम्'। इसका उपर्युक्त प्रकार से विश्लेषण करने के बाद यह प्रतिपादित किया गया है कि क्रिया का फल धातु से ही ज्ञात हो जाता है, इसलिए द्वितीया-विभक्ति या कर्मप्रत्यय का अर्थ आधेयत्व तथा भेद को स्वीकार किया जाता है। नागेश द्वारा अनूदित यह मत प्रायः तत्त्वदीधितिकार रघुनाथ का है, जिसका निर्देश भूषणसारदर्पण ( पृ० १४२ ) में हरिवल्लभ ने भी किया है । भूषणसार की काशिका टीका ( पृ० ३७१ ) में हरिराम भी इस मत का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। द्वितीयार्थ-विषयक इस न्यायमत के अनुसार
१. 'शरीरावच्छिन्नं कर्तृ, अन्तःकरणावच्छिन्नं करणं, निरवच्छिन्नं निरीहं कर्म' ।
-प० ल० म०, पृ० १८४ २. सर्वदर्शनसंग्रह, पृ० ३१ । ३. निषेध-वाक्यों में विभक्तियों का विचार ऊपर हो चुका है ( अध्याय-३ )।
--प० ल० म०, पृ० १७७