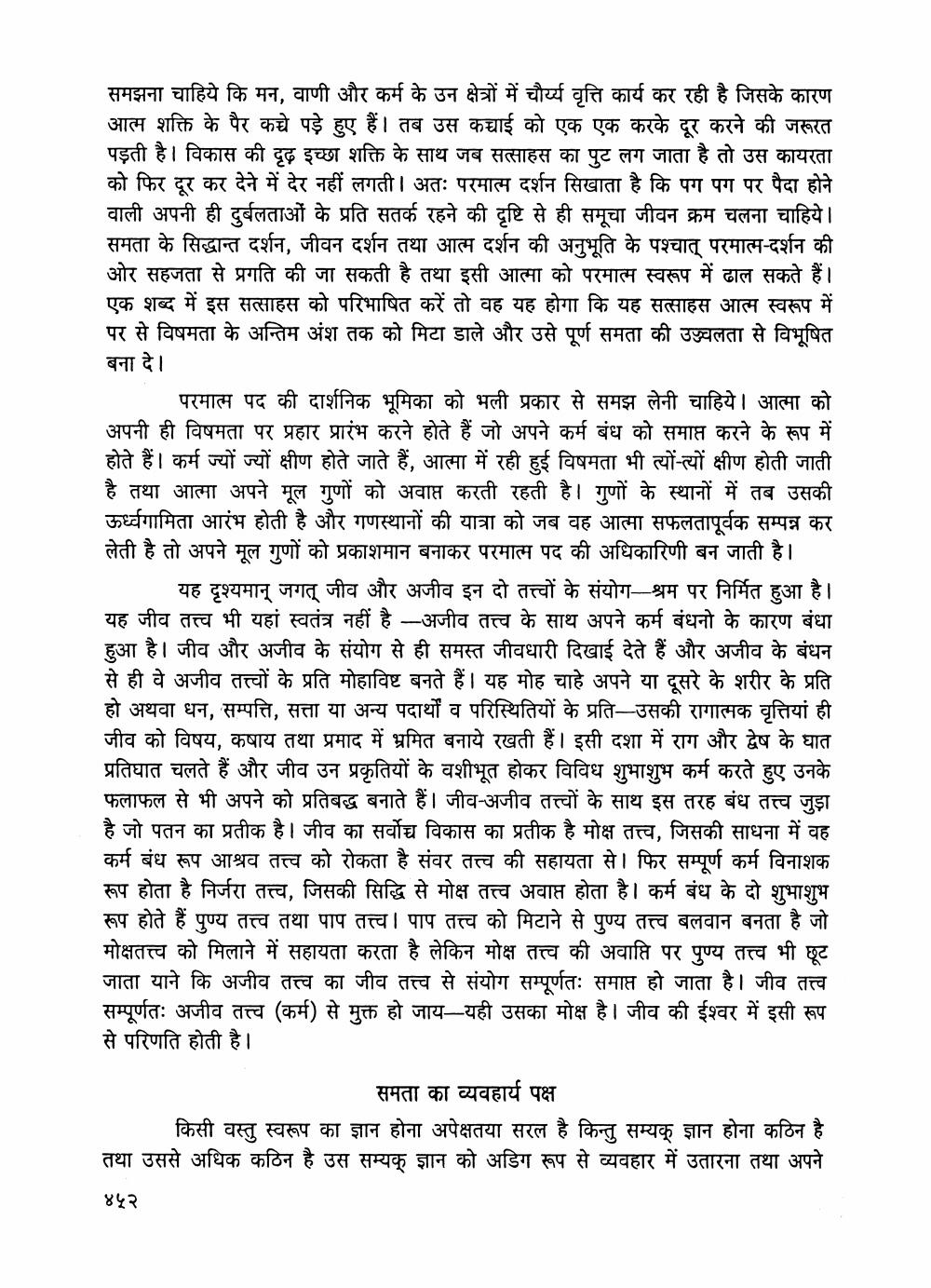________________
समझना चाहिये कि मन, वाणी और कर्म के उन क्षेत्रों में चौर्य्य वृत्ति कार्य कर रही है जिसके कारण आत्म शक्ति के पैर कच्चे पड़े हुए हैं। तब उस कच्चाई को एक एक करके दूर करने की जरूरत पड़ती है। विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब सत्साहस का पुट लग जाता है तो उस कायरता को फिर दूर कर देने में देर नहीं लगती। अतः परमात्म दर्शन सिखाता है कि पग पग पर पैदा होने वाली अपनी ही दुर्बलताओं के प्रति सतर्क रहने की दृष्टि से ही समूचा जीवन क्रम चलना चाहिये। समता के सिद्धान्त दर्शन, जीवन दर्शन तथा आत्म दर्शन की अनुभूति के पश्चात् परमात्म-दर्शन की
ओर सहजता से प्रगति की जा सकती है तथा इसी आत्मा को परमात्म स्वरूप में ढाल सकते हैं। एक शब्द में इस सत्साहस को परिभाषित करें तो वह यह होगा कि यह सत्साहस आत्म स्वरूप में पर से विषमता के अन्तिम अंश तक को मिटा डाले और उसे पूर्ण समता की उज्ज्वलता से विभूषित बना दे।
परमात्म पद की दार्शनिक भूमिका को भली प्रकार से समझ लेनी चाहिये। आत्मा को अपनी ही विषमता पर प्रहार प्रारंभ करने होते हैं जो अपने कर्म बंध को समाप्त करने के रूप में होते हैं। कर्म ज्यों ज्यों क्षीण होते जाते हैं, आत्मा में रही हुई विषमता भी त्यों-त्यों क्षीण होती जाती है तथा आत्मा अपने मूल गुणों को अवाप्त करती रहती है। गुणों के स्थानों में तब उसकी ऊर्ध्वगामिता आरंभ होती है और गणस्थानों की यात्रा को जब वह आत्मा सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेती है तो अपने मूल गुणों को प्रकाशमान बनाकर परमात्म पद की अधिकारिणी बन जाती है।
यह दृश्यमान् जगत् जीव और अजीव इन दो तत्त्वों के संयोग श्रम पर निर्मित हुआ है। यह जीव तत्त्व भी यहां स्वतंत्र नहीं है -अजीव तत्त्व के साथ अपने कर्म बंधनो के कारण बंधा हुआ है। जीव और अजीव के संयोग से ही समस्त जीवधारी दिखाई देते हैं और अजीव के बंधन से ही वे अजीव तत्त्वों के प्रति मोहाविष्ट बनते हैं। यह मोह चाहे अपने या दूसरे के शरीर के प्रति हो अथवा धन, सम्पत्ति, सत्ता या अन्य पदार्थों व परिस्थितियों के प्रति उसकी रागात्मक वृत्तियां ही जीव को विषय, कषाय तथा प्रमाद में भ्रमित बनाये रखती हैं। इसी दशा में राग और द्वेष के घात प्रतिघात चलते हैं और जीव उन प्रकृतियों के वशीभूत होकर विविध शुभाशुभ कर्म करते हुए उनके फलाफल से भी अपने को प्रतिबद्ध बनाते हैं। जीव-अजीव तत्त्वों के साथ इस तरह बंध तत्त्व जुड़ा है जो पतन का प्रतीक है। जीव का सर्वोच्च विकास का प्रतीक है मोक्ष तत्त्व, जिसकी साधना में वह कर्म बंध रूप आश्रव तत्त्व को रोकता है संवर तत्त्व की सहायता से। फिर सम्पूर्ण कर्म विनाशक रूप होता है निर्जरा तत्त्व, जिसकी सिद्धि से मोक्ष तत्त्व अवाप्त होता है। कर्म बंध के दो शुभाशुभ रूप होते हैं पुण्य तत्त्व तथा पाप तत्त्व। पाप तत्त्व को मिटाने से पुण्य तत्त्व बलवान बनता है जो मोक्षतत्त्व को मिलाने में सहायता करता है लेकिन मोक्ष तत्त्व की अवाप्ति पर पुण्य तत्त्व भी छूट जाता याने कि अजीव तत्त्व का जीव तत्त्व से संयोग सम्पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जीव तत्त्व सम्पूर्णतः अजीव तत्त्व (कर्म) से मुक्त हो जाय—यही उसका मोक्ष है। जीव की ईश्वर में इसी रूप से परिणति होती है।
समता का व्यवहार्य पक्ष किसी वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना अपेक्षतया सरल है किन्तु सम्यक् ज्ञान होना कठिन है तथा उससे अधिक कठिन है उस सम्यक् ज्ञान को अडिग रूप से व्यवहार में उतारना तथा अपने
४५२