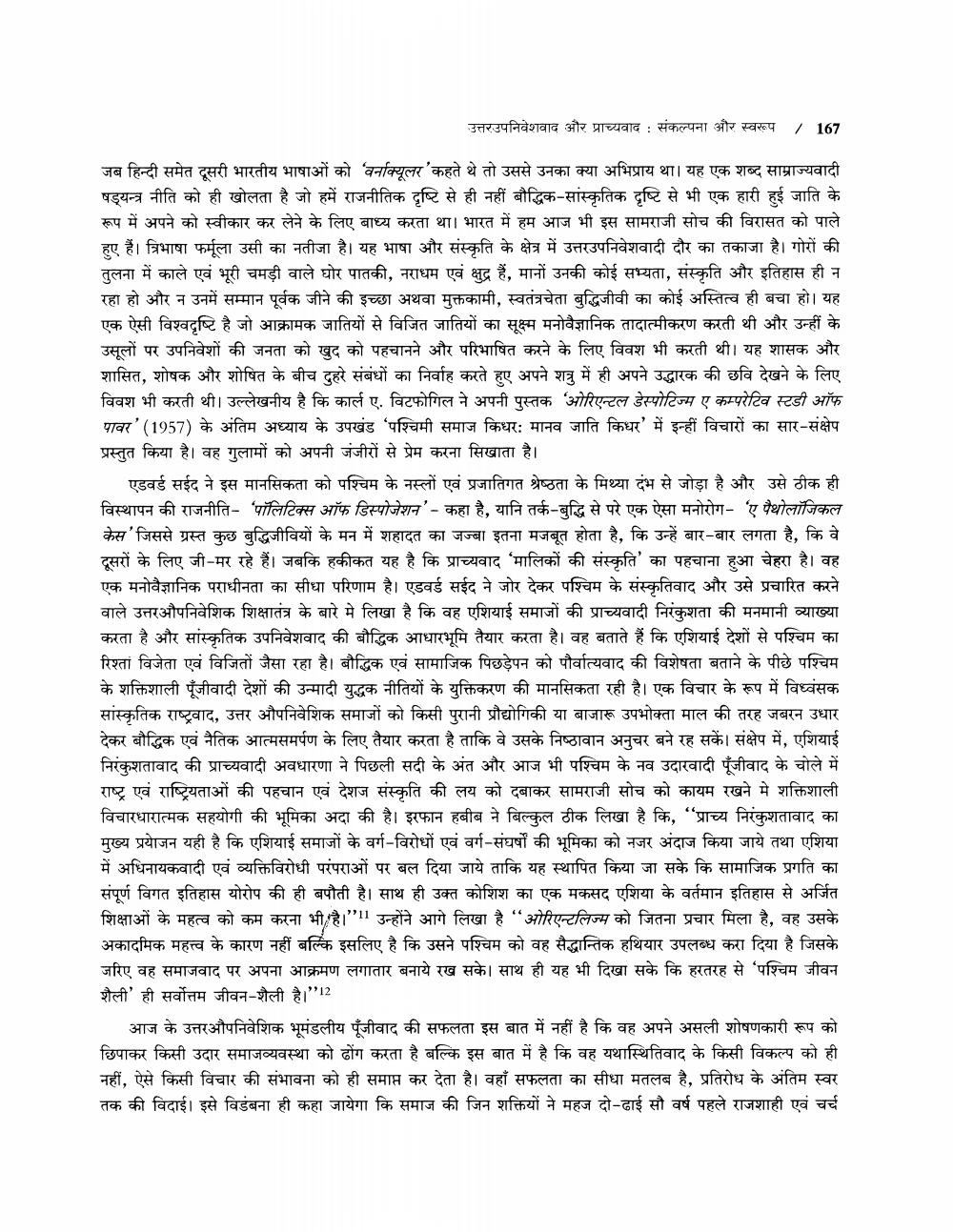________________
उत्तरउपनिवेशवाद और प्राच्यवाद : संकल्पना और स्वरूप / 167
जब हिन्दी समेत दूसरी भारतीय भाषाओं को 'वर्नाक्यूलर' कहते थे तो उससे उनका क्या अभिप्राय था। यह एक शब्द साम्राज्यवादी षड्यन्त्र नीति को ही खोलता है जो हमें राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बौद्धिक-सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक हारी हुई जाति के रूप में अपने को स्वीकार कर लेने के लिए बाध्य करता था। भारत में हम आज भी इस सामराजी सोच की विरासत को पाले हुए हैं। त्रिभाषा फर्मूला उसी का नतीजा है। यह भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में उत्तरउपनिवेशवादी दौर का तकाजा है। गोरों की तुलना में काले एवं भूरी चमड़ी वाले घोर पातकी, नराधम एवं क्षुद्र हैं, मानों उनकी कोई सभ्यता, संस्कृति और इतिहास ही न रहा हो और न उनमें सम्मान पूर्वक जीने की इच्छा अथवा मुक्तकामी, स्वतंत्रचेता बुद्धिजीवी का कोई अस्तित्व ही बचा हो। यह एक ऐसी विश्वदृष्टि है जो आक्रामक जातियों से विजित जातियों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तादात्मीकरण करती थी और उन्हीं के उसूलों पर उपनिवेशों की जनता को खुद को पहचानने और परिभाषित करने के लिए विवश भी करती थी। यह शासक और शासित, शोषक और शोषित के बीच दुहरे संबंधों का निर्वाह करते हुए अपने शत्रु में ही अपने उद्धारक की छवि देखने के लिए विवश भी करती थी। उल्लेखनीय है कि कार्ल ए. विटफोगिल ने अपनी पुस्तक 'ओरिएन्टल डेस्पोटिज्म ए कम्परेटिव स्टडी ऑफ पावर' (1957) के अंतिम अध्याय के उपखंड ‘पश्चिमी समाज किधर: मानव जाति किधर' में इन्हीं विचारों का सार-संक्षेप प्रस्तुत किया है। वह गुलामों को अपनी जंजीरों से प्रेम करना सिखाता है।
एडवर्ड सईद ने इस मानसिकता को पश्चिम के नस्लों एवं प्रजातिगत श्रेष्ठता के मिथ्या दंभ से जोड़ा है और उसे ठीक ही विस्थापन की राजनीति- 'पॉलिटिक्स ऑफ डिस्पोजेशन'- कहा है, यानि तर्क-बुद्धि से परे एक ऐसा मनोरोग- 'ए पैथोलॉजिकल केस'जिससे ग्रस्त कुछ बुद्धिजीवियों के मन में शहादत का जज्बा इतना मजबूत होता है, कि उन्हें बार-बार लगता है, कि वे दूसरों के लिए जी-मर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि प्राच्यवाद 'मालिकों की संस्कृति' का पहचाना हुआ चेहरा है। वह एक मनोवैज्ञानिक पराधीनता का सीधा परिणाम है। एडवर्ड सईद ने जोर देकर पश्चिम के संस्कृतिवाद और उसे प्रचारित करने वाले उत्तरऔपनिवेशिक शिक्षातंत्र के बारे मे लिखा है कि वह एशियाई समाजों की प्राच्यवादी निरंकुशता की मनमानी व्याख्या करता है और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की बौद्धिक आधारभूमि तैयार करता है। वह बताते हैं कि एशियाई देशों से पश्चिम का रिश्तां विजेता एवं विजितों जैसा रहा है। बौद्धिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को पौर्वात्यवाद की विशेषता बताने के पीछे पश्चिम के शक्तिशाली पूँजीवादी देशों की उन्मादी युद्धक नीतियों के युक्तिकरण की मानसिकता रही है। एक विचार के रूप में विध्वंसक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उत्तर औपनिवेशिक समाजों को किसी पुरानी प्रौद्योगिकी या बाजारू उपभोक्ता माल की तरह जबरन उधार देकर बौद्धिक एवं नैतिक आत्मसमर्पण के लिए तैयार करता है ताकि वे उसके निष्ठावान अनुचर बने रह सकें। संक्षेप में, एशियाई निरंकुशतावाद की प्राच्यवादी अवधारणा ने पिछली सदी के अंत और आज भी पश्चिम के नव उदारवादी पूँजीवाद के चोले में राष्ट्र एवं राष्ट्रियताओं की पहचान एवं देशज संस्कृति की लय को दबाकर सामराजी सोच को कायम रखने मे शक्तिशाली विचारधारात्मक सहयोगी की भूमिका अदा की है। इरफान हबीब ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि, “प्राच्य निरंकुशतावाद का मुख्य प्रयोजन यही है कि एशियाई समाजों के वर्ग-विरोधों एवं वर्ग-संघर्षों की भूमिका को नजर अंदाज किया जाये तथा एशिया में अधिनायकवादी एवं व्यक्तिविरोधी परंपराओं पर बल दिया जाये ताकि यह स्थापित किया जा सके कि सामाजिक प्रगति का संपूर्ण विगत इतिहास योरोप की ही बपौती है। साथ ही उक्त कोशिश का एक मकसद एशिया के वर्तमान इतिहास से अर्जित शिक्षाओं के महत्व को कम करना भी है।"11 उन्होंने आगे लिखा है “ओरिएन्टलिज्म को जितना प्रचार मिला है, वह उसके अकादमिक महत्त्व के कारण नहीं बल्कि इसलिए है कि उसने पश्चिम को वह सैद्धान्तिक हथियार उपलब्ध करा दिया है जिसके जरिए वह समाजवाद पर अपना आक्रमण लगातार बनाये रख सके। साथ ही यह भी दिखा सके कि हरतरह से पश्चिम जीवन शैली' ही सर्वोत्तम जीवन-शैली है।"12
आज के उत्तरऔपनिवेशिक भूमंडलीय पूँजीवाद की सफलता इस बात में नहीं है कि वह अपने असली शोषणकारी रूप को छिपाकर किसी उदार समाजव्यवस्था को ढोंग करता है बल्कि इस बात में है कि वह यथास्थितिवाद के किसी विकल्प को ही नहीं, ऐसे किसी विचार की संभावना को ही समाप्त कर देता है। वहाँ सफलता का सीधा मतलब है, प्रतिरोध के अंतिम स्वर तक की विदाई। इसे विडंबना ही कहा जायेगा कि समाज की जिन शक्तियों ने महज दो-ढाई सौ वर्ष पहले राजशाही एवं चर्च