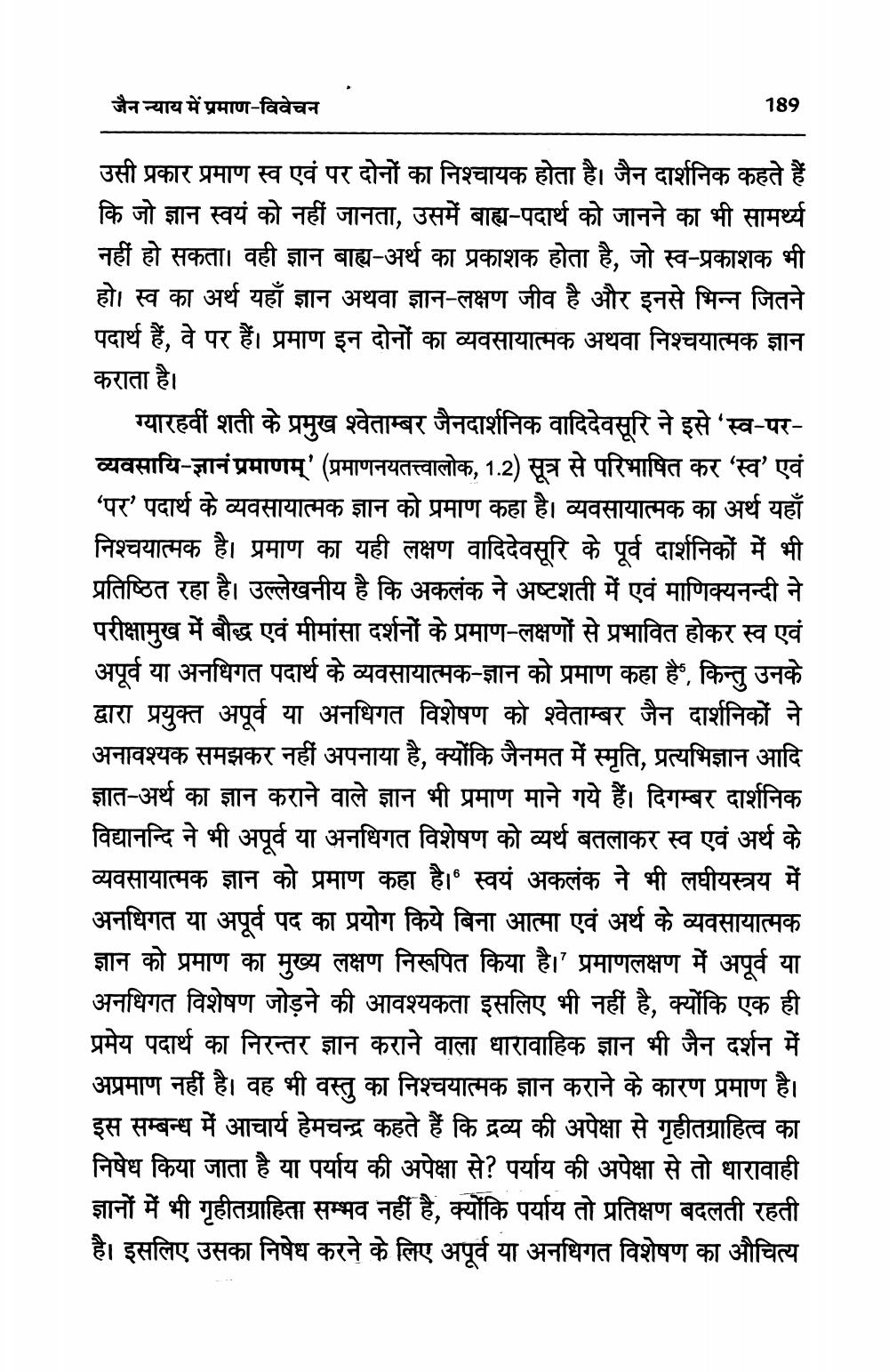________________
जैन न्याय में प्रमाण-विवेचन ।
189
उसी प्रकार प्रमाण स्व एवं पर दोनों का निश्चायक होता है। जैन दार्शनिक कहते हैं कि जो ज्ञान स्वयं को नहीं जानता, उसमें बाह्य-पदार्थ को जानने का भी सामर्थ्य नहीं हो सकता। वही ज्ञान बाह्य-अर्थ का प्रकाशक होता है, जो स्व-प्रकाशक भी हो। स्व का अर्थ यहाँ ज्ञान अथवा ज्ञान-लक्षण जीव है और इनसे भिन्न जितने पदार्थ हैं, वे पर हैं। प्रमाण इन दोनों का व्यवसायात्मक अथवा निश्चयात्मक ज्ञान कराता है।
ग्यारहवीं शती के प्रमुख श्वेताम्बर जैनदार्शनिक वादिदेवसूरि ने इसे 'स्व-परव्यवसायि-ज्ञानं प्रमाणम्' (प्रमाणनयतत्त्वालोक, 1.2) सूत्र से परिभाषित कर 'स्व' एवं 'पर' पदार्थ के व्यवसायात्मक ज्ञान को प्रमाण कहा है। व्यवसायात्मक का अर्थ यहाँ निश्चयात्मक है। प्रमाण का यही लक्षण वादिदेवसूरि के पूर्व दार्शनिकों में भी प्रतिष्ठित रहा है। उल्लेखनीय है कि अकलंक ने अष्टशती में एवं माणिक्यनन्दी ने परीक्षामुख में बौद्ध एवं मीमांसा दर्शनों के प्रमाण-लक्षणों से प्रभावित होकर स्व एवं अपूर्व या अनधिगत पदार्थ के व्यवसायात्मक-ज्ञान को प्रमाण कहा है, किन्तु उनके द्वारा प्रयुक्त अपूर्व या अनधिगत विशेषण को श्वेताम्बर जैन दार्शनिकों ने अनावश्यक समझकर नहीं अपनाया है, क्योंकि जैनमत में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञात-अर्थ का ज्ञान कराने वाले ज्ञान भी प्रमाण माने गये हैं। दिगम्बर दार्शनिक विद्यानन्दि ने भी अपूर्व या अनधिगत विशेषण को व्यर्थ बतलाकर स्व एवं अर्थ के व्यवसायात्मक ज्ञान को प्रमाण कहा है। स्वयं अकलंक ने भी लघीयस्त्रय में अनधिगत या अपूर्व पद का प्रयोग किये बिना आत्मा एवं अर्थ के व्यवसायात्मक ज्ञान को प्रमाण का मुख्य लक्षण निरूपित किया है।' प्रमाणलक्षण में अपूर्व या अनधिगत विशेषण जोड़ने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है, क्योंकि एक ही प्रमेय पदार्थ का निरन्तर ज्ञान कराने वाला धारावाहिक ज्ञान भी जैन दर्शन में अप्रमाण नहीं है। वह भी वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान कराने के कारण प्रमाण है। इस सम्बन्ध में आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं कि द्रव्य की अपेक्षा से गृहीतग्राहित्व का निषेध किया जाता है या पर्याय की अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से तो धारावाही ज्ञानों में भी गृहीतग्राहिता सम्भव नहीं है, क्योंकि पर्याय तो प्रतिक्षण बदलती रहती है। इसलिए उसका निषेध करने के लिए अपूर्व या अनधिगत विशेषण का औचित्य