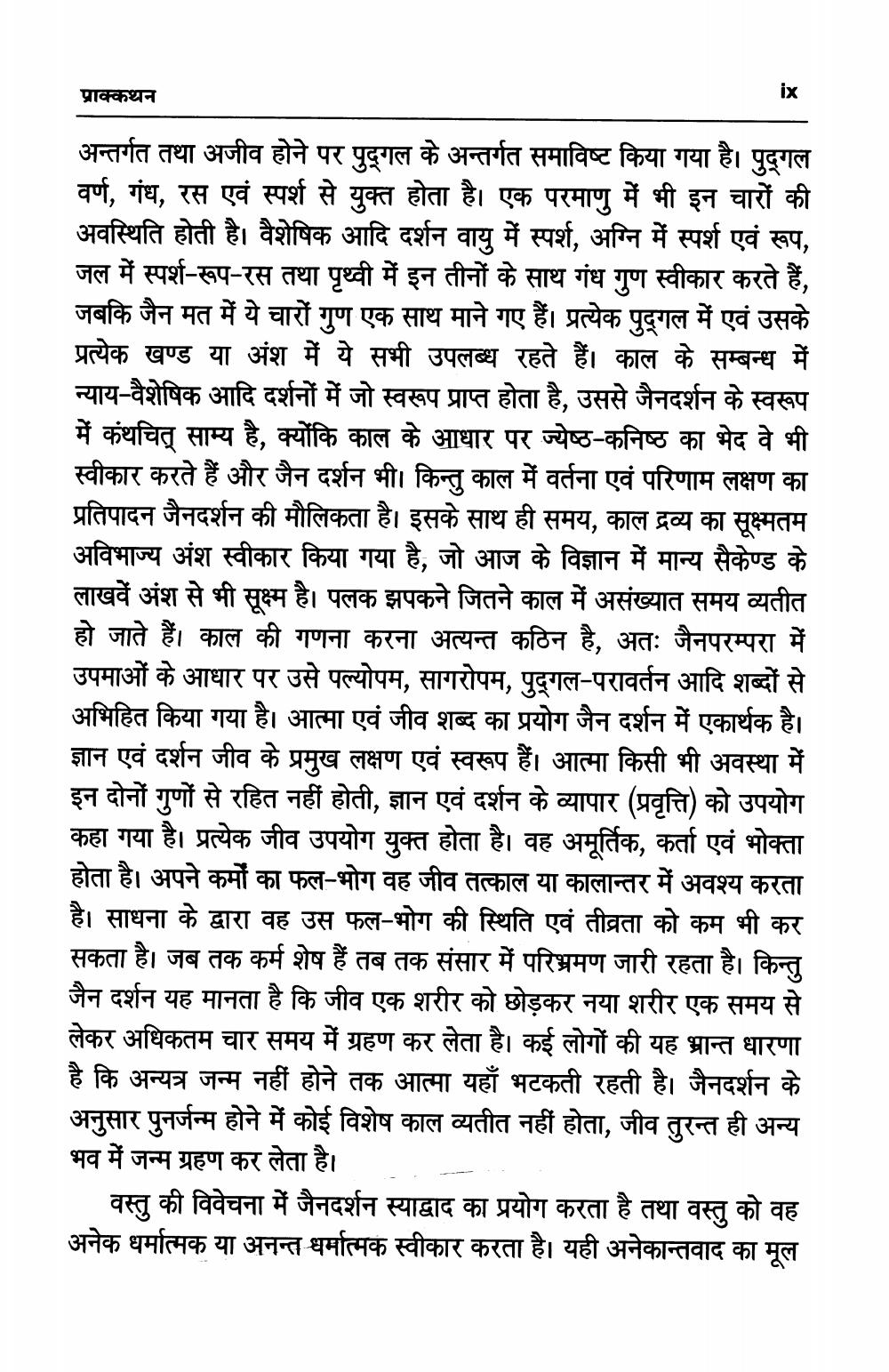________________
प्राक्कथन
अन्तर्गत तथा अजीव होने पर पुद्गल के अन्तर्गत समाविष्ट किया गया है। पुद्गल वर्ण, गंध, रस एवं स्पर्श से युक्त होता है। एक परमाणु में भी इन चारों की अवस्थिति होती है। वैशेषिक आदि दर्शन वायु में स्पर्श, अग्नि में स्पर्श एवं रूप, जल में स्पर्श-रूप-रस तथा पृथ्वी में इन तीनों के साथ गंध गुण स्वीकार करते हैं, जबकि जैन मत में ये चारों गुण एक साथ माने गए हैं। प्रत्येक पुद्गल में एवं उसके प्रत्येक खण्ड या अंश में ये सभी उपलब्ध रहते हैं। काल के सम्बन्ध में न्याय-वैशेषिक आदि दर्शनों में जो स्वरूप प्राप्त होता है, उससे जैनदर्शन के स्वरूप में कंथचित् साम्य है, क्योंकि काल के आधार पर ज्येष्ठ-कनिष्ठ का भेद वे भी स्वीकार करते हैं और जैन दर्शन भी। किन्तु काल में वर्तना एवं परिणाम लक्षण का प्रतिपादन जैनदर्शन की मौलिकता है। इसके साथ ही समय, काल द्रव्य का सूक्ष्मतम अविभाज्य अंश स्वीकार किया गया है, जो आज के विज्ञान में मान्य सैकेण्ड के लाखवें अंश से भी सक्ष्म है। पलक झपकने जितने काल में असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं। काल की गणना करना अत्यन्त कठिन है, अतः जैनपरम्परा में उपमाओं के आधार पर उसे पल्योपम, सागरोपम, पुद्गल-परावर्तन आदि शब्दों से अभिहित किया गया है। आत्मा एवं जीव शब्द का प्रयोग जैन दर्शन में एकार्थक है। ज्ञान एवं दर्शन जीव के प्रमुख लक्षण एवं स्वरूप हैं। आत्मा किसी भी अवस्था में इन दोनों गुणों से रहित नहीं होती, ज्ञान एवं दर्शन के व्यापार (प्रवृत्ति) को उपयोग कहा गया है। प्रत्येक जीव उपयोग युक्त होता है। वह अमूर्तिक, कर्ता एवं भोक्ता होता है। अपने कर्मों का फल-भोग वह जीव तत्काल या कालान्तर में अवश्य करता है। साधना के द्वारा वह उस फल-भोग की स्थिति एवं तीव्रता को कम भी कर सकता है। जब तक कर्म शेष हैं तब तक संसार में परिभ्रमण जारी रहता है। किन्तु जैन दर्शन यह मानता है कि जीव एक शरीर को छोड़कर नया शरीर एक समय से लेकर अधिकतम चार समय में ग्रहण कर लेता है। कई लोगों की यह भ्रान्त धारणा है कि अन्यत्र जन्म नहीं होने तक आत्मा यहाँ भटकती रहती है। जैनदर्शन के अनुसार पुनर्जन्म होने में कोई विशेष काल व्यतीत नहीं होता, जीव तुरन्त ही अन्य भव में जन्म ग्रहण कर लेता है।
वस्तु की विवेचना में जैनदर्शन स्याद्वाद का प्रयोग करता है तथा वस्तु को वह अनेक धर्मात्मक या अनन्त धर्मात्मक स्वीकार करता है। यही अनेकान्तवाद का मूल