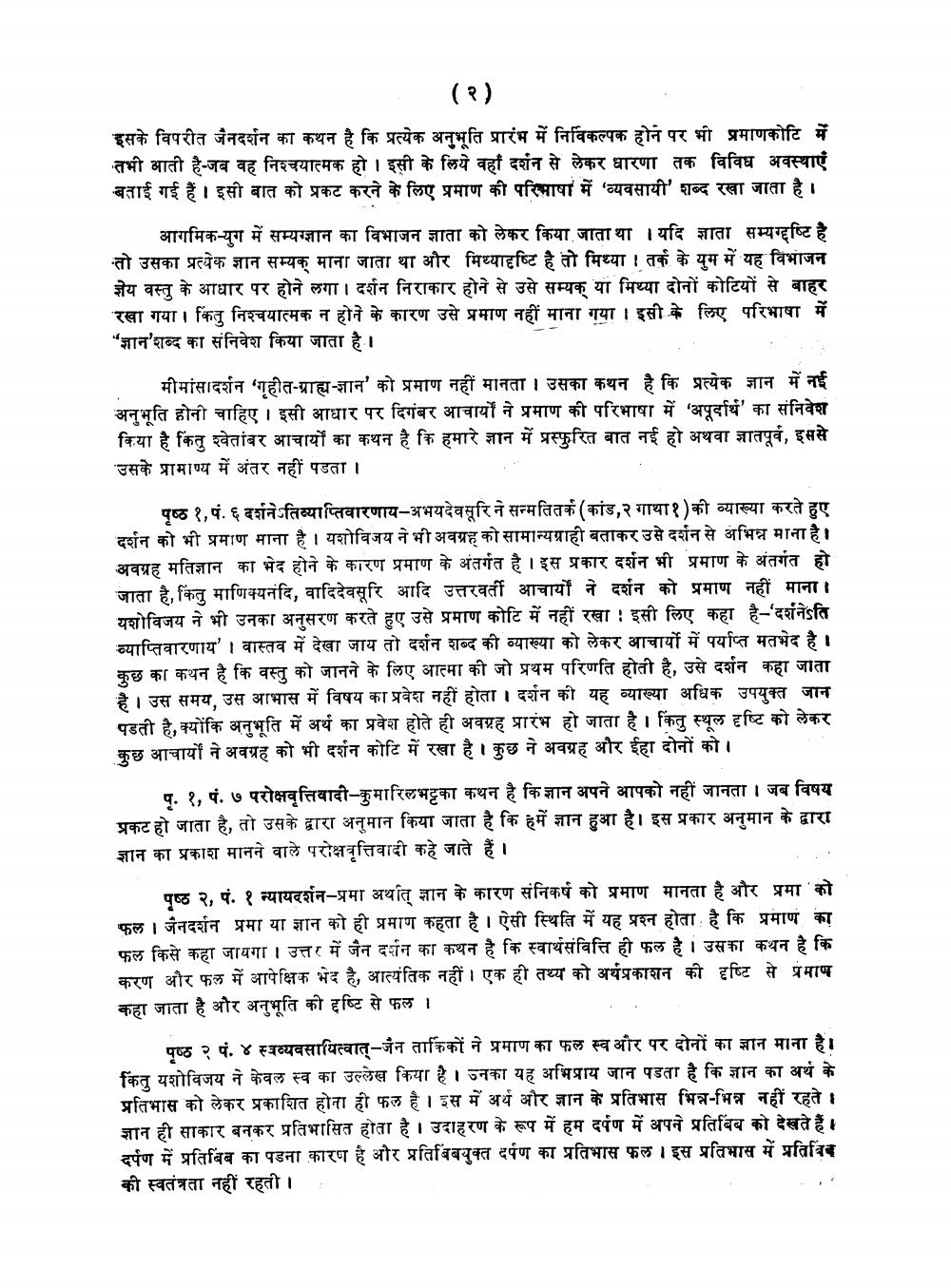________________
(२)
इसके विपरीत जैनदर्शन का कथन है कि प्रत्येक अनुभूति प्रारंभ में निर्विकल्पक होने पर भी प्रमाणकोटि में तभी आती है-जब वह निश्चयात्मक हो । इसी के लिये वहाँ दर्शन से लेकर धारणा तक विविध अवस्थाएं बताई गई हैं। इसी बात को प्रकट करने के लिए प्रमाण की परिभाषा में 'व्यवसायी' शब्द रखा जाता है।
आगमिक-युग में सम्यग्ज्ञान का विभाजन ज्ञाता को लेकर किया जाता था । यदि ज्ञाता सम्यग्दृष्टि है तो उसका प्रत्येक ज्ञान सम्यक् माना जाता था और मिथ्यादृष्टि है तो मिथ्या । तर्क के युग में यह विभाजन ज्ञेय वस्तु के आधार पर होने लगा। दर्शन निराकार होने से उसे सम्यक् या मिथ्या दोनों कोटियों से बाहर रखा गया। किंतु निश्चयात्मक न होने के कारण उसे प्रमाण नहीं माना गया। इसी के लिए परिभाषा में "ज्ञान' शब्द का संनिवेश किया जाता है।
- मीमांसादर्शन 'गृहीत-ग्राह्य-ज्ञान' को प्रमाण नहीं मानता। उसका कथन है कि प्रत्येक ज्ञान में नई अनुभूति होनी चाहिए । इसी आधार पर दिगंबर आचार्यों ने प्रमाण की परिभाषा में 'अपूर्वार्थ' का संनिवेश किया है किंतु श्वेतांबर आचार्यों का कथन है कि हमारे ज्ञान में प्रस्फुरित बात नई हो अथवा ज्ञातपूर्व, इससे उसके प्रामाण्य में अंतर नहीं पड़ता।
पृष्ठ १,पं. ६ दर्शने तिव्याप्तिवारणाय-अभयदेवसूरि ने सन्मतितर्क (कांड,२ गाथा१)की व्याख्या करते हुए दर्शन को भी प्रमाण माना है। यशोविजय ने भी अवग्रह को सामान्यग्राही बताकर उसे दर्शन से अभिन्न माना है। अवग्रह मतिज्ञान का भेद होने के कारण प्रमाण के अंतर्गत है । इस प्रकार दर्शन भी प्रमाण के अंतर्गत हो जाता है, किंतु माणिक्यनंदि, वादिदेवसूरि आदि उत्तरवर्ती आचार्यों ने दर्शन को प्रमाण नहीं माना। यशोविजय ने भी उनका अनुसरण करते हुए उसे प्रमाण कोटि में नहीं रखा ! इसी लिए कहा है-'दर्शनेऽति व्याप्तिवारणाय' । वास्तव में देखा जाय तो दर्शन शब्द की व्याख्या को लेकर आचार्यों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ का कथन है कि वस्तु को जानने के लिए आत्मा की जो प्रथम परिणति होती है, उसे दर्शन कहा जाता है। उस समय, उस आभास में विषय का प्रवेश नहीं होता। दर्शन की यह व्याख्या अधिक उपयुक्त जान पडती है, क्योंकि अनुभूति में अर्थ का प्रवेश होते ही अवग्रह प्रारंभ हो जाता है। किंतु स्थूल दृष्टि को लेकर कुछ आचार्यों ने अवग्रह को भी दर्शन कोटि में रखा है। कुछ ने अवग्रह और ईहा दोनों को।
पृ. १, पं. ७ परोक्षवृत्तिवादी-कुमारिल भट्टका कथन है कि ज्ञान अपने आपको नहीं जानता। जब विषय प्रकट हो जाता है, तो उसके द्वारा अनुमान किया जाता है कि हमें ज्ञान हुआ है। इस प्रकार अनुमान के द्वारा ज्ञान का प्रकाश मानने वाले परोक्षवृत्तिवादी कहे जाते हैं।
पृष्ठ २, पं. १ न्यायदर्शन-प्रमा अर्थात् ज्ञान के कारण संनिकर्ष को प्रमाण मानता है और प्रमा को फल । जनदर्शन प्रमा या ज्ञान को ही प्रमाण कहता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न होता है कि प्रमाण का फल किसे कहा जायगा। उत्तर में जैन दर्शन का कथन है कि स्वार्थसंवित्ति ही फल है। उसका कथन है कि करण और फल में आपेक्षिक भेद है, आत्यंतिक नहीं। एक ही तथ्य को अर्थप्रकाशन की दृष्टि से प्रमाण कहा जाता है और अनुभूति को दृष्टि से फल ।
__पृष्ठ २ पं. ४ स्वव्यवसायित्वात्-जैन तार्किकों ने प्रमाण का फल स्व और पर दोनों का ज्ञान माना है। किंतु यशोविजय ने केवल स्व का उल्लेख किया है। उनका यह अभिप्राय जान पडता है कि ज्ञान का अर्थ के प्रतिभास को लेकर प्रकाशित होना ही फल है। इस में अर्थ और ज्ञान के प्रतिभास भिन्न-भिन्न नहीं रहते। ज्ञान ही साकार बनकर प्रतिभासित होता है । उदाहरण के रूप में हम दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब का पडना कारण है और प्रतिबिंबयुक्त दर्पण का प्रतिभास फल । इस प्रतिभास में प्रतिबिंब की स्वतंत्रता नहीं रहती।