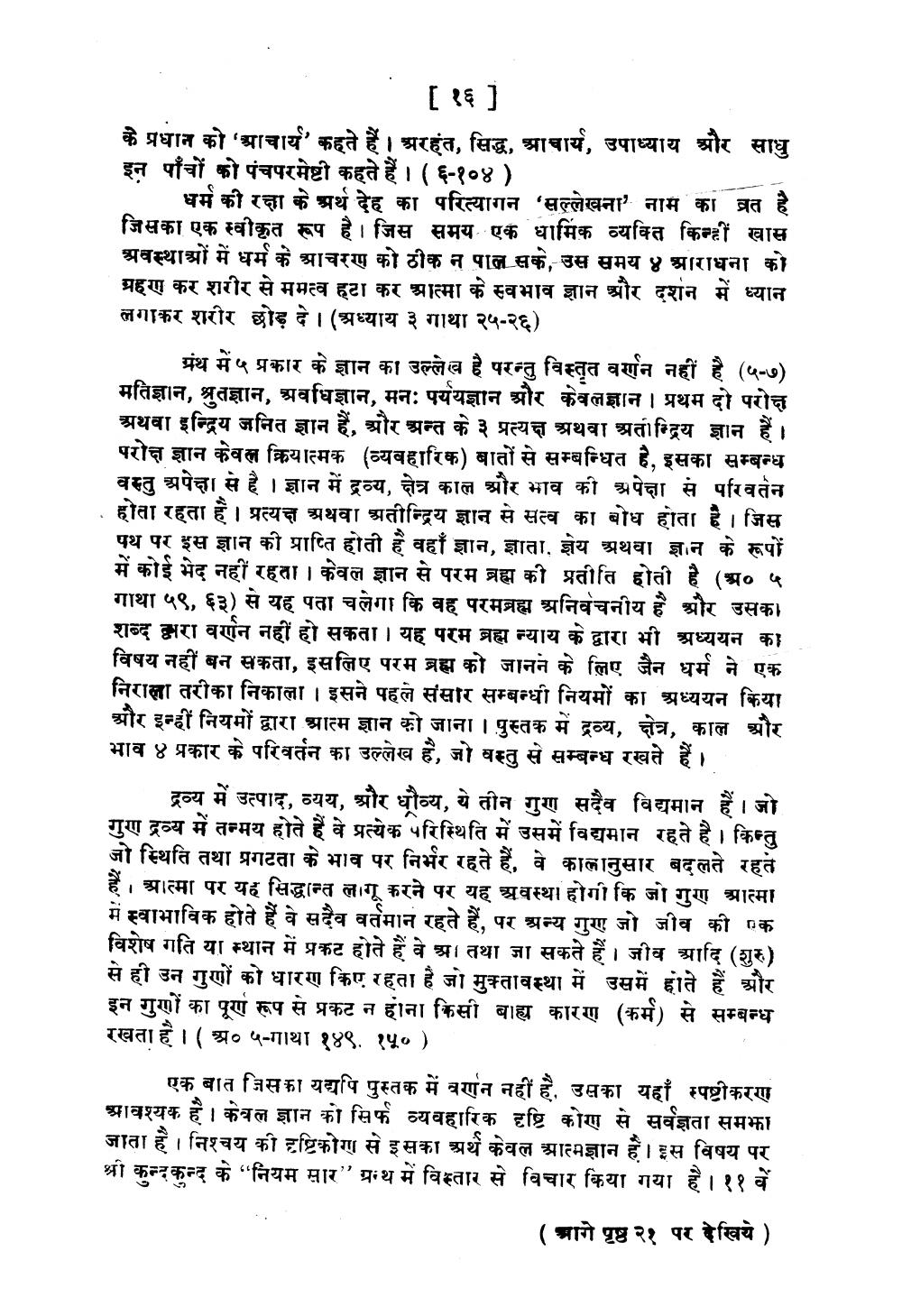________________
[१६] के प्रधान को 'आचार्य' कहते हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पाँचों को पंचपरमेष्टी कहते हैं । ( ६-१०४)
धर्म की रक्षा के अर्थ देह का परित्यागन 'सल्लेखना' नाम का व्रत है जिसका एक स्वीकृत रूप है। जिस समय एक धार्मिक व्यक्ति किन्हीं खास अवस्थाओं में धर्म के आचरण को ठीक न पाल सके, उस समय ४ आराधना को ग्रहण कर शरीर से ममत्व हटा कर आत्मा के स्वभाव ज्ञान और दर्शन में ध्यान लगाकर शरीर छोड़ दे । (अध्याय ३ गाथा २५-२६)
ग्रंथ में ५ प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है परन्तु विस्तृत वर्णन नहीं है (५-७) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पययज्ञान और केवलज्ञान । प्रथम दो परोक्ष अथवा इन्द्रिय जनित ज्ञान हैं, और अन्त के ३ प्रत्यक्ष अथवा अतीन्द्रिय ज्ञान हैं। परोक्ष ज्ञान केवल क्रियात्मक (व्यवहारिक) बातों से सम्बन्धित है, इसका सम्बन्ध वस्तु अपेक्षा से है । ज्ञान में द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा सं परिवतेन होता रहता है । प्रत्यक्ष अथवा अतीन्द्रिय ज्ञान से सत्व का बोध होता है । जिस पथ पर इस ज्ञान की प्राप्ति होती है वहाँ ज्ञान, ज्ञाता. ज्ञेय अथवा ज्ञान के रूपों में कोई भेद नहीं रहता। केवल ज्ञान से परम ब्रह्म की प्रतीति होती है (अ० ५ गाथा ५९, ६३) से यह पता चलेगा कि वह परमब्रह्म अनिर्वचनीय है और उसकी शब्द द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। यह परम ब्रह्म न्याय के द्वारा भी अध्ययन का विषय नहीं बन सकता, इसलिए परम ब्रह्म को जानने के लिए जैन धर्म ने एक निराला तरीका निकाला। इसने पहले संसार सम्बन्धी नियमों का अध्ययन किया
और इन्हीं नियमों द्वारा आत्म ज्ञान को जाना । पुस्तक में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ४ प्रकार के परिवर्तन का उल्लेख है, जो वस्तु से सम्बन्ध रखते हैं।
द्रव्य में उत्पाद, व्यय, और धौव्य, ये तीन गुण सदैव विद्यमान हैं । जो गुण द्रव्य में तन्मय होते हैं वे प्रत्येक परिस्थिति में उसमें विद्यमान रहते है। किन्तु जो स्थिति तथा प्रगटता के भाव पर निर्भर रहते हैं, वे कालानुसार बदलते रहते हैं। आत्मा पर यह सिद्धान्त लागू करने पर यह अवस्था होगी कि जो गुण आत्मा में स्वाभाविक होते हैं वे सदैव वर्तमान रहते हैं, पर अन्य गुण जो जीव की एक विशेष गति या स्थान में प्रकट होते हैं वे अा तथा जा सकते हैं। जीव आदि (शुरु) से ही उन गुणों को धारण किए रहता है जो मुक्तावस्था में उसमें होते हैं और इन गुणों का पूर्ण रूप से प्रकट न होना किसी बाह्य कारण (कर्म) से सम्बन्ध रखता है । ( अ० ५-गाथा १४९. १५० )
एक बात जिसका यद्यपि पुस्तक में वर्णन नहीं है, उसका यहाँ स्पष्टीकरण आवश्यक है। केवल ज्ञान को सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि कोण से सर्वज्ञता समझा जाता है। निश्चय की दृष्टिकोगा से इसका अर्थ केवल आत्मज्ञान है। इस विषय पर श्री कुन्दकुन्द के "नियम सार' ग्रन्थ में विस्तार से विचार किया गया है। ११ वें
(भागे पृष्ठ २१ पर देखिये )