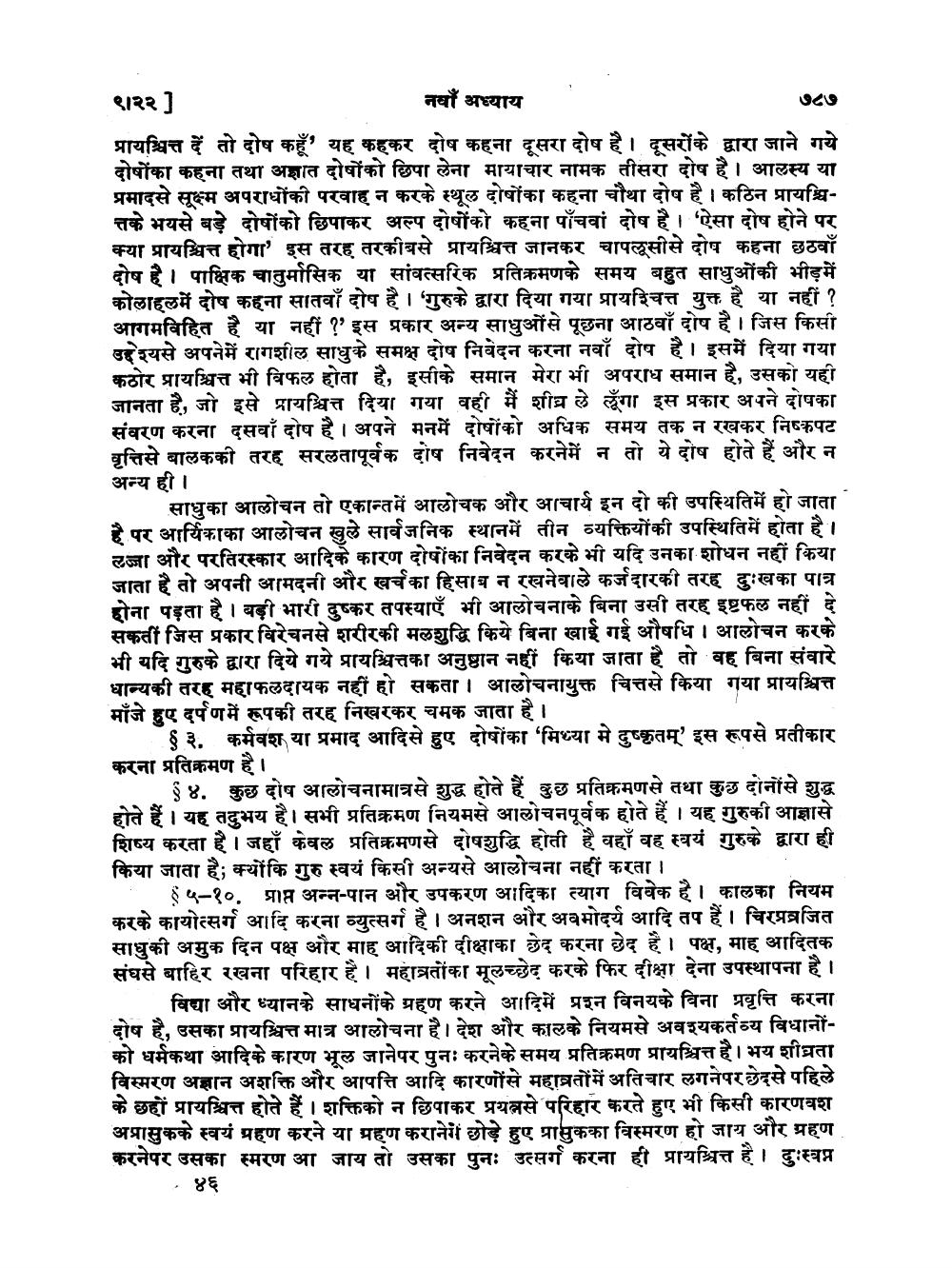________________
नवाँ अध्याय
७८७
९।२२]
प्रायश्चित्त दें तो दोष कहूँ' यह कहकर दोष कहना दूसरा दोष है। दूसरोंके द्वारा जाने गये दोषों का कहना तथा अज्ञात दोषोंको छिपा लेना मायाचार नामक तीसरा दोष है। आलस्य या प्रमादसे सूक्ष्म अपराधोंकी परवाह न करके स्थूल दोषोंका कहना चौथा दोष है । कठिन प्रायश्चिके भय से बड़े दोषों को छिपाकर अल्प दोषोंको कहना पाँचवां दोष है । 'ऐसा दोष होने पर क्या प्रायश्चित्त होगा' इस तरह तरकीब से प्रायश्चित्त जानकर चापलूसीसे दोष कहना छठवाँ दोष है। पाक्षिक चातुर्मासिक या सांवत्सरिक प्रतिक्रमणके समय बहुत साधुओंकी भीड़ में कोलाहलमें दोष कहना सातवाँ दोष है । 'गुरुके द्वारा दिया गया प्रायश्चित्त युक्त है या नहीं ? आगमविहित है या नहीं ?' इस प्रकार अन्य साधुओं से पूछना आठवाँ दोष है। जिस किसी उद्देश्यसे अपने में रागशील साधुके समक्ष दोष निवेदन करना नवाँ दोष है । इसमें दिया गया कठोर प्रायश्चित्त भी विफल होता है, इसीके समान मेरा भी अपराध समान है, उसको यही जानता है, जो इसे प्रायश्चित्त दिया गया वही मैं शीघ्र ले लूँगा इस प्रकार अपने दोपका संवरण करना दसवाँ दोष है । अपने मनमें दोषोंको अधिक समय तक न रखकर निष्कपट वृत्तिसे बालककी तरह सरलतापूर्वक दोष निवेदन करनेमें न तो ये दोष होते हैं और न अन्य ही ।
साधुका आलोचन तो एकान्त में आलोचक और आचार्य इन दो की उपस्थिति में हो जाता है पर आर्यिका का आलोचन खुले सार्वजनिक स्थानमें तीन व्यक्तियोंकी उपस्थिति में होता है । लज्जा और परतिरस्कार आदिके कारण दोषोंका निवेदन करके भी यदि उनका शोधन नहीं किया जाता है तो अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब न रखनेवाले कर्जदारकी तरह दुःखका पात्र होना पड़ता । बड़ी भारी दुष्कर तपस्याएँ भी आलोचनाके बिना उसी तरह इष्टफल नहीं दे सकतीं जिस प्रकार विरेचनसे शरीर की मलशुद्धि किये बिना खाई गई औषधि । आलोचन करके भी यदि गुरुके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तका अनुष्ठान नहीं किया जाता है तो वह बिना संवारे धान्यकी तरह महाफलदायक नहीं हो सकता । आलोचनायुक्त चित्तसे किया गया प्रायश्चित्त माँ हुए दर्पण में रूपकी तरह निखरकर चमक जाता है ।
६३. कर्मवश या प्रमाद आदिसे हुए दोषोंका 'मिध्या मे दुष्कृतम्' इस रूपसे प्रतीकार करना प्रतिक्रमण है ।
१४. कुछ दोष आलोचनामात्र से शुद्ध होते हैं कुछ प्रतिक्रमण से तथा कुछ दोनों से शुद्ध होते हैं । यह तदुभय है । सभी प्रतिक्रमण नियमसे आलोचनपूर्वक होते हैं । यह गुरुकी आज्ञासे शिष्य करता है । जहाँ केवल प्रतिक्रमणसे दोषशुद्धि होती है वहाँ वह स्वयं गुरुके द्वारा ही किया जाता है; क्योंकि गुरु स्वयं किसी अन्यसे आलोचना नहीं करता ।
१५-१०. प्राप्त अन्न-पान और उपकरण आदिका त्याग विवेक है । कालका नियम करके कायोत्सर्ग आदि करना व्युत्सर्ग है । अनशन और अवमोदर्य आदि तप हैं । चिरप्रव्रजित साधुकी अमुक दिन पक्ष और माह आदिकी दीक्षाका छेद करना छेद हैं। पक्ष, माह आदितक संघसे बाहिर रखना परिहार है । महात्रतों का मूलच्छेद करके फिर दीक्षा देना उपस्थापना है ।
विद्या और ध्यानके साधनोंके ग्रहण करने आदिमें प्रश्न विनयके विना प्रवृत्ति करना दोष है, उसका प्रायश्चित्त मात्र आलोचना है। देश और कालके नियमसे अवश्यकर्तव्य विधानोंको धर्मकथा आदिके कारण भूल जानेपर पुनः करने के समय प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है । भय शीघ्रता विस्मरण अज्ञान अशक्ति और आपत्ति आदि कारणोंसे महाव्रतों में अतिचार लगनेपर छेद से पहिले के छहीं प्रायश्चित्त होते हैं। शक्तिको न छिपाकर प्रयत्नसे परिहार करते हुए भी किसी कारणवश अप्राकके स्वयं ग्रहण करने या ग्रहण करानेगें छोड़े हुए प्राकका विस्मरण हो जाय और ग्रहण करनेपर उसका स्मरण आ जाय तो उसका पुनः उत्सर्ग करना ही प्रायश्रित है । दुःस्व
४६