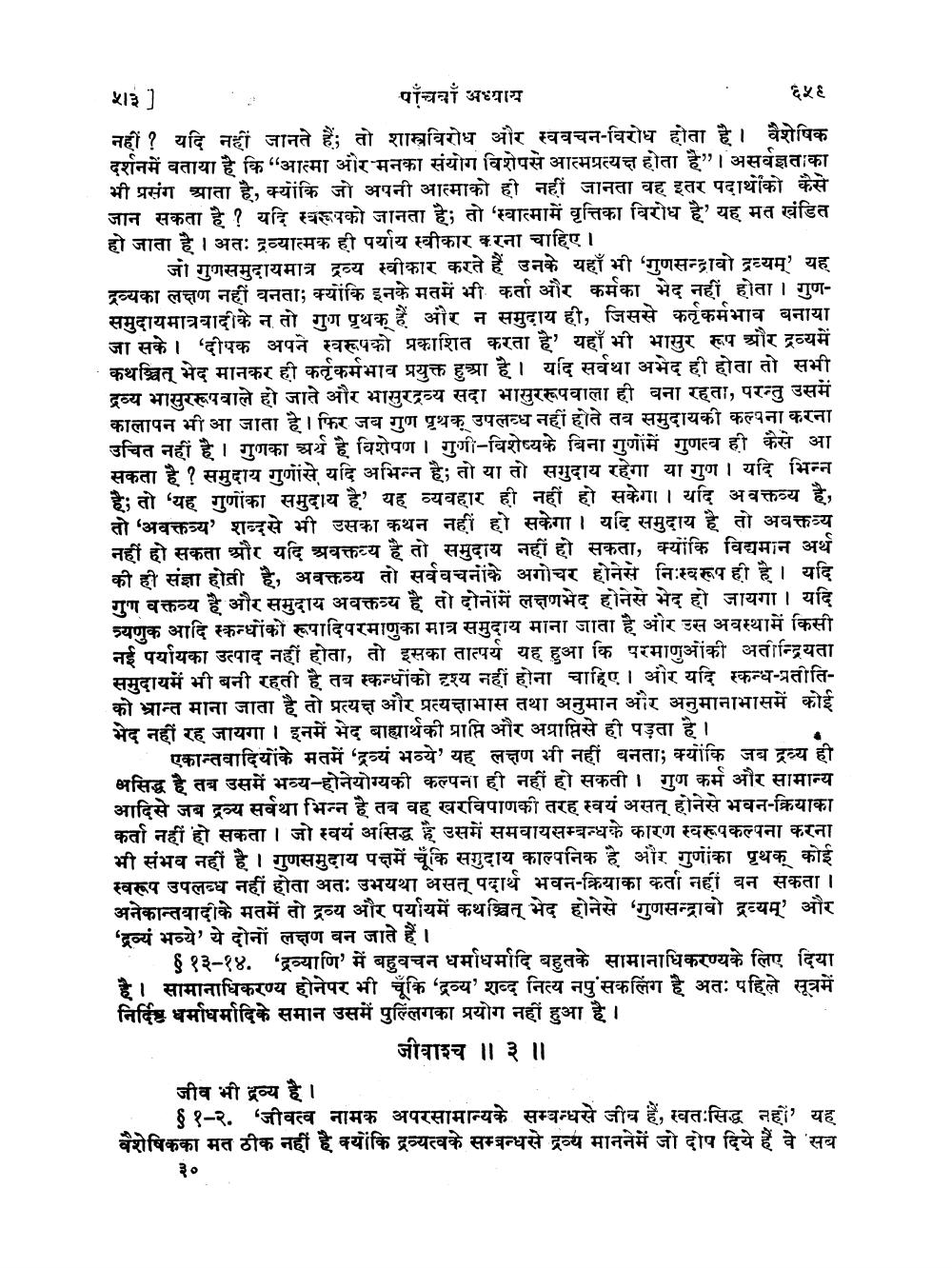________________
श३] पाँचवाँ अध्याय
६५६ नहीं ? यदि नहीं जानते हैं; तो शास्त्रविरोध और स्ववचन-विरोध होता है। वैशेषिक दर्शनमें बताया है कि "आत्मा और मनका संयोग विशेपसे आत्मप्रत्यक्ष होता है"। असर्वज्ञताका
संग आता है, क्योंकि जो अपनी आत्माको ही नहीं जानता वह इतर पदार्थोंको कैसे जान सकता है ? यदि स्वरूपको जानता है; तो 'स्वात्मामें वृत्तिका विरोध है' यह मत खंडित हो जाता है । अतः द्रव्यात्मक ही पर्याय स्वीकार करना चाहिए।
जो गुणसमुदायमात्र द्रव्य स्वीकार करते हैं उनके यहाँ भी 'गुणसन्द्रावो द्रव्यम्' यह द्रव्यका लक्षण नहीं वनता; क्योंकि इनके मतमें भी कर्ता और कर्मका भेद नहीं होता। गुणसमुदायमात्रवादीके न तो गुण पृथक् हैं और न समुदाय ही, जिससे कर्तृकर्मभाव बनाया जा सके। 'दीपक अपने स्वरूपको प्रकाशित करता है' यहाँ भी भासुर रूप और द्रव्यमें कथञ्चित् भेद मानकर ही कर्तृकर्मभाव प्रयुक्त हुआ है। यदि सर्वथा अभेद ही होता तो सभी द्रव्य भासुररूपवाले हो जाते और भासुरद्रव्य सदा भासुररूपवाला ही बना रहता, परन्तु उसमें कालापन भी आ जाता है। फिर जब गुण पृथक उपलब्ध नहीं होते तव समुदायकी कल्पना करना उचित नहीं है। गुणका अर्थ है विशेपण । गुणी-विशेष्यके बिना गुणोंमें गुणत्व ही कैसे आ सकता है ? समुदाय गुणांसे यदि अभिन्न है; तो या तो समुदाय रहेगा या गुण । यदि भिन्न है; तो 'यह गुणोंका समुदाय है' यह व्यवहार ही नहीं हो सकेगा। यदि अवक्तव्य है, तो 'अवक्तव्य' शब्दसे भी उसका कथन नहीं हो सकेगा। यदि समुदाय है तो अवक्तव्य नहीं हो सकता और यदि अवक्तव्य है तो समुदाय नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यमान अर्थ की ही संज्ञा होती है, अवक्तव्य तो सर्ववचनीके अगोचर होनेसे निःस्वरूप ही है। यदि गुण वक्तव्य है और समुदाय अवक्तव्य है तो दोनोंमें लक्षणभेद होनेसे भेद हो जायगा । यदि त्र्यणुक आदि स्कन्धोंको रूपादिपरमाणुका मात्र समुदाय माना जाता है और उस अवस्थामें किसी नई पर्यायका उत्पाद नहीं होता, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमाणुओंकी अतीन्द्रियता समुदायमें भी बनी रहती है तब स्कन्धोंको दृश्य नहीं होना चाहिए। और यदि स्कन्ध-प्रतीतिको भ्रान्त माना जाता है तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षाभास तथा अनुमान और अनुमानाभासमें कोई भेद नहीं रह जायगा। इनमें भेद बाह्यार्थकी प्राप्ति और अप्राप्तिसे ही पड़ता है।
एकान्तवादियोंके मतमें 'द्रव्यं भव्ये' यह लक्षण भी नहीं बनता; क्योंकि जब द्रव्य ही असिद्ध है तब उसमें भव्य-होनेयोग्यकी कल्पना ही नहीं हो सकती। गुण कर्म और सामान्य आदिसे जब द्रव्य सर्वथा भिन्न है तब वह खरविपाणकी तरह स्वयं असत् होनेसे भवन-क्रियाका कर्ता नहीं हो सकता। जो स्वयं असिद्ध है उसमें समवायसम्बन्धके कारण स्वरूपकल्पना करना भी संभव नहीं है। गुणसमुदाय पक्षमें चूँकि समुदाय काल्पनिक है और गुणोंका पृथक कोई स्वरूप उपलब्ध नहीं होता अतः उभयथा असत् पदाथे भवन-क्रियाका कर्ता नहीं बन सकता। अनेकान्तवादीके मतमें तो द्रव्य और पर्यायमें कथञ्चित् भेद होनेसे 'गुणसन्द्रावो द्रव्यम्' और 'द्रव्यं भव्ये' ये दोनों लक्षण बन जाते हैं।
१३-१४. 'द्रव्याणि' में बहुवचन धर्माधर्मादि बहुतके सामानाधिकरण्यके लिए दिया है। सामानाधिकरण्य होनेपर भी चूँकि 'द्रव्य' शब्द नित्य नपुसकलिंग है अतः पहिले सूत्र में निर्दिष्ट धर्माधर्मादिके समान उसमें पुल्लिगका प्रयोग नहीं हुआ है।
जीवाश्च ॥ ३ ॥ जीव भी द्रव्य है।
६१-२. 'जीवत्व नामक अपरसामान्यके सम्बन्धसे जीव हैं, स्वतःसिद्ध नहीं यह वैशेषिकका मत ठीक नहीं है क्योंकि द्रव्यत्वके सम्बन्धसे द्रव्य मानने में जो दोष दिये हैं वे 'सब