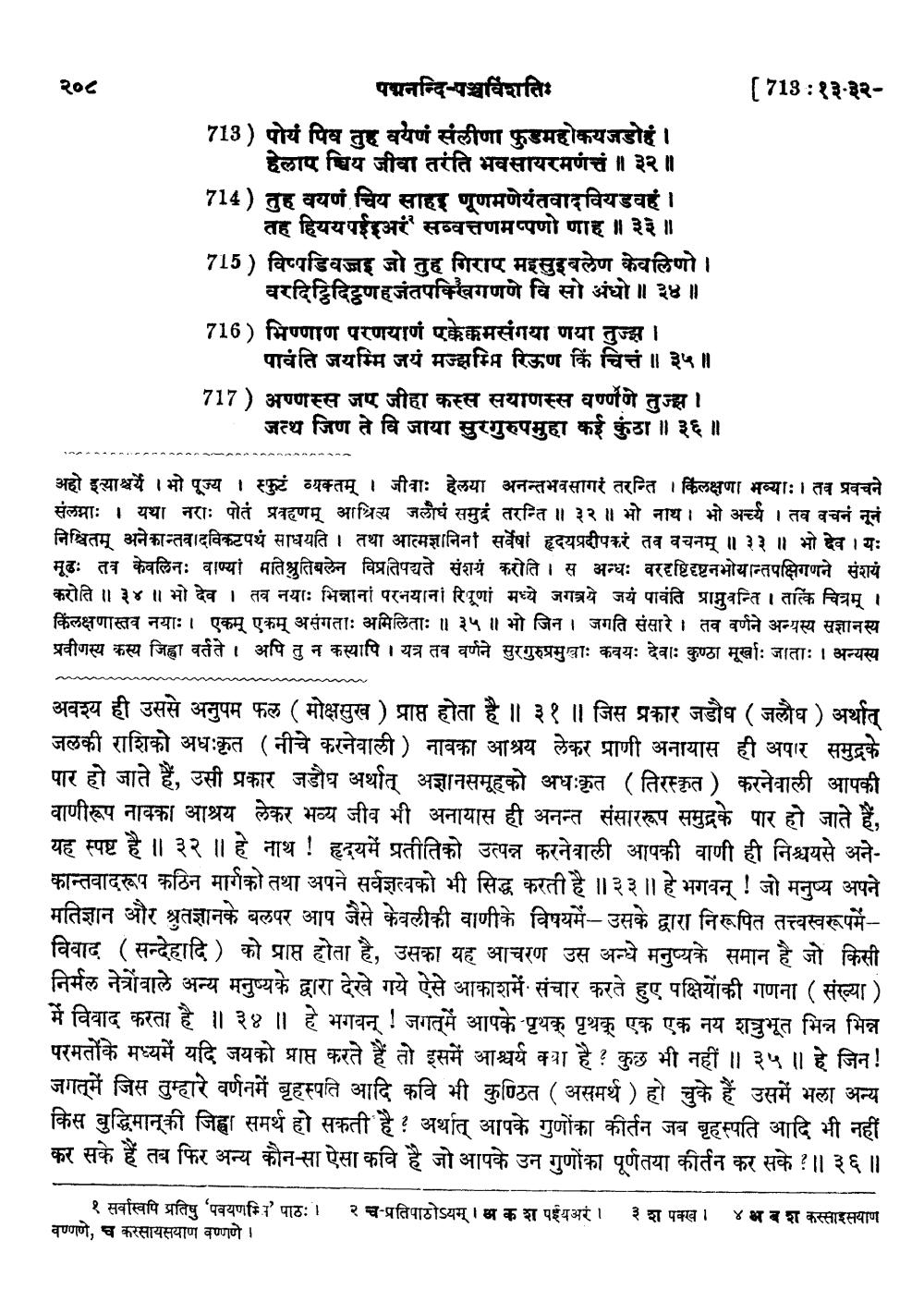________________
२०८
[718:१३-३२
पभनन्दि-पञ्चविंशतिः 713) पोयं पिव तुह वयणं संलीणा फुडमहोकयजडोहं ।
हेलाए चिय जीवा तरंति भवसायरमणत्तं ॥ ३२॥ 714) तुह वयणं चिय साहइ गृणमणेयंतवादवियडवहं ।
तह हिययपईइअरं' सव्वत्तणमप्पणो णाह ॥ ३३ ॥ 715) विपडिवजह जो तुह गिराए मइसुइवलेण केवलिणो।
वरदिट्ठिदिट्ठणहजंतपक्खिगणणे वि सो अंधो॥ ३४॥ 716) भिण्णाण परणयाणं एकेकमसंगया णया तुज्झ ।
पावंति जयम्मि जयं मज्झम्मि रिऊण किं चित्तं ॥ ३५ ॥ 717) अण्णस्स जए जीहा कस्स सयाणस्स वर्णणे तुज्झ ।
जत्थ जिण ते वि जाया सुरगुरुपमुहा कई कुंठा ॥ ३६ ॥
अहो इत्याश्चर्ये । भो पूज्य । स्फुटं व्यक्तम् । जीवाः हेलया अनन्तभवसागरं तरन्ति । किलक्षणा भव्याः । तव प्रवचने संलग्नाः । यथा नराः पोतं प्रवहणम् आश्रित्य जलौघं समुद्रं तरन्ति ॥ ३२॥ भो नाथ। भो अर्घ्य । तव वचनं नूनं निश्चितम अनेकान्तवादविकटपथं साधयति । तथा आत्मज्ञानिनां सर्वेषां हृदयप्रदीपकरं तव वचनम् ॥ ३३ ॥ भो देव । यः मढः तव केवलिनः वाण्यां मतिश्रतियलेन विप्रतिपद्यते संशयं करोति। स अन्धः वरदृष्टिदृष्टनभोयान्तपक्षिगणने संशयं करोति ॥ ३४ ॥ भो देव । तव नयाः भिन्नानां परनयानां रिपूणां मध्ये जगत्रये जयं पावंति प्राप्नुवन्ति । तत्किं चित्रम् । किंलक्षणास्तव नयाः। एकम् एकम् असंगताः अमिलिताः ॥ ३५ ॥ भो जिन । जगति संसारे। तव वर्णने अन्यस्य सज्ञानस्य प्रवीणस्य कस्य जिह्वा वर्तते । अपि तु न कस्यापि । यत्र तव वर्णने सुरगुरुप्रमुखाः कवयः देवाः कुण्ठा मूर्खाः जाताः । अन्यस्य
अवश्य ही उससे अनुपम फल ( मोक्षसुख ) प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार जडौष ( जलौघ ) अर्थात् जलकी राशिको अधःकृत (नीचे करनेवाली) नावका आश्रय लेकर प्राणी अनायास ही अपार समुद्रके पार हो जाते हैं, उसी प्रकार जडौघ अर्थात् अज्ञानसमूहको अधःकृत (तिरस्कृत) करनेवाली आपकी वाणीरूप नाक्का आश्रय लेकर भव्य जीव भी अनायास ही अनन्त संसाररूप समुद्रके पार हो जाते हैं, यह स्पष्ट है ॥ ३२ ॥ हे नाथ ! हृदयमें प्रतीतिको उत्पन्न करनेवाली आपकी वाणी ही निश्चयसे अने. कान्तवादरूप कठिन मार्गको तथा अपने सर्वज्ञत्वको भी सिद्ध करती है ॥३३॥ हे भगवन् ! जो मनुष्य अपने मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके बलपर आप जैसे केवलीकी वाणीके विषयमें- उसके द्वारा निरूपित तत्त्वस्वरूपमेंविवाद (सन्देहादि) को प्राप्त होता है, उसका यह आचरण उस अन्धे मनुष्यके समान है जो किसी निर्मल नेत्रोंवाले अन्य मनुष्यके द्वारा देखे गये ऐसे आकाशमें संचार करते हुए पक्षियोंकी गणना (संख्या) में विवाद करता है ॥ ३४ ॥ हे भगवन् ! जगत्में आपके पृथक् पृथक् एक एक नय शत्रुभूत भिन्न भिन्न परमतोंके मध्यमें यदि जयको प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है ? कुछ भी नहीं ॥ ३५ ॥ हे जिन! जगत्में जिस तुम्हारे वर्णनमें बृहस्पति आदि कवि भी कुण्ठित ( असमर्थ ) हो चुके हैं उसमें भला अन्य किस बुद्धिमान्की जिह्वा समर्थ हो सकती है ? अर्थात् आपके गुणोंका कीर्तन जब बृहस्पति आदि भी नहीं कर सके हैं तब फिर अन्य कौन-सा ऐसा कवि है जो आपके उन गुणोंका पूर्णतया कीर्तन कर सके ? ॥ ३६॥
२ च-प्रतिपाठोऽयम् ।
१ सर्वास्वपि प्रतिषु ‘पवयणमि' पाठः। वण्णणे, च करसायसयाण वण्णणे।
क श पईयअरं । ३श पक्ख । ४ भबश कस्साइसयाण