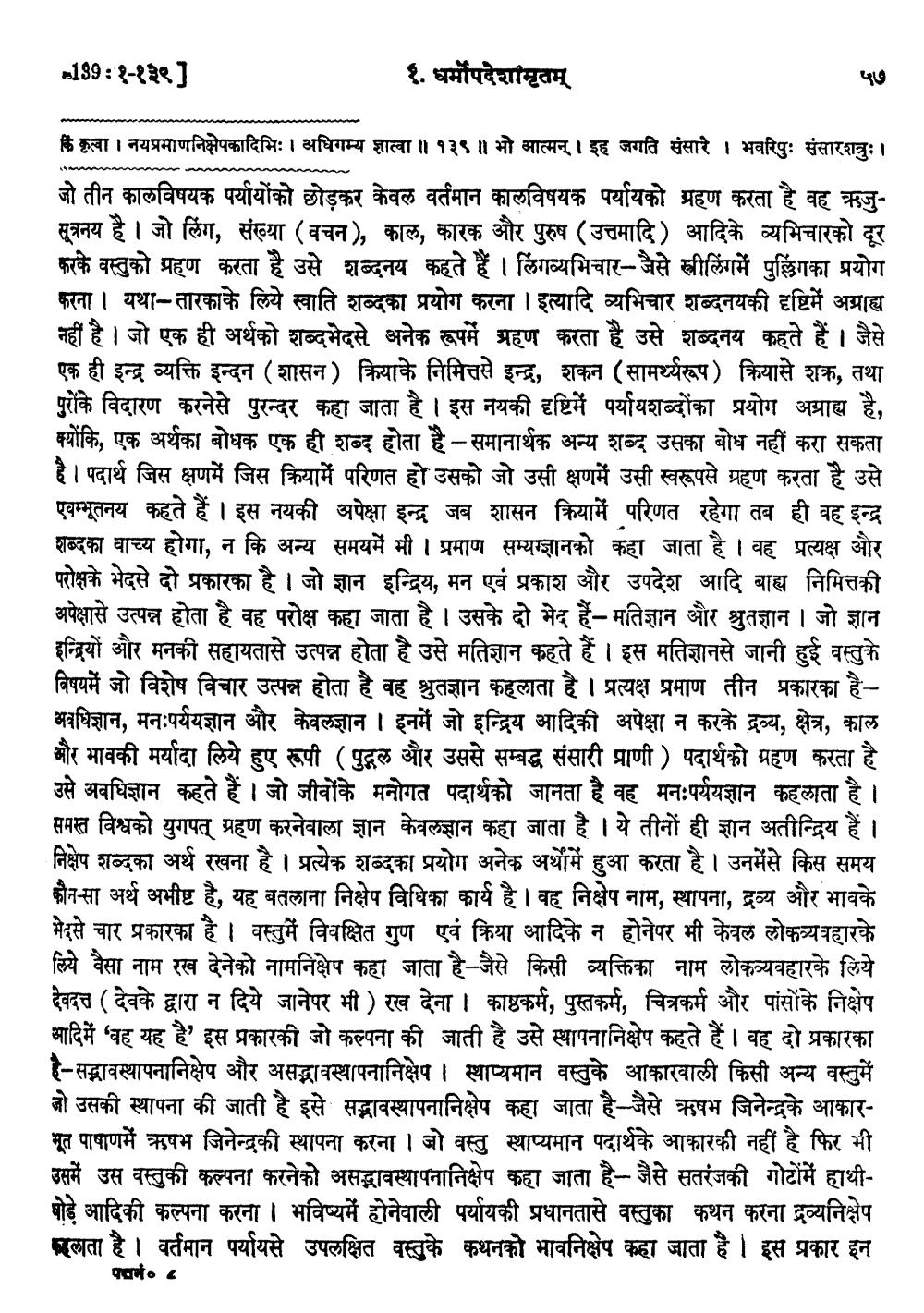________________
-139:१-१३९]
१. धर्मोपदेशामृतम्
किं कृत्वा । नयप्रमाणनिक्षेपकादिभिः । अधिगम्य ज्ञात्वा ॥ १३९ ॥ भो आत्मन् । इह जगति संसारे । भवरिपुः संसारशत्रुः । जो तीन कालविषयक पर्यायोंको छोड़कर केवल वर्तमान कालविषयक पर्यायको ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्रनय है । जो लिंग, संख्या (वचन), काल, कारक और पुरुष (उत्तमादि) आदिके व्यभिचारको दूर करके वस्तुको ग्रहण करता है उसे शब्दनय कहते हैं । लिंगव्यभिचार-जैसे स्त्रीलिंगमें पुलिंगका प्रयोग करना । यथा-तारकाके लिये स्वाति शब्दका प्रयोग करना । इत्यादि व्यभिचार शब्दनयकी दृष्टिमें अग्राह्य नहीं है । जो एक ही अर्थको शब्दभेदसे अनेक रूपमें ग्रहण करता है उसे शब्दनय कहते हैं । जैसे एक ही इन्द्र व्यक्ति इन्दन (शासन) क्रियाके निमित्तसे इन्द्र, शकन (सामर्थ्यरूप) क्रियासे शक्र, तथा पुरोंके विदारण करनेसे पुरन्दर कहा जाता है । इस नयकी दृष्टिमें पर्यायशब्दोंका प्रयोग अग्राह्य है, क्योंकि, एक अर्थका बोधक एक ही शब्द होता है - समानार्थक अन्य शब्द उसका बोध नहीं करा सकता है । पदार्थ जिस क्षणमें जिस क्रियामें परिणत हो उसको जो उसी क्षणमें उसी स्वरूपसे ग्रहण करता है उसे एवम्भूतनय कहते हैं । इस नयकी अपेक्षा इन्द्र जब शासन क्रियामें परिणत रहेगा तब ही वह इन्द्र शब्दका वाच्य होगा, न कि अन्य समयमें भी । प्रमाण सम्यग्ज्ञानको कहा जाता है । वह प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है । जो ज्ञान इन्द्रिय, मन एवं प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तकी अपेक्षासे उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहा जाता है । उसके दो भेद हैं- मतिज्ञान और श्रुतज्ञान । जो ज्ञान इन्द्रियों और मनकी सहायतासे उत्पन्न होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । इस मतिज्ञानसे जानी हुई वस्तुके विषयमें जो विशेष विचार उत्पन्न होता है वह श्रुतज्ञान कहलाता है । प्रत्यक्ष प्रमाण तीन प्रकारका हैअवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान । इनमें जो इन्द्रिय आदिकी अपेक्षा न करके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी (पुद्गल और उससे सम्बद्ध संसारी प्राणी) पदार्थको ग्रहण करता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं । जो जीवोंके मनोगत पदार्थको जानता है वह मनःपर्ययज्ञान कहलाता है। समस्त विश्वको युगपत् ग्रहण करनेवाला ज्ञान केवलज्ञान कहा जाता है । ये तीनों ही ज्ञान अतीन्द्रिय हैं। निक्षेप शब्दका अर्थ रखना है । प्रत्येक शब्दका प्रयोग अनेक अर्थोंमें हुआ करता है। उनमेंसे किस समय कौन-सा अर्थ अभीष्ट है, यह बतलाना निक्षेप विधिका कार्य है । वह निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे चार प्रकारका है। वस्तुमें विवक्षित गुण एवं क्रिया आदिके न होनेपर भी केवल लोकव्यवहारके लिये वैसा नाम रख देनेको नामनिक्षेप कहा जाता है जैसे किसी व्यक्तिका नाम लोकव्यवहारके लिये देवदत्त ( देवके द्वारा न दिये जानेपर भी) रख देना। काष्ठकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म और पांसोंके निक्षेप आदिमें 'वह यह है' इस प्रकारकी जो कल्पना की जाती है उसे स्थापनानिक्षेप कहते हैं । वह दो प्रकारका है-सद्भावस्थापनानिक्षेप और असद्भावस्थापनानिक्षेप । स्थाप्यमान वस्तुके आकारवाली किसी अन्य वस्तुमें जो उसकी स्थापना की जाती है इसे सद्भावस्थापनानिक्षेप कहा जाता है-जैसे ऋषभ जिनेन्द्रके आकारभूत पाषाणमें ऋषभ जिनेन्द्रकी स्थापना करना । जो वस्तु स्थाप्यमान पदार्थके आकारकी नहीं है फिर भी उसमें उस वस्तुकी कल्पना करनेको असद्भावस्थापनानिक्षेप कहा जाता है- जैसे सतरंजकी गोटोंमें हाथीघोड़े आदिकी कल्पना करना । भविष्यमें होनेवाली पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुका कथन करना द्रव्यनिक्षेप पहलाता है। वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित वस्तुके कथनको भावनिक्षेप कहा जाता है। इस प्रकार इन
पचनं.