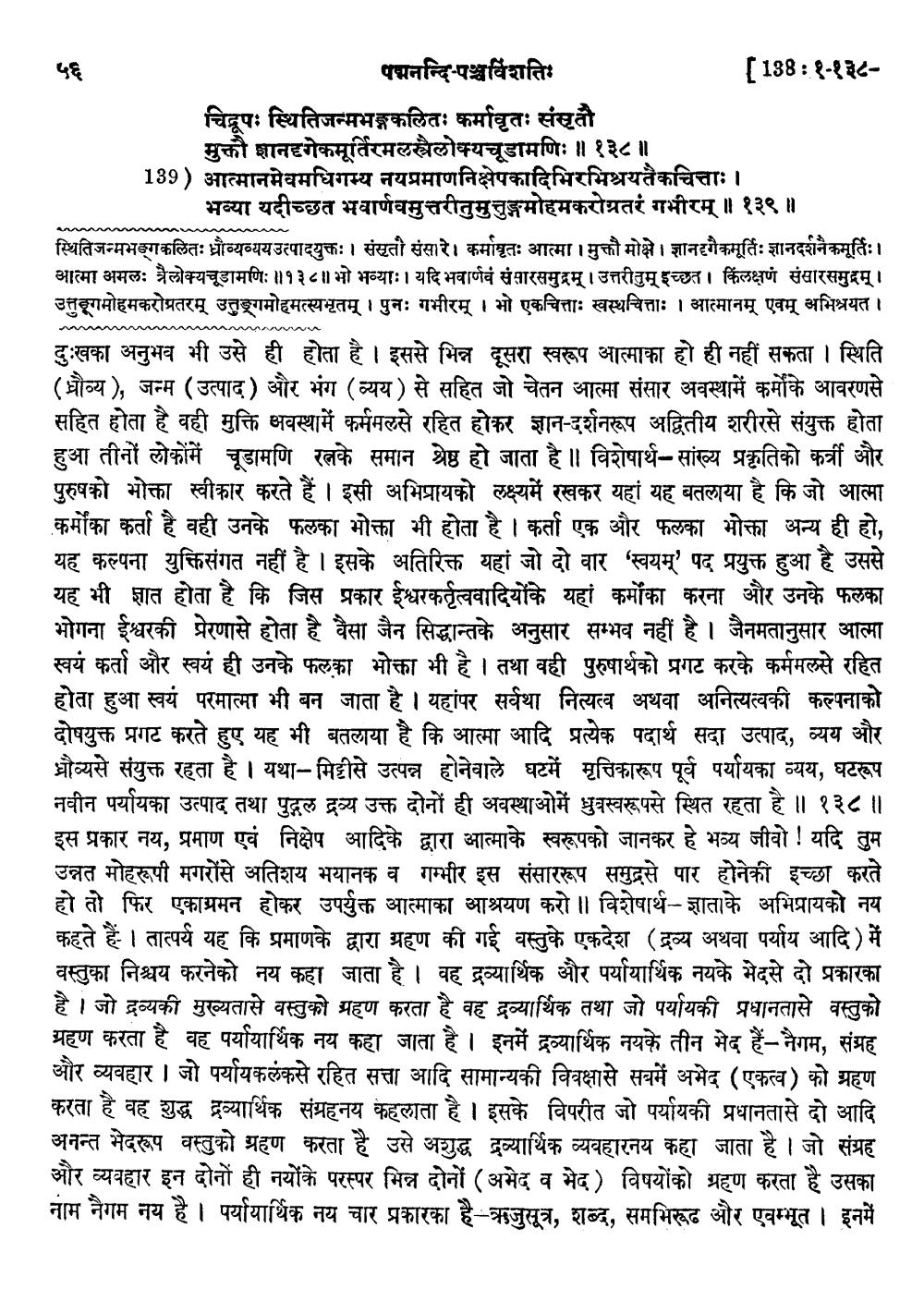________________
५६
anmannnnnnnamona
पमनन्दि-पञ्चविंशतिः
[138:१-१३८चिद्रूपः स्थितिजन्मभङ्गकलितः कर्मावृतः संसृतौ
मुक्तौ शानदृगेकमूर्तिरमलस्त्रैलोक्यचूडामणिः ॥ १३८ ॥ 139) आत्मानमेवमधिगम्य नयप्रमाणनिक्षेपकादिभिरभिश्रयतैकचित्ताः।
भव्या यदीच्छत भवार्णवमुत्तरीतुमुत्तुङ्गमोहमकरोग्रतरं गभीरम् ॥ १३९ ॥ स्थितिजन्मभङ्गकलितः ध्रौव्यव्ययउत्पादयुक्तः। संसृती संसारे। कर्मावृतः आत्मा । मुक्तौ मोक्षे । ज्ञानदृगैकमूर्तिः ज्ञानदर्शनैकमूर्तिः। आत्मा अमलः त्रैलोक्यचूडामणिः ॥१३८॥ भो भव्याः। यदि भवार्णवं संसारसमुद्रम् । उत्तरीतुम् इच्छत। किंलक्षणं संसारसमुद्रम् । उत्तुगमोहमकरोग्रतरम् उत्तुङ्गमोहमत्स्यभृतम् । पुनः गभीरम् । भो एकचित्ताः स्वस्थचित्ताः । आत्मानम् एवम् अभिश्रयत। दुःखका अनुभव भी उसे ही होता है। इससे भिन्न दूसरा स्वरूप आत्माका हो ही नहीं सकता । स्थिति (ध्रौव्य), जन्म (उत्पाद) और भंग (व्यय) से सहित जो चेतन आत्मा संसार अवस्थामें कर्मोके आवरणसे सहित होता है वही मुक्ति अवस्थामें कर्ममलसे रहित होकर ज्ञान-दर्शनरूप अद्वितीय शरीरसे संयुक्त होता हुआ तीनों लोकोंमें चूडामणि रत्नके समान श्रेष्ठ हो जाता है। विशेषार्थ- सांख्य प्रकृतिको की और पुरुषको भोक्ता स्वीकार करते हैं । इसी अभिप्रायको लक्ष्यमें रखकर यहां यह बतलाया है कि जो आत्मा कर्मोंका कर्ता है वही उनके फलका भोक्ता भी होता है । कर्ता एक और फलका भोक्ता अन्य ही हो, यह कल्पना युक्तिसंगत नहीं है । इसके अतिरिक्त यहां जो दो वार 'स्वयम्' पद प्रयुक्त हुआ है उससे यह भी ज्ञात होता है कि जिस प्रकार ईश्वरकर्तृत्ववादियोंके यहां कोंका करना और उनके फलका भोगना ईश्वरकी प्रेरणासे होता है वैसा जैन सिद्धान्तके अनुसार सम्भव नहीं है। जैनमतानुसार आत्मा स्वयं कर्ता और स्वयं ही उनके फलका भोक्ता भी है । तथा वही पुरुषार्थको प्रगट करके कर्ममलसे रहित होता हुआ स्वयं परमात्मा भी बन जाता है। यहांपर सर्वथा नित्यत्व अथवा अनित्यत्वकी कल्पनाको दोषयुक्त प्रगट करते हुए यह भी बतलाया है कि आत्मा आदि प्रत्येक पदार्थ सदा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यसे संयुक्त रहता है । यथा-मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घटमें मृत्तिकारूप पूर्व पर्यायका व्यय, घटरूप नवीन पर्यायका उत्पाद तथा पुद्गल द्रव्य उक्त दोनों ही अवस्थाओमें ध्रुवस्वरूपसे स्थित रहता है ॥ १३८ ॥ इस प्रकार नय, प्रमाण एवं निक्षेप आदिके द्वारा आत्माके स्वरूपको जानकर हे भव्य जीवो ! यदि तुम उन्नत मोहरूपी मगरोंसे अतिशय भयानक व गम्भीर इस संसाररूप समुद्रसे पार होनेकी इच्छा करते हो तो फिर एकाग्रमन होकर उपर्युक्त आत्माका आश्रयण करो ॥ विशेषार्थ- ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हैं । तात्पर्य यह कि प्रमाणके द्वारा ग्रहण की गई वस्तुके एकदेश (द्रव्य अथवा पर्याय आदि) में वस्तुका निश्चय करनेको नय कहा जाता है। वह द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके भेदसे दो प्रकारका है । जो द्रव्यकी मुख्यतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक तथा जो पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय कहा जाता है। इनमें द्रव्यार्थिक नयके तीन भेद हैं-नैगम, संग्रह और व्यवहार । जो पर्यायकलंकसे रहित सत्ता आदि सामान्यकी विवक्षासे सबमें अभेद (एकत्व) को ग्रहण करता है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक संग्रहनय कहलाता है। इसके विपरीत जो पर्यायकी प्रधानतासे दो आदि अनन्त भेदरूप वस्तुको ग्रहण करता है उसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक व्यवहारनय कहा जाता है । जो संग्रह और व्यवहार इन दोनों ही नयोंके परस्पर भिन्न दोनों (अभेद व भेद) विषयोंको ग्रहण करता है उसका नाम नैगम नय है। पर्यायार्थिक नय चार प्रकारका है-ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवम्भूत । इनमें