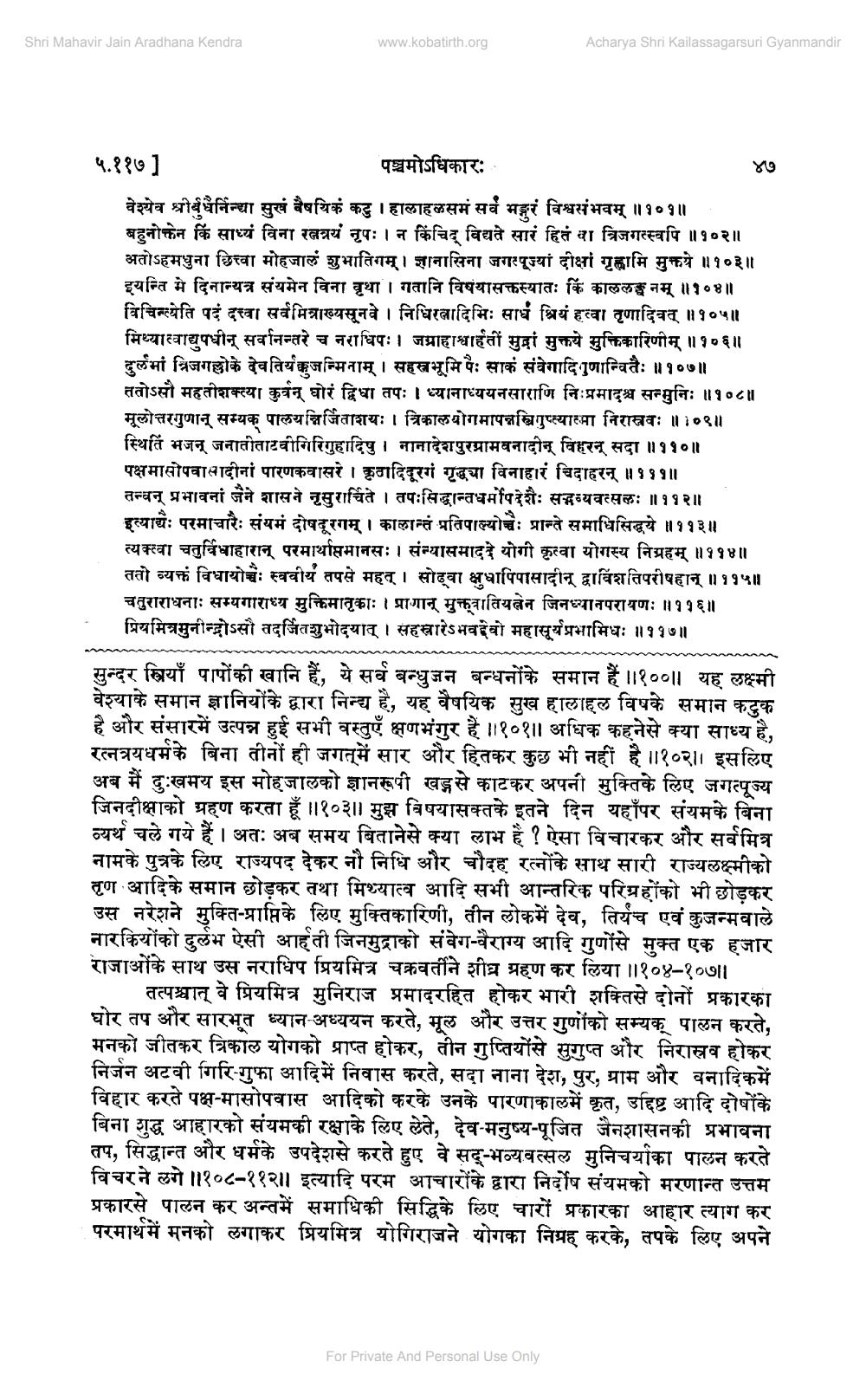________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
५.११७ ] पञ्चमोऽधिकारः
४७ वेश्येव श्रीवुधैर्निन्द्या सुखं वैषयिक कटु । हालाहलसमं सर्व भङ्गुरं विश्वसंभवम् ॥१०॥ बहुनोक्तेन किं साध्यं विना रत्नत्रयं नृपः । न किंचिद् विद्यते सारं हितं वा त्रिजगत्स्वपि ॥१०२॥ अतोऽहमधुना छित्त्वा मोहजालं शुभातिगम् । ज्ञानासिना जगत्पूज्यां दीक्षां गृह्णामि मुक्तये ॥१०३॥ इयन्ति मे दिनान्यत्र संयमेन विना वृथा । गतानि विषयासक्तस्यातः किं काललङ्घनम् ॥१०॥ विचिन्त्येति पदं दत्त्वा सर्वमित्राख्यसूनवे । निधिरत्नादिमिः साधं श्रियं हत्वा तृणादिवत् ॥१०५॥ मिथ्यात्वाद्युपधीन् सर्वानन्तरे च नराधिपः। जग्राहाश्वाती मुद्रां मुक्तये मुक्तिकारिणीम् ॥१०६॥ दुर्लमां त्रिजगल्लोके देवतिर्यक्कुजन्मिनाम् । सहस्त्रभूमि पैः साकं संवेगादिगुणान्वितैः ॥१०७॥ ततोऽसौ महतीशक्त्या कुर्वन् घोरं द्विधा तपः । ध्यानाध्ययनसाराणि निःप्रमादश्च सन्मुनिः ॥१०८॥ मुलोत्तरगुणान् सम्यक पालयतिर्जिताशयः । त्रिकालयोगमापन्नस्त्रिगुपस्यारुमा निराम्रवः ॥१०॥ स्थिति भजन जनातीताटवीगिरिगुहादिषु । नानादेशपुरनामवनादीन् विहरन् सदा ॥११०॥ पक्षमासोपवालादीनां पारणकवासरे । कृतादिदूरगं गृध्या विनाहारं चिदाहरन् ॥१११॥ तन्वन् प्रभावनां जेने शासने नृसुरार्चिते । तपःसिद्धान्तधर्मोपदेशैः सद्भग्यवत्सलः ॥११२॥ इत्यायैः परमाचारैः संयमं दोषदूरगम् । कालान्तं प्रतिपाल्योच्चैः प्रान्ते समाधिसिद्धये ॥११३॥ त्यक्त्वा चतुर्विधाहारान् परमार्थाप्तमानसः । संन्यासमाददे योगी कृत्वा योगस्य निग्रहम् ॥११॥ ततो व्यक्तं विधायोच्चैः स्ववीयं तपसे महत् । सोढ्वा क्षुधापिपासादीन् द्वाविंशतिपरीषहान् ॥११५॥ चतुराराधनाः सम्यगाराध्य मुक्तिमातृकाः। प्राणान् मुक्तवातियतेन जिनध्यानपरायणः ॥११६॥ प्रियमित्रमुनीन्द्रोऽसौ तदर्जितशुभोदयात् । सहस्रारेऽभवदेवो महासूर्यप्रभामिधः ॥११७॥
सुन्दर स्त्रियाँ पापोंकी खानि हैं, ये सर्व बन्धुजन बन्धनोंके समान हैं ॥१००। यह लक्ष्मी वेश्याके समान ज्ञानियों के द्वारा निन्द्य है, यह वैषयिक सुख हालाहल विषके समान कटुक है और संसारमें उत्पन्न हुई सभी वस्तुएँ क्षणभंगुर हैं ॥१०१।। अधिक कहनेसे क्या साध्य है, रत्नत्रयधर्मके बिना तीनों ही जगत्में सार और हितकर कुछ भी नहीं है ।।१०२।। इसलिए अब मैं दःखमय इस मोहजालको ज्ञानरूपी खडसे काटकर अपनी मुक्तिके लिए जगत्पज्य जिनदीक्षाको ग्रहण करता हूँ ॥१०३।। मुझ विषयासक्तके इतने दिन यहाँपर संयमके बिना व्यर्थ चले गये हैं । अतः अब समय बितानेसे क्या लाभ है ? ऐसा विचारकर और सर्वमित्र नामके पुत्रके लिए राज्यपद देकर नौ निधि और चौदह रत्नोंके साथ सारी राज्यलक्ष्मीको तृण आदिके समान छोड़कर तथा मिथ्यात्व आदि सभी आन्तरिक परिग्रहोंको भी छोड़कर उस नरेशने मुक्ति-प्राप्तिके लिए मुक्तिकारिणी, तीन लोकमें देव, तिर्यंच एवं कुजन्मवाले नारकियोंको दुर्लभ ऐसी आर्हती जिनमुद्राको संवेग-वैराग्य आदि गुणोंसे मुक्त एक हजार राजाओंके साथ उस नराधिप प्रिय मित्र चक्रवर्तीने शीघ्र ग्रहण कर लिया ॥१०४-१०७॥
तत्पश्चात् वे प्रियमित्र मुनिराज प्रमादरहित होकर भारी शक्तिसे दोनों प्रकारका घोर तप और सारभूत ध्यान-अध्ययन करते, मूल और उत्तर गुणोंको सम्यक् पालन करते, मनको जीतकर त्रिकाल योगको प्राप्त होकर, तीन गुप्तियोंसे सुगुप्त और निरास्रव होकर निर्जन अटवी गिरि-गफा आदिमें निवास करते, सदा नाना देश, पुर, ग्राम और वनादिकमें विहार करते पक्ष-मासोपवास आदिको करके उनके पारणाकालमें कृत, उद्दिष्ट आदि दोषोंके बिना शुद्ध आहारको संयमकी रक्षाके लिए लेते, देव-मनुष्य-पूजित जैनशासनकी प्रभावना तप, सिद्धान्त और धर्मके उपदेशसे करते हुए वे सद्-भव्यवत्सल मुनिचर्याका पालन करते विचरने लगे॥१०८-११२॥ इत्यादि परम आचारोंके द्वारा निर्दोष संयमको मरणान्त उत्तम प्रकारसे पालन कर अन्तमें समाधिकी सिद्धिके लिए चारों प्रकारका आहार त्याग कर परमार्थमें मनको लगाकर प्रियमित्र योगिराजने योगका निग्रह करके, तपके लिए अपने
For Private And Personal Use Only