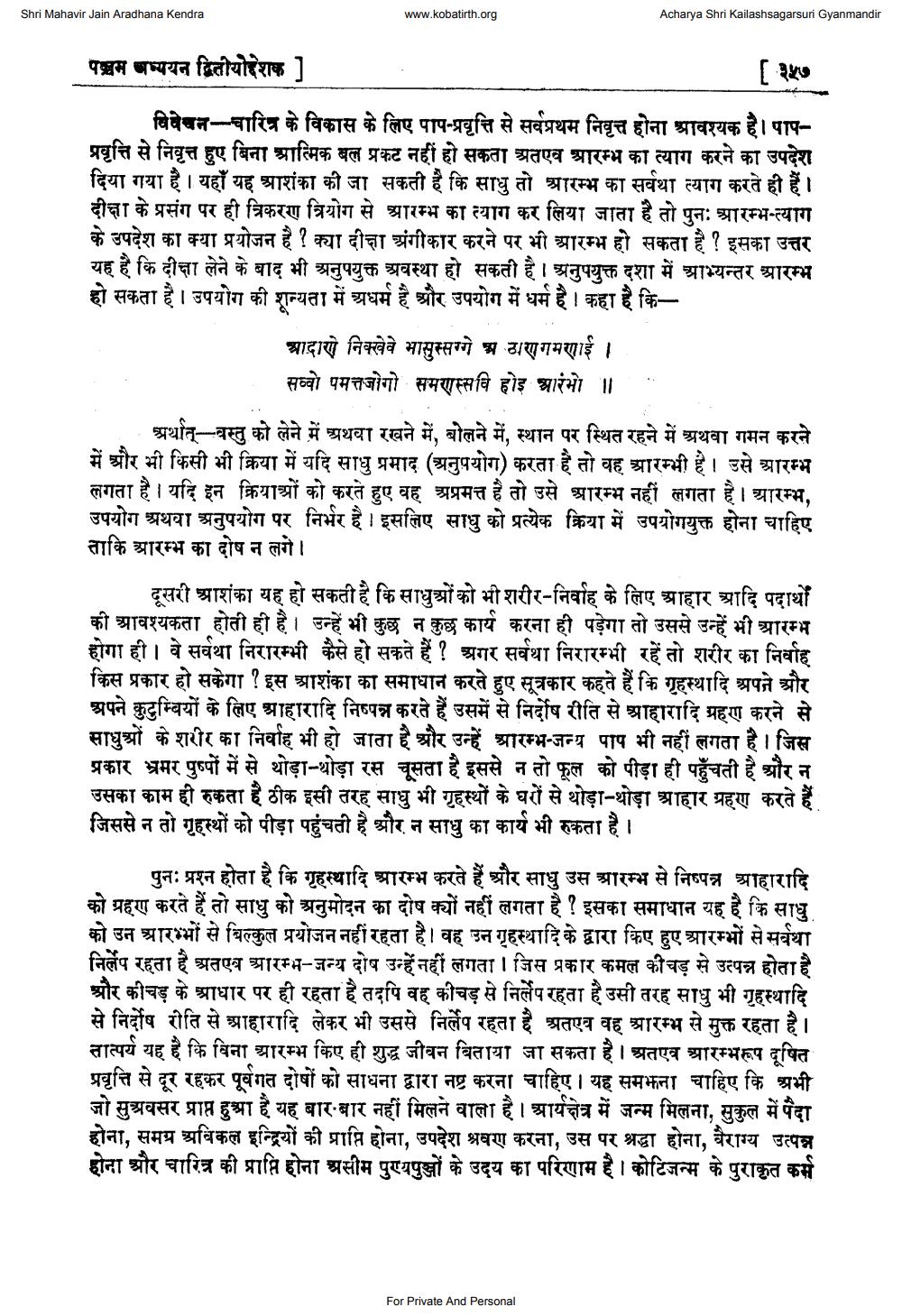________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailashsagarsuri Gyanmandir
पञ्चम अध्ययन द्वितीयोदेशक]
-
विवेचन-चारित्र के विकास के लिए पाप-प्रवृत्ति से सर्वप्रथम निवृत्त होना आवश्यक है। पापप्रवृत्ति से निवृत्त हुए बिना अात्मिक बल प्रकट नहीं हो सकता अतएव प्रारम्भ का त्याग करने का उपदेश दिया गया है । यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि साधु तो श्रारम्भ का सर्वथा त्याग करते ही हैं। दीक्षा के प्रसंग पर ही त्रिकरण त्रियोग से प्रारम्भ का त्याग कर लिया जाता है तो पुनः प्रारम्भ-त्याग के उपदेश का क्या प्रयोजन है ? क्या दीक्षा अंगीकार करने पर भी आरम्भ हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि दीक्षा लेने के बाद भी अनुपयुक्त अवस्था हो सकती है । अनुपयुक्त दशा में आभ्यन्तर आरम्भ हो सकता है। उपयोग की शून्यता में अधर्म है और उपयोग में धर्म है। कहा है कि
श्रादाणे निक्खेवे भासुस्सग्गे अ ठाणगमणाई । सव्वो पमत्तजोगो समणस्स वि होइ आरंभो ॥
. अर्थात्-वस्तु को लेने में अथवा रखने में, बोलने में, स्थान पर स्थित रहने में अथवा गमन करने में और भी किसी भी क्रिया में यदि साधु प्रमाद (अनुपयोग) करता है तो वह आरम्भी है। उसे प्रारम्भ लगता है। यदि इन क्रियाओं को करते हुए वह अप्रमत्त है तो उसे प्रारम्भ नहीं लगता है। श्रारम्भ, उपयोग अथवा अनुपयोग पर निर्भर है। इसलिए साधु को प्रत्येक क्रिया में उपयोगयुक्त होना चाहिए ताकि आरम्भ का दोष न लगे।
दूसरी आशंका यह हो सकती है कि साधुओं को भी शरीर-निर्वाह के लिए आहार आदि पदार्थों की आवश्यकता होती ही है। उन्हें भी कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ेगा तो उससे उन्हें भी प्रारम्भ होगा ही। वे सर्वथा निरारम्भी कैसे हो सकते हैं ? अगर सर्वथा निरारम्भी रहें तो शरीर का निर्वाह किस प्रकार हो सकेगा ? इस आशंका का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि गृहस्थादि अपने और अपने कुटुम्बियों के लिए आहारादि निष्पन्न करते हैं उसमें से निर्दोष रीति से आहारादि ग्रहण करने से साधुओं के शरीर का निर्वाह भी हो जाता है और उन्हें आरम्भ-जन्य पाप भी नहीं लगता है । जिस प्रकार भ्रमर पुष्पों में से थोड़ा-थोड़ा रस चूसता है इससे न तो फूल को पीड़ा ही पहुँचती है और न उसका काम ही रुकता है ठीक इसी तरह साधु भी गृहस्थों के घरों से थोड़ा-थोड़ा आहार ग्रहण करते हैं. जिससे न तो गृहस्थों को पीड़ा पहुंचती है और न साधु का कार्य भी रुकता है ।
पुनः प्रश्न होता है कि गृहस्थादि प्रारम्भ करते हैं और साधु उस आरम्भ से निष्पन्न आहारादि को ग्रहण करते हैं तो साधु को अनुमोदन का दोष क्यों नहीं लगता है ? इसका समाधान यह है कि साधु को उन प्रारम्भों से बिल्कुल प्रयोजन नहीं रहता है। वह उन गृहस्थादि के द्वारा किए हुए प्रारम्भों से सर्वथा निर्लेप रहता है अतएव आरम्भ-जन्य दोष उन्हें नहीं लगता । जिस प्रकार कमल कीचड़ से उत्पन्न होता है
और कीचड़ के आधार पर ही रहता है तदपि वह कीचड़ से निर्लेप रहता है उसी तरह साधु भी गृहस्थादि से निर्दोष रीति से आहारादि लेकर भी उससे निर्लेप रहता है अतएव वह प्रारम्भ से मुक्त रहता है। तात्पर्य यह है कि विना प्रारम्भ किए ही शुद्ध जीवन बिताया जा सकता है । अतएव प्रारम्भरूप दूषित प्रवृत्ति से दूर रहकर पूर्वगत दोषों को साधना द्वारा नष्ट करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि अभी जो सुअवसर प्राप्त हुआ है यह बार-बार नहीं मिलने वाला है । आर्यक्षेत्र में जन्म मिलना, सुकुल में पैदा होना, समग्र अविकल इन्द्रियों की प्राप्ति होना, उपदेश श्रवण करना, उस पर श्रद्धा होना, वैराग्य उत्पन्न होना और चारित्र की प्राप्ति होना असीम पुण्यपुओं के उदय का परिणाम है । कोटिजन्म के पुराकृत कर्म
For Private And Personal