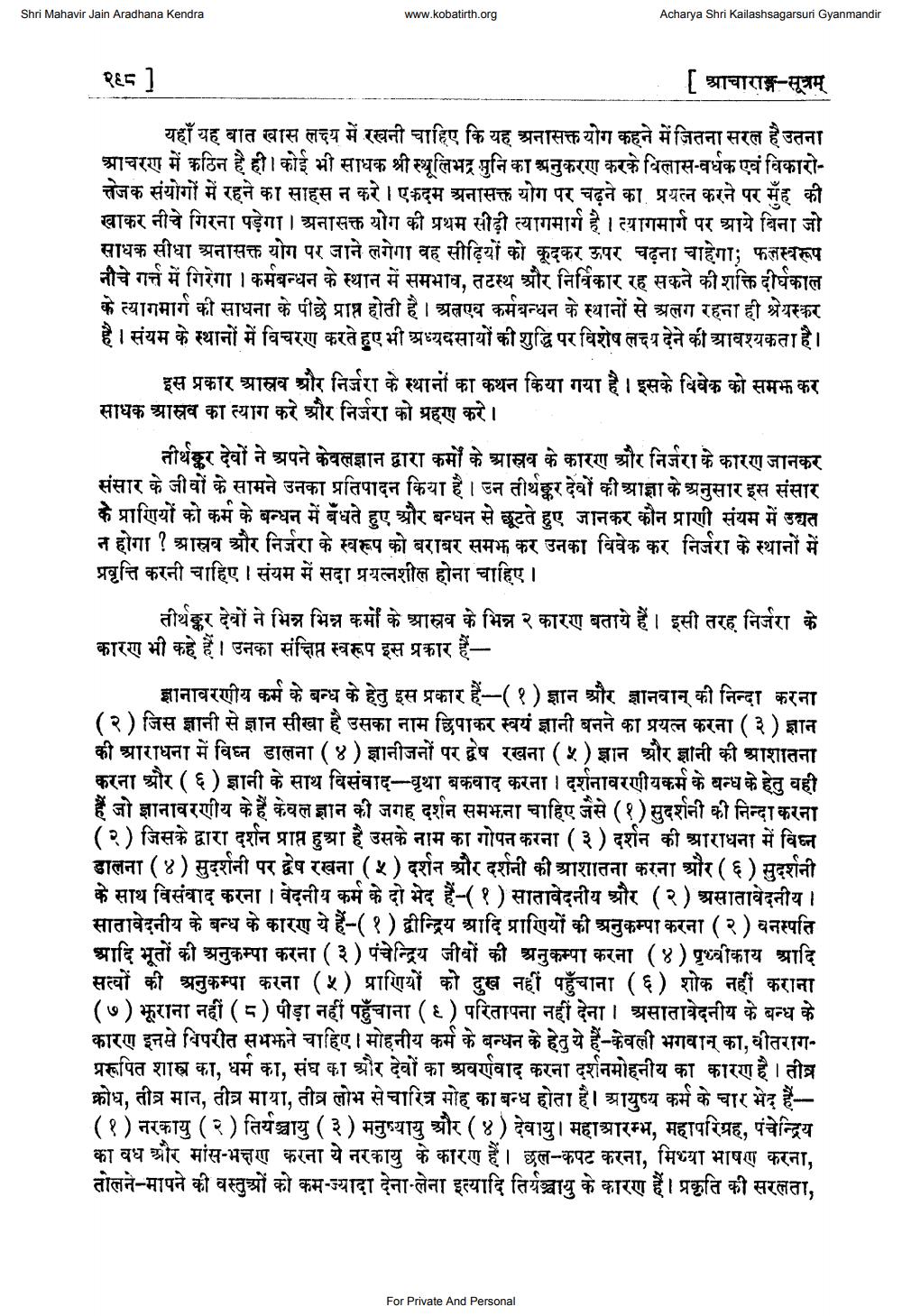________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailashsagarsuri Gyanmandir
२६८ ]
[ आचाराङ्ग-सूत्रम्
यहाँ यह बात खास लक्ष्य में रखनी चाहिए कि यह अनासक्त योग कहने में जितना सरल है उतना आचरण में कठिन है ही। कोई भी साधक श्री स्थूलभद्र मुनि का अनुकरण करके विलास-वर्धक एवं विकारोतेजक संयोगों में रहने का साहस न करे । एकदम अनासक्त योग पर चढ़ने का प्रयत्न करने पर मुँह की खाकर नीचे गिरना पड़ेगा । अनासक्त योग की प्रथम सीढ़ी त्यागमार्ग है। त्यागमार्ग पर आये बिना जो साधक सीधा अनासक्त योग पर जाने लगेगा वह सीढ़ियों को कूदकर ऊपर चढ़ना चाहेगा; फलस्वरूप नीचे गर्भ में गिरेगा | कर्मबन्धन के स्थान में समभाव, तटस्थ और निर्विकार रह सकने की शक्ति दीर्घकाल के त्यागमार्ग की साधना के पीछे प्राप्त होती है । अतएव कर्मबन्धन के स्थानों से अलग रहना ही श्रेयस्कर है । संयम के स्थानों में विचरण करते हुए भी अध्यवसायों की शुद्धि पर विशेष लक्ष्य देने की आवश्यकता है।
इस प्रकार आस्रव और निर्जरा के स्थानों का कथन किया गया है। इसके विवेक को समझ कर साधक आस्रव का त्याग करे और निर्जरा को ग्रहण करे ।
तीर्थकर देवों ने अपने केवलज्ञान द्वारा कर्मों के आसव के कारण और निर्जरा के कारण जानकर संसार के जीवों के सामने उनका प्रतिपादन किया है। उन तीर्थङ्कर देवों की आज्ञा के अनुसार इस संसार के प्राणियों को कर्म के बन्धन में बँधते हुए और बन्धन से छूटते हुए जानकर कौन प्राणी संयम में उद्यत न होगा ? स्रव और निर्जरा के स्वरूप को बराबर समझ कर उनका विवेक कर निर्जरा के स्थानों में प्रवृत्ति करनी चाहिए । संयम में सदा प्रयत्नशील होना चाहिए ।
तीर्थङ्कर देवों ने भिन्न भिन्न कर्मों के प्रसव के भिन्न २ कारण बताये हैं । इसी तरह निर्जरा के कारण भी कहे हैं। उनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैं
ज्ञानावरणीय कर्म के बन्ध के हेतु इस प्रकार हैं- ( १ ) ज्ञान और ज्ञानवान् की निन्दा करना (२) जिस ज्ञानी से ज्ञान सीखा है उसका नाम छिपाकर स्वयं ज्ञानी बनने का प्रयत्न करना (३) ज्ञान की आराधना में विघ्न डालना ( ४ ) ज्ञानीजनों पर द्वेष रखना ( ५ ) ज्ञान और ज्ञानी की आशातना करना और ( ६ ) ज्ञानी के साथ विसंवाद - वृथा बकवाद करना । दर्शनावरणीयकर्म के बन्ध के हेतु वही ज्ञानावरणीय हैं केवल ज्ञान की जगह दर्शन समझना चाहिए जैसे (१) सुदर्शनी की निन्दा करना (२) जिसके द्वारा दर्शन प्राप्त हुआ है उसके नाम का गोपन करना ( ३ ) दर्शन की आराधना में डालना (४) सुदर्शनी पर द्वेष रखना (५) दर्शन और दर्शनी की आशातना करना और (६) सुदर्शनी
साथ विसंवाद करना । वेदनीय कर्म के दो भेद हैं- ( १ ) सातावेदनीय और ( २ ) असातावेदनीय । सातावेदनीय के बन्ध के कारण ये हैं- (१) द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों की अनुकम्पा करना ( २ ) वनस्पति आदि भूतों की अनुकम्पा करना (३) पंचेन्द्रिय जीवों की अनुकम्पा करना ( ४ ) पृथ्वीका आदि सत्वों की अनुकम्पा करना ( ५ ) प्राणियों को दुख नहीं पहुँचाना ( ६ ) शोक नहीं कराना (७) भूराना नहीं ( ८ ) पीड़ा नहीं पहुँचाना ( ६ ) परितापना नहीं देना । असातावेदनीय के बन्ध के कारण इनसे विपरीत समझने चाहिए। मोहनीय कर्म के बन्धन के हेतु ये हैं-केवली भगवान् का, वीतरागप्ररूपित शास्त्र का, धर्म का, संघ का और देवों का अवर्णवाद करना दर्शनमोहनीय का कारण है। तीव्र क्रोध, तीत्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ से चारित्र मोह का बन्ध होता है। आयुष्य कर्म के चार भेद हैं(१) नरकायु ( २ ) तिर्यञ्चायु (३) मनुष्यायु और ( ४ ) देवायु। महाआरम्भ, महापरिग्रह, पंचेन्द्रिय का वध और मांस भक्षण करना ये नरकायु के कारण हैं। छल-कपट करना, मिथ्या भाषण करना, तोलने - मापने की वस्तुओं को कम-ज्यादा देना लेना इत्यादि तिर्यञ्चायु के कारण हैं । प्रकृति की सरलता,
For Private And Personal