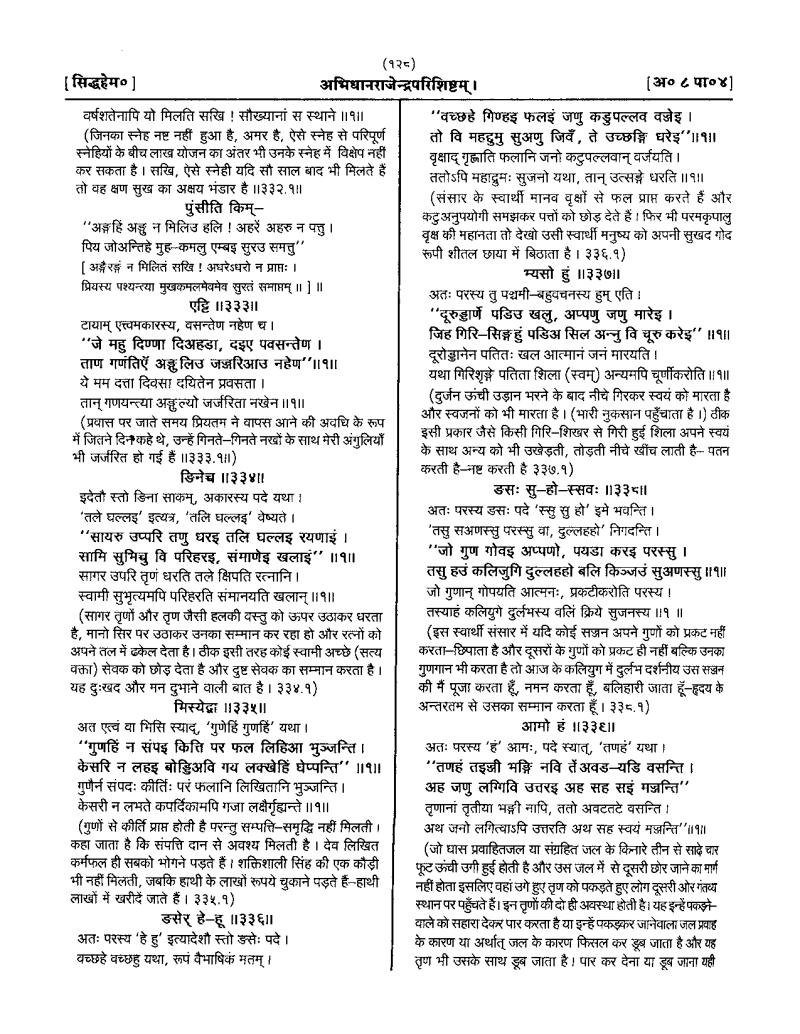________________ (128) [सिद्धहेम०] अभिधानराजेन्द्रपरिशिष्टम्। [अ०८पा०४] वर्षशतेनापि यो मिलति सखि ! सौख्यानां स स्थाने ||1|| "वच्छहे गिण्हइ फलई जणु कडुपल्लव वज्जेइ। (जिनका स्नेह नष्ट नहीं हुआ है, अमर है, ऐसे स्नेह से परिपूर्ण तो वि महहुमु सुअणु जिवँ, ते उच्छङ्गि घरेइ"||१|| स्नेहियों के बीच लाख योजन का अंतर भी उनके स्नेह में विक्षेप नहीं वृक्षाद् गृह्णाति फलानि जनो कटुपल्लवान् वर्जयति। कर सकता है। सखि, ऐसे स्नेही यदि सौ साल बाद भी मिलते हैं ततोऽपि महाद्रुमः सुजनो यथा, तान् उत्सङ्गे धरति / / 1 / / तो वह क्षण सुख का अक्षय भंडार है // 332.1 / / (संसार के स्वार्थी मानव वृक्षों से फल प्राप्त करते हैं और पुंसीति किम् कटु अनुपयोगी समझकर पत्तों को छोड़ देते हैं। फिर भी परमकृपालु "अङ्गहिं अङ्गु न मिलिउ हलि ! अहरें अहरु न पत्तु / वृक्ष की महानता तो देखो उसी स्वार्थी मनुष्य को अपनी सुखद गोद पिय जोअन्तिहे मुह कमलु एम्बइ सुरउ समत्तु" रूपी शीतल छाया में बिठाता है। 336.1) [ अझैरङ्गं न मिलितं सखि ! अधरेऽधरो न प्राप्तः / म्यसो हुं // 337|| प्रियस्य पश्यन्त्या मुखकमलमेवमेव सुरतं समाप्तम् // ] || अतः परस्य तु पञ्चमी-बहुवचनस्य हुम् एति। एट्टि // 333 / / "दूरुड्डाणे पडिउ खलु, अप्पणु जणु मारेइ / टायाम् एत्त्वमकारस्य, वसन्तेण नहेण च / जिह गिरि-सिङ्गहुं पडिअ सिल अन्नु वि चूरु करेइ" ||1|| "जे महु दिण्णा दिअहडा, दइए पवसन्तेण / दूरोड्डानेन पतितः खल आत्मानं जनं मारयति / ताण गणंतिऍ अङ्गुलिउ जज्जरिआउ नहेण"||१|| ये मम दत्ता दिवसा दयितेन प्रवसता। यथा गिरिशृङ्गे पतिता शिला (स्वम्) अन्यमपि चूर्णीकरोति // 1 // तान् गणयन्त्या अडल्यो जर्जरिता नखेन / / 1 / / (दुर्जन ऊंची उड़ान भरने के बाद नीचे गिरकर स्वयं को मारता है (प्रवास पर जाते समय प्रियतम ने वापस आने की अवधि के रूप और स्वजनों को भी मारता है। (भारी नुकसान पहुंचाता है।) ठीक में जितने दिन कहे थे, उन्हें गिनते-गिनते नखों के साथ मेरी अंगुलियाँ इसी प्रकार जैसे किसी गिरि-शिखर से गिरी हुई शिला अपने स्वयं भी जर्जरित हो गई हैं // 333.11) के साथ अन्य को भी उखेड़ती, तोड़ती नीचे खींच लाती है-- पतन डिनेच // 33 // करती है-नष्ट करती है 337.1) इदेतौ स्तो डिना साकम्, अकारस्य पदे यथा / ङसः सु-हो-स्सवः // 33 // 'तले घल्लइ' इत्यत्र, 'तलि घल्लइ' वेष्यते। अतः परस्य डसः पदे 'स्सु सु हो' इमे भवन्ति / "सायरु उप्परि तणु धरइ तलि घल्लइ रयणाई। 'तसु सअणस्सु परस्सु वा, दुल्लहहो' निगदन्ति / सामि सुभिचु वि परिहरइ, संमाणेइ खलाई" ||1|| "जो गुण गोवइ अप्पणो, पयडा करइ परस्सु / सागर उपरि तृणं धरति तले क्षिपति रत्नानि। तसु हउं कलिजुगि दुल्लहहो बलि किञ्जउं सुअणस्सु // 1 // स्वामी सुभृत्यमपि परिहरति संमानयति खलान् / / 1 / / जो गुणान् गोपयति आत्मनः, प्रकटीकरोति परस्य / (सागर तृणों और तृण जैसी हलकी वस्तु को ऊपर उठाकर धरता तस्याहं कलियुगे दुर्लभस्य वलिं क्रिये सुजनस्य // 1 // है, मानो सिर पर उठाकर उनका सम्मान कर रहा हो और रत्नों को (इस स्वार्थी संसार में यदि कोई सज्जन अपने गुणों को प्रकट नहीं अपने तल में ढकेल देता है। ठीक इसी तरह कोई स्वामी अच्छे (सत्य करता-छिपाता है और दूसरों के गुणों को प्रकट ही नहीं बल्कि उनका वक्ता) सेवक को छोड़ देता है और दुष्ट सेवक का सम्मान करता है। गुणगान भी करता है तो आज के कलियुग में दुर्लभ दर्शनीय उस सज्जन यह दुःखद और मन दुभाने वाली बात है। 334.1) की मैं पूजा करता हूँ, नमन करता हूँ, बलिहारी जाता हूँ-हृदय के मिस्येदा // 33 // अन्तरतम से उसका सम्मान करता हूँ। 338.1) अत एत्वं या भिसि स्याद्, 'गुणेहिं गुणहिं' यथा / आमो हं // 336 / / "गुणहिं न संपइ कित्ति पर फल लिहिआ भुञ्जन्ति। अतः परस्य 'हं' आमः, पदे स्यात्, 'तणहं' यथा। केसरि न लहइ बोड्डिअवि गय लक्खेहिं घेप्पन्ति" ||1|| "तणहं तइजी भङ्गि नवि तें अवड-यडि वसन्ति / गुणैर्न संपदः कीर्तिः परं फलानि लिखितानि भुञ्जन्ति / अह जणु लग्गिवि उत्तरइ अह सह सई मज्जन्ति" केसरी न लभते कपर्दिकामपि गजा लक्षैर्गृह्यन्ते / / 1 / / तृणानां तृतीया भङ्गी नापि, ततो अवटतटे वसन्ति / (गुणों से कीर्ति प्राप्त होती है परन्तु सम्पत्ति-समृद्धि नहीं मिलती। अथ जनो लगित्वाऽपि उत्तरति अथ सह स्वयं मजन्ति"||१|| कहा जाता है कि संपत्ति दान से अवश्य मिलती है। देव लिखित (जो घास प्रवाहितजल या संग्रहित जल के किनारे तीन से साढ़े चार कर्मफल ही सबको भोगने पड़ते हैं। शक्तिशाली सिंह की एक कौड़ी फूट ऊंची उगी हुई होती है और उस जल में से दूसरी छोर जाने का मार्ग भी नहीं मिलती, जबकि हाथी के लाखों रूपये चुकाने पड़ते हैं-हाथी नहीं होता इसलिए वहां उगे हुए तृण को पकड़ते हुए लोग दूसरी ओर गंतव्य लाखों में खरीदें जाते हैं / 335.1) स्थान पर पहुँचते हैं। इन तृणों की दो ही अवस्था होती है। यह इन्हें पकड़ो ङसेर् हे-हू // 336|| वाले को सहारा देकर पार करता है या इन्हें पकड़कर जानेवाला जल प्रवाह अतः परस्य 'हे हु' इत्यादेशौ स्तो उसेः पदे। के कारण या अर्थात् जल के कारण फिसल कर डूब जाता है और यह वच्छहे वच्छहु यथा, रूपं वैभाषिक मतम् / तृण भी उसके साथ डूब जाता है। पार कर देना या डूब जाना यही