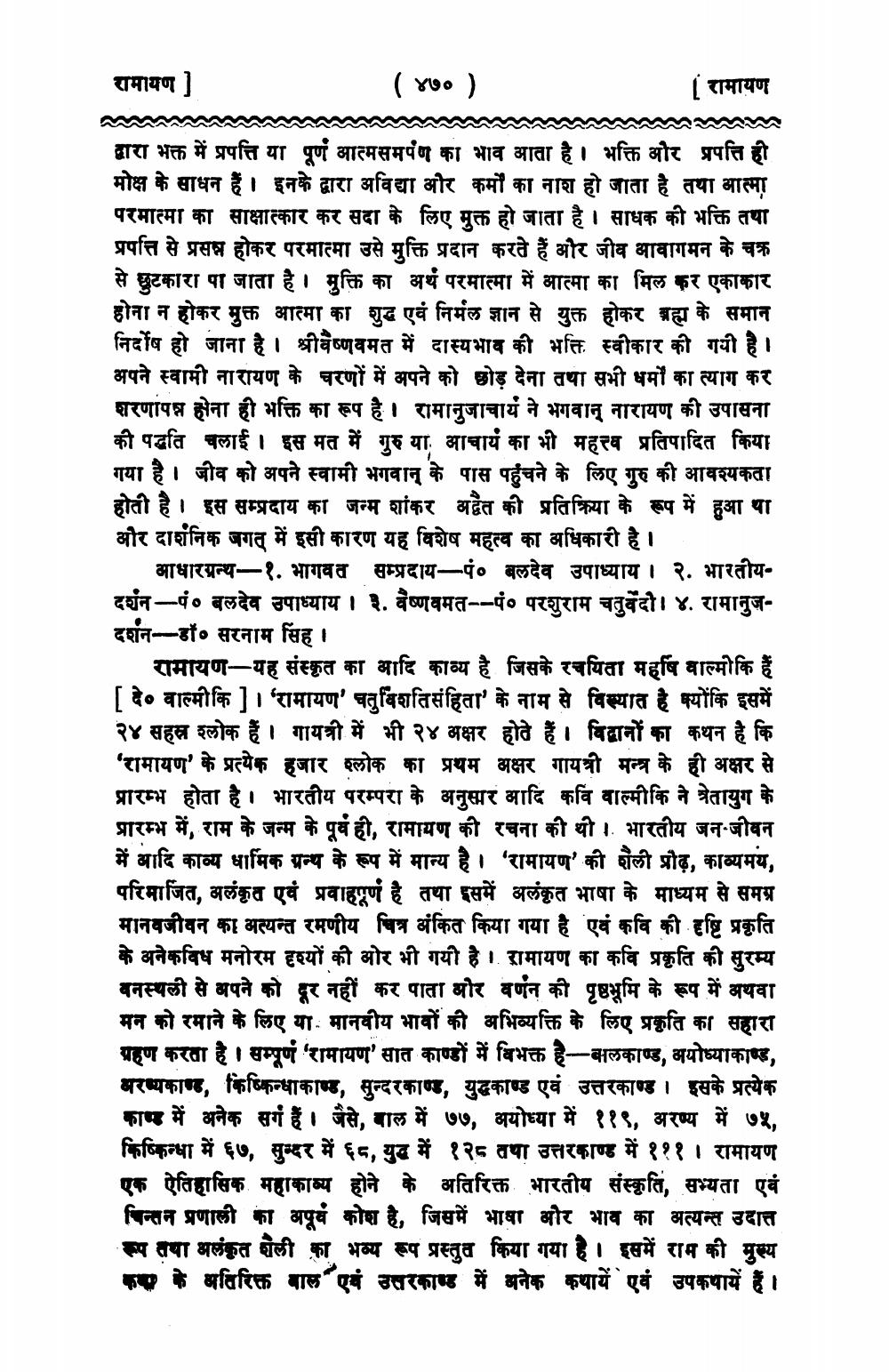________________
रामायण]
( ४७० )
रामायण
द्वारा भक्त में प्रपत्ति या पूर्ण आत्मसमर्पण का भाव आता है। भक्ति और प्रपत्ति ही मोक्ष के साधन हैं। इनके द्वारा अविद्या और कर्मों का नाश हो जाता है तथा आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सदा के लिए मुक्त हो जाता है । साधक की भक्ति तथा प्रपत्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा उसे मुक्ति प्रदान करते हैं और जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। मुक्ति का अर्थ परमात्मा में आत्मा का मिल कर एकाकार होना न होकर मुक्त आत्मा का शुद्ध एवं निर्मल ज्ञान से युक्त होकर ब्रह्म के समान निर्दोष हो जाना है। श्रीवैष्णवमत में दास्यभाव की भक्ति स्वीकार की गयी है। अपने स्वामी नारायण के चरणों में अपने को छोड़ देना तथा सभी धर्मों का त्याग कर शरणापन्न होना ही भक्ति का रूप है। रामानुजाचार्य ने भगवान् नारायण की उपासना की पद्धति चलाई। इस मत में गुरु या. आचार्य का भी महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। जीव को अपने स्वामी भगवान् के पास पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इस सम्प्रदाय का जन्म शांकर अद्वैत की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था और दार्शनिक जगत् में इसी कारण यह विशेष महत्व का अधिकारी है।
आधारग्रन्थ-१. भागवत सम्प्रदाय-पं. बलदेव उपाध्याय । २. भारतीयदर्शन-पं० बलदेव उपाध्याय । ३. वैष्णवमत--पं० परशुराम चतुर्वेदी। ४. रामानुजदर्शन-डॉ० सरनाम सिंह।
रामायण-यह संस्कृत का आदि काव्य है जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं [३० वाल्मीकि ] | 'रामायण' चतुर्विशतिसंहिता' के नाम से विख्यात है क्योंकि इसमें २४ सहस्र श्लोक हैं। गायत्री में भी २४ अक्षर होते हैं। विद्वानों का कथन है कि 'रामायण' के प्रत्येक हजार श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मन्त्र के ही अक्षर से प्रारम्भ होता है। भारतीय परम्परा के अनुसार आदि कवि वाल्मीकि ने त्रेतायुग के प्रारम्भ में, राम के जन्म के पूर्व ही, रामायण की रचना की थी। भारतीय जन-जीवन में आदि काव्य धार्मिक ग्रन्थ के रूप में मान्य है। 'रामायण' की शैली प्रौढ़, काव्यमय, परिमार्जित, अलंकृत एवं प्रवाहपूर्ण है तथा इसमें अलंकृत भाषा के माध्यम से समग्र मानवजीवन का अत्यन्त रमणीय चित्र अंकित किया गया है एवं कवि की दृष्टि प्रकृति के अनेकविध मनोरम दृश्यों की ओर भी गयी है। रामायण का कवि प्रकृति की सुरम्य वनस्थली से अपने को दूर नहीं कर पाता और वर्णन की पृष्ठभूमि के रूप में अथवा मन को रमाने के लिए याः मानवीय भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति का सहारा ग्रहण करता है । सम्पूर्ण 'रामायण' सात काण्डों में विभक्त है-बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, बरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड । इसके प्रत्येक काड में अनेक सर्ग हैं। जैसे, बाल में ७७, अयोध्या में ११९, अरण्य में ७५, किष्किन्धा में ६७, सुन्दर में ६८, युद्ध में १२८ तथा उत्तरकाण्ड में १११ । रामायण एक ऐतिहासिक महाकाव्य होने के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं चिन्तन प्रणाली का अपूर्व कोश है, जिसमें भाषा और भाव का अत्यन्त उदात्त स्प तथा अलंकृत शैली का भव्य रूप प्रस्तुत किया गया है। इसमें राम की मुख्य का के अतिरिक्त बाल एवं उत्तरकाण्ड में अनेक कथायें एवं उपकथायें हैं।