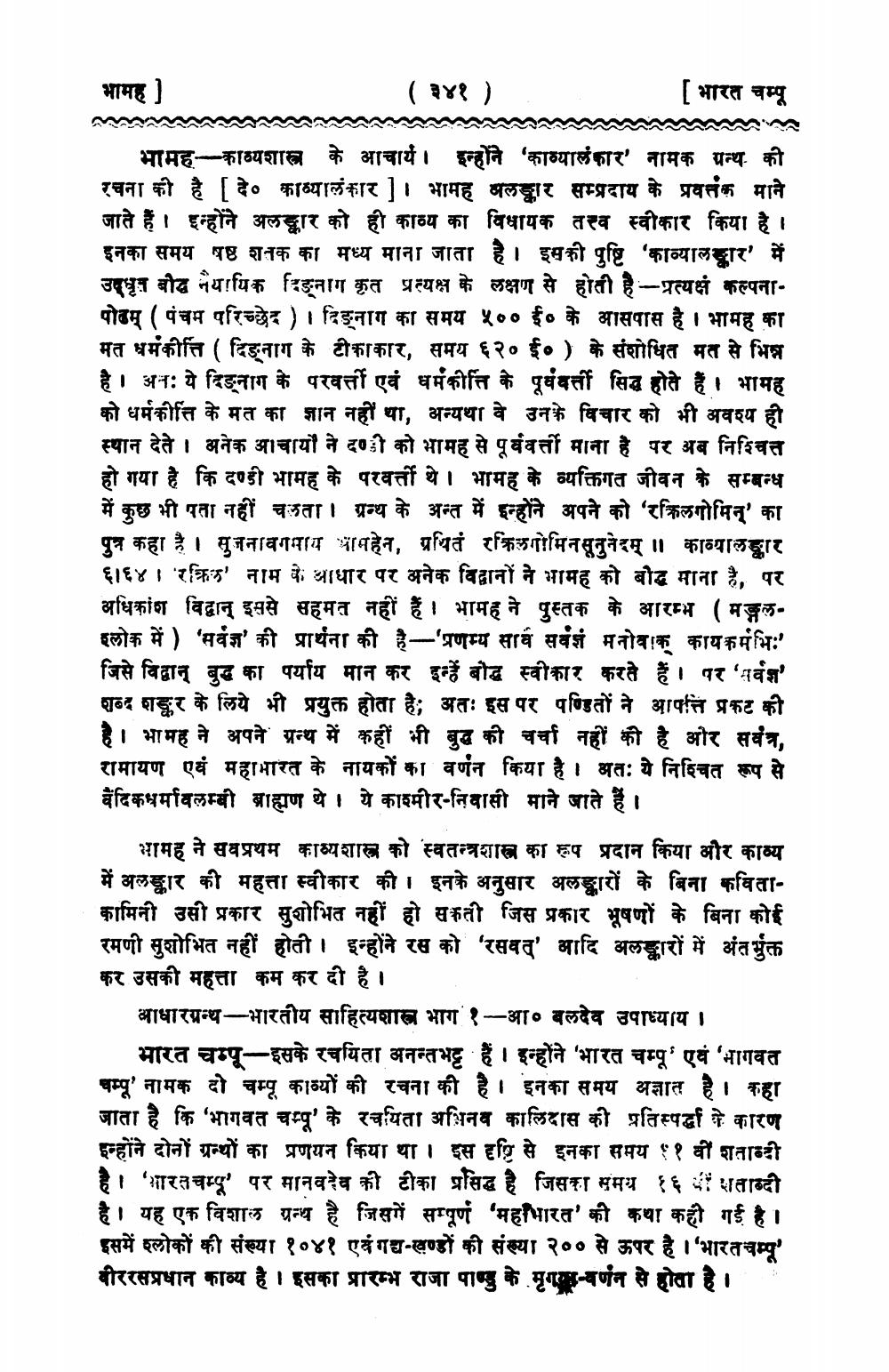________________
भामह
(३४१ )
[ भारत चम्पू
भामह-काव्यशास्त्र के आचार्य। इन्होंने 'काव्यालंकार' नामक ग्रन्थ की रचना की है [ दे० काव्यालंकार ] । भामह अलङ्कार सम्प्रदाय के प्रवत्तंक माने जाते हैं। इन्होंने अलङ्कार को ही काव्य का विधायक तत्व स्वीकार किया है । इनका समय षष्ठ शतक का मध्य माना जाता है। इसकी पुष्टि 'काव्यालङ्कार' में उद्धृत बौद्ध नैयायिक दिङ्नाग कृत प्रत्यक्ष के लक्षण से होती है-प्रत्यक्षं कल्पनापोढम् (पंचम परिच्छेद)। दिङ्नाग का समय ५०० ई. के आसपास है। भामह का मत धर्मकीति ( दिङ्नाग के टीकाकार, समय ६२० ई.) के संशोधित मत से भिन्न है। अत: ये दिङ्नाग के परवर्ती एवं धर्मकीत्ति के पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। भामह को धर्मकीत्ति के मत का ज्ञान नहीं था, अन्यथा वे उनके विचार को भी अवश्य ही स्थान देते। अनेक आचार्यों ने दण्डी को भामह से पूर्ववर्ती माना है पर अब निश्चित हो गया है कि दण्डी भामह के परवर्ती थे। भामह के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चलता। ग्रन्थ के अन्त में इन्होंने अपने को 'रक्रिलगोमिन्' का पुत्र कहा है। सुजनावगमाय भामहेन, प्रथितं रक्रिलगोमिनसूनुनेदम् ॥ काव्यालङ्कार ६।६४ । 'रक्रिक' नाम के आधार पर अनेक विद्वानों ने भामह को बौद्ध माना है, पर अधिकांश विद्वान् इससे सहमत नहीं हैं। भामह ने पुस्तक के आरम्भ ( मङ्गलश्लोक में ) 'सर्वज्ञ' की प्रार्थना की है-'प्रणम्य सावं सर्वशं मनोवाक् कायकर्मभिः' जिसे विद्वान् बुद्ध का पर्याय मान कर इन्हें बौद्ध स्वीकार करते हैं। पर 'सर्वश' शब्द शङ्कर के लिये भी प्रयुक्त होता है; अतः इस पर पण्डितों ने आपत्ति प्रकट की है। भामह ने अपने ग्रन्थ में कहीं भी बुद्ध की चर्चा नहीं की है और सर्वत्र, रामायण एवं महाभारत के नायकों का वर्णन किया है। अतः ये निश्चित रूप से वैदिकधर्मावलम्बी ब्राह्मण थे। ये काश्मीर-निवासी माने जाते हैं।
भामह ने सवप्रथम काव्यशास्त्र को स्वतन्त्रशास्त्र का रूप प्रदान किया और काव्य में अलङ्कार की महत्ता स्वीकार की। इनके अनुसार अलङ्कारों के बिना कविताकामिनी उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो सकती जिस प्रकार भूषणों के बिना कोई रमणी सुशोभित नहीं होती। इन्होंने रस को 'रसवत्' आदि अलङ्कारों में अंतर्भुक्त कर उसकी महत्ता कम कर दी है।
आधारग्रन्थ-भारतीय साहित्यशास्त्र भाग १-आ० बलदेव उपाध्याय ।
भारत चम्पू-इसके रचयिता अनन्तभट्ट हैं। इन्होंने 'भारत चम्पू' एवं 'भागवत चम्पू' नामक दो चम्पू काव्यों की रचना की है। इनका समय अज्ञात है। कहा जाता है कि 'भागवत चम्पू' के रचयिता अभिनव कालिदास की प्रतिस्पर्धा के कारण इन्होंने दोनों ग्रन्थों का प्रणयन किया था। इस दृष्टि से इनका समय ६१ वीं शताब्दी है। भारत चम्पू' पर मानवदेव की टीका प्रसिद्ध है जिसका समय १६ वी शताब्दी है। यह एक विशाल ग्रन्थ है जिसमें सम्पूर्ण 'महाभारत' की कथा कही गई है। इसमें श्लोकों की संख्या १०४१ एवं गद्य-खण्डों की संख्या २०० से ऊपर है । भारतचम्पू वीररसप्रधान काव्य है । इसका प्रारम्भ राजा पातु के मृगा-वर्णन से होता है।