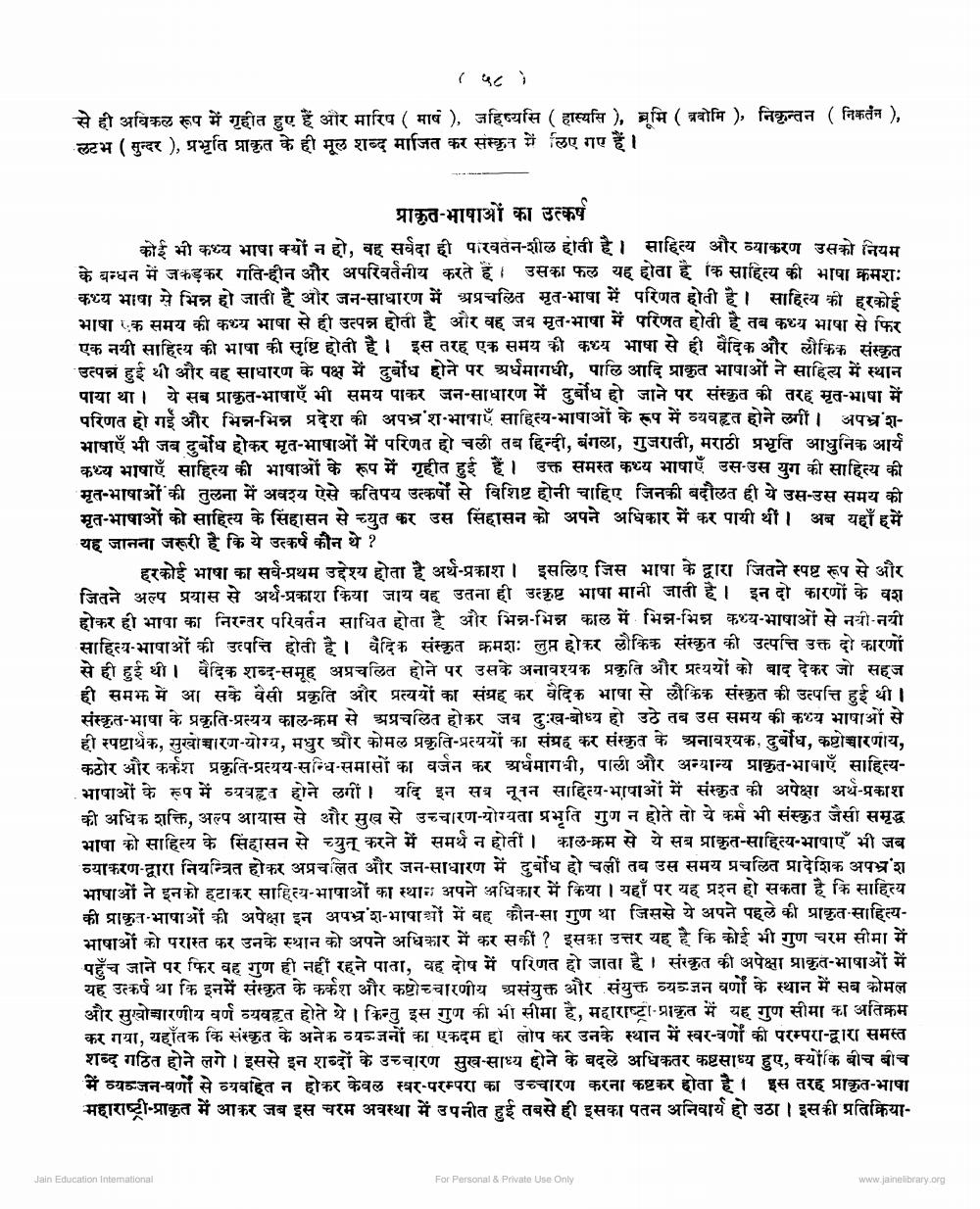________________
( ५८ )
से ही अविकल रूप में गृहीत हुए हैं और मारिप ( मार्ष ), जहिष्यसि ( हास्यसि ), ब्रूमि ( ब्रवोमि ), निकृन्तन ( निकर्तन ), लटभ ( सुन्दर ), प्रभृति प्राकृत के ही मूल शब्द माजित कर संस्कृत में लिए गए हैं ।
प्राकृत भाषाओं का उत्कर्ष
कोई भी कथ्य भाषा क्यों न हो, वह सर्वदा ही परिवर्तन-शील होती है । साहित्य और व्याकरण उसको नियम के बन्धन में जकड़कर गति-हीन और अपरिवर्तनीय करते हैं । उसका फल यह होता है कि साहित्य की भाषा क्रमशः कथ्य भाषा से भिन्न हो जाती है और जन-साधारण में अप्रचलित मृत भाषा में परिणत होती है । साहित्य की हरकोई भाषा एक समय की कथ्य भाषा से ही उत्पन्न होती है और वह जब मृत भाषा में परिणत होती है तब कथ्य भाषा से फिर एक नयी साहित्य की भाषा की सृष्टि होती है । इस तरह एक समय की कध्य भाषा से ही वैदिक और लौकिक संस्कृत उत्पन्न हुई थी और वह साधारण के पक्ष में दुर्बोध होने पर अर्धमागधी, पालि आदि प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में स्थान पाया था। ये सब प्राकृत- भाषाएँ भी समय पाकर जन-साधारण में दुर्बोध हो जाने पर संस्कृत की तरह मृत भाषा में परिणत हो गई और भिन्न-भिन्न प्रदेश की अपभ्रंश भाषाएँ साहित्य भाषाओं के रूप में व्यवहृत होने लगीं। अपभ्रंशभाषाएँ भी जब दुर्बोध होकर मृत भाषाओं में परिणत हो चली तब हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी प्रभृति आधुनिक कथ्य भाषाएँ साहित्य की भाषाओं के रूप में गृहीत हुई हैं । उक्त समस्त कथ्य भाषाएँ उस उस युग की साहित्य की मृत-भाषाओं की तुलना में अवश्य ऐसे कतिपय उत्कर्षो से विशिष्ट होनी चाहिए जिनकी बदौलत ही ये उस-उस समय की मृत भाषाओं को साहित्य के सिंहासन से च्युत कर उस सिंहासन को अपने अधिकार में कर पायी थीं । अब यहाँ हमें यह जानना जरूरी है कि ये उत्कर्ष कौन थे ?
हरकोई भाषा का सर्व प्रथम उद्देश्य होता है अर्थ- प्रकाश । इसलिए जिस भाषा के द्वारा जितने स्पष्ट रूप से और जितने अल्प प्रयास से अर्थ प्रकाश किया जाय वह उतना ही उत्कृष्ट भाषा मानी जाती है। इन दो कारणों के वश होकर ही भाषा का निरन्तर परिवर्तन साधित होता है और भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न कथ्य भाषाओं से नयी-नयी साहित्य भाषाओं की उत्पत्ति होती है । वैदिक संस्कृत क्रमशः लुप्त होकर लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति उक्त दो कारणों से ही हुई थी । वैदिक शब्द समूह अप्रचलित होने पर उसके अनावश्यक प्रकृति और प्रत्ययों को बाद देकर जो सहज ही समझ में आ सके वैसी प्रकृति और प्रत्ययों का संग्रह कर वैदिक भाषा से लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई थी । संस्कृत भाषा के प्रकृति-प्रत्यय काल-क्रम से अप्रचलित होकर जब दुःख बोध्य हो उठे तब उस समय की कथ्य भाषाओं से ही स्पष्टार्थक, सुखोच्चारण-योग्य, मधुर और कोमल प्रकृति-प्रत्ययों का संग्रह कर संस्कृत के अनावश्यक, दुर्बोध, कष्टोच्चारणीय, कठोर और कर्कश प्रकृति-प्रत्यय- सन्धि-समासों का वर्जन कर अर्धमागधी, पाली और अन्यान्य प्राकृत-भाषाएँ साहित्य• भाषाओं के रूप में व्यवहृत होने लगीं। यदि इन सब नूतन साहित्य भाषाओं में संस्कृत की अपेक्षा अर्थ- प्रकाश की अधिक शक्ति, अल्प आयास से और सुख से उच्चारण-योग्यता प्रभृति गुण न होते तो ये कर्म भी संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा को साहित्य के सिंहासन से च्युत करने में समर्थ न होतीं । काल-क्रम से ये सब प्राकृत-साहित्य-भाषाएँ भी जब व्याकरण- द्वारा नियन्त्रित होकर अप्रचलित और जन-साधारण में दुर्बोध हो चलीं तब उस समय प्रचलित प्रादेशिक अपभ्रंश भाषाओं ने इनको हटाकर साहित्य भाषाओं का स्थान अपने अधिकार में किया । यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि साहित्य की प्राकृत भाषाओं की अपेक्षा इन अपभ्रंश भाषाओं में वह कौन-सा गुण था जिससे ये अपने पहले की प्राकृत-साहित्यभाषाओं को परास्त कर उनके स्थान को अपने अधिकार में कर सकीं ? इसका उत्तर यह है कि कोई भी गुण चरम सीमा में पहुँच जाने पर फिर वह गुण ही नहीं रहने पाता, वह दोष में परिणत हो जाता है। संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत भाषाओं में यह उत्कर्ष था कि इनमें संस्कृत के कर्कश और कष्टोच्चारणीय असंयुक्त और संयुक्त व्यञ्जन वर्णों के स्थान सब कोमल और सुखोचारणीय वर्ण व्यवहृत होते थे । किन्तु इस गुण की भी सीमा है, महाराष्ट्री प्राकृत में यह गुण सीमा का अतिक्रम कर गया, यहाँतक कि संस्कृत के अनेक व्यञ्जनों का एकदम हो लोप कर उनके स्थान में स्वर वर्णों की परम्परा द्वारा समस्त शब्द गठित होने लगे । इससे इन शब्दों के उच्चारण सुख-साध्य होने के बदले अधिकतर कष्टसाध्य हुए, क्योंकि बीच बीच में व्यञ्जन वर्णों से व्यवहित न होकर केवल स्वर-परम्परा का उच्चारण करना कष्टकर होता है । इस तरह प्राकृत भाषा महाराष्ट्री प्राकृत में आकर जब इस चरम अवस्था में उपनीत हुई तबसे ही इसका पतन अनिवार्य हो उठा। इसकी प्रतिक्रिया
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org