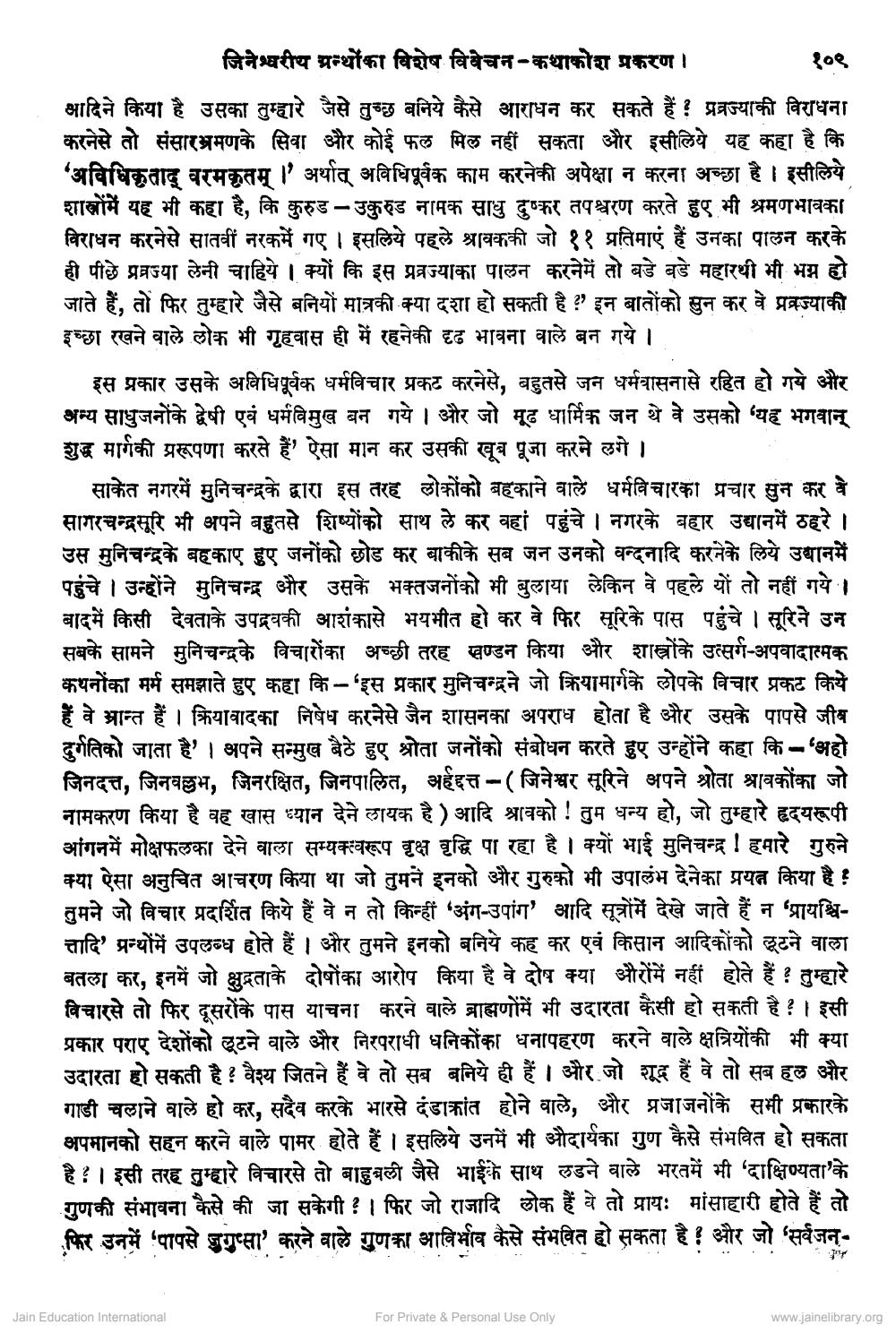________________
जिनेश्वरीय ग्रन्थों का विशेष विवेचन-कथाकोश प्रकरण ।
१०९
आदिने किया है उसका तुम्हारे जैसे तुच्छ बनिये कैसे आराधन कर सकते हैं ? प्रव्रज्याकी विराधना करनेसे तो संसारभ्रमणके सिवा और कोई फल मिल नहीं सकता और इसीलिये यह कहा है कि 'अविधिकृताद् वरमकृतम् ।' अर्थात् अविधिपूर्वक काम करनेकी अपेक्षा न करना अच्छा है । इसीलिये शास्त्रोंमें यह भी कहा है, कि कुरुड - उकुरुड नामक साधु दुष्कर तपश्चरण करते हुए भी श्रमणभावका विराधन करने से सातवीं नरकमें गए । इसलिये पहले श्रावककी जो ११ प्रतिमाएं हैं उनका पालन करके ही पीछे प्रव्रज्या लेनी चाहिये । क्यों कि इस प्रव्रज्याका पालन करनेमें तो बडे बडे महारथी भी भग्न हो जाते हैं, तो फिर तुम्हारे जैसे बनियों मात्रकी क्या दशा हो सकती है ?' इन बातों को सुन कर वे प्रव्रज्याकी इच्छा रखने वाले लोक भी गृहवास ही में रहनेकी दृढ भावना वाले बन गये ।
इस प्रकार उसके अविधिपूर्वक धर्मविचार प्रकट करनेसे, बहुतसे जन धर्मवासना से रहित हो गये और अन्य साधुजनोंके द्वेषी एवं धर्मविमुख बन गये । और जो मूढ धार्मिक जन थे वे उसको 'यह भगवान् शुद्ध मार्गी प्ररूपणा करते हैं' ऐसा मान कर उसकी खूब पूजा करने लगे ।
1
1
साकेत नगर में मुनिचन्द्रके द्वारा इस तरह लोकोंको बहकाने वाले धर्मविचारका प्रचार सुन कर वे सागरचन्द्रसूरि भी अपने बहुतसे शिष्यों को साथ ले कर वहां पहुंचे । नगरके बहार उद्यानमें ठहरे । उस मुनिचन्द्र के बहकाए हुए जनोंको छोड कर बाकी सब जन उनको वन्दनादि करनेके लिये उद्यान में पहुंचे। उन्होंने मुनिचन्द्र और उसके भक्तजनोंको भी बुलाया लेकिन वे पहले यों तो नहीं गये । बाद में किसी देवताके उपद्रवकी आशंकासे भयभीत हो कर वे फिर सूरि के पास पहुंचे । सूरिने उन सबके सामने मुनिचन्द्रके विचारोंका अच्छी तरह खण्डन किया और शास्त्रोंके उत्सर्ग - अपवादात्मक कथनों का मर्म समझाते हुए कहा कि - 'इस प्रकार मुनिचन्द्रने जो क्रियामार्गके लोपके विचार प्रकट किये हैं वे भ्रान्त हैं । क्रियावादका निषेध करनेसे जैन शासनका अपराध होता है और उसके पापसे जीब दुर्गतिको जाता है' । अपने सन्मुख बैठे हुए श्रोता जनोंको संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि - 'अहो जिनदत्त, जिनवल्लभ, जिनरक्षित, जिनपालित, अर्हदत्त - ( जिनेश्वर सूरिने अपने श्रोता श्रावकों का जो नामकरण किया है वह खास ध्यान देने लायक है ) आदि श्रावको ! तुम धन्य हो, जो तुम्हारे हृदयरूपी आंगन में मोक्षफलका देने वाला सम्यक्त्वरूप वृक्ष वृद्धि पा रहा है । क्यों भाई मुनिचन्द्र ! हमारे गुरुने क्या ऐसा अनुचित आचरण किया था जो तुमने इनको और गुरुको भी उपालंभ देनेका प्रयत्न किया है ! तुमने जो विचार प्रदर्शित किये हैं वे न तो किन्हीं 'अंग - उपांग' आदि सूत्रोंमें देखे जाते हैं न 'प्रायश्चितादि' प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं । और तुमने इनको बनिये कह कर एवं किसान आदिकों को लूटने वाला बतला कर, इनमें जो क्षुद्रता के दोषोंका आरोप किया है वे दोष क्या औरोंमें नहीं होते हैं ? तुम्हारे विचारसे तो फिर दूसरोंके पास याचना करने वाले ब्राह्मणोंमें भी उदारता कैसी हो सकती है ? । इसी प्रकार पराए देशोंको लूटने वाले और निरपराधी धनिकोंका धनापहरण करने वाले क्षत्रियोंकी भी क्या उदारता हो सकती है ? वैश्य जितने हैं वे तो सब बनिये ही हैं । और जो शूद्र हैं वे तो सब हल और गाडी चलाने वाले हो कर, सदैव करके भारसे दंडाक्रांत होने वाले, और प्रजाजनोंके सभी प्रकार के अपमानको सहन करने वाले पामर होते हैं । इसलिये उनमें भी औदार्यका गुण कैसे संभवित हो सकता है ? । इसी तरह तुम्हारे विचारसे तो बाहुबली जैसे भाई के साथ लडने वाले भरत में भी 'दाक्षिण्यता' के गुणकी संभावना कैसे की जा सकेगी ? । फिर जो राजादि लोक हैं वे तो प्रायः मांसाहारी होते हैं तो फिर उनमें 'पापसे जुगुप्सा' करने वाले गुणका आविर्भाव कैसे संभवित हो सकता है ? और जो 'सर्वजन -
psp
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org