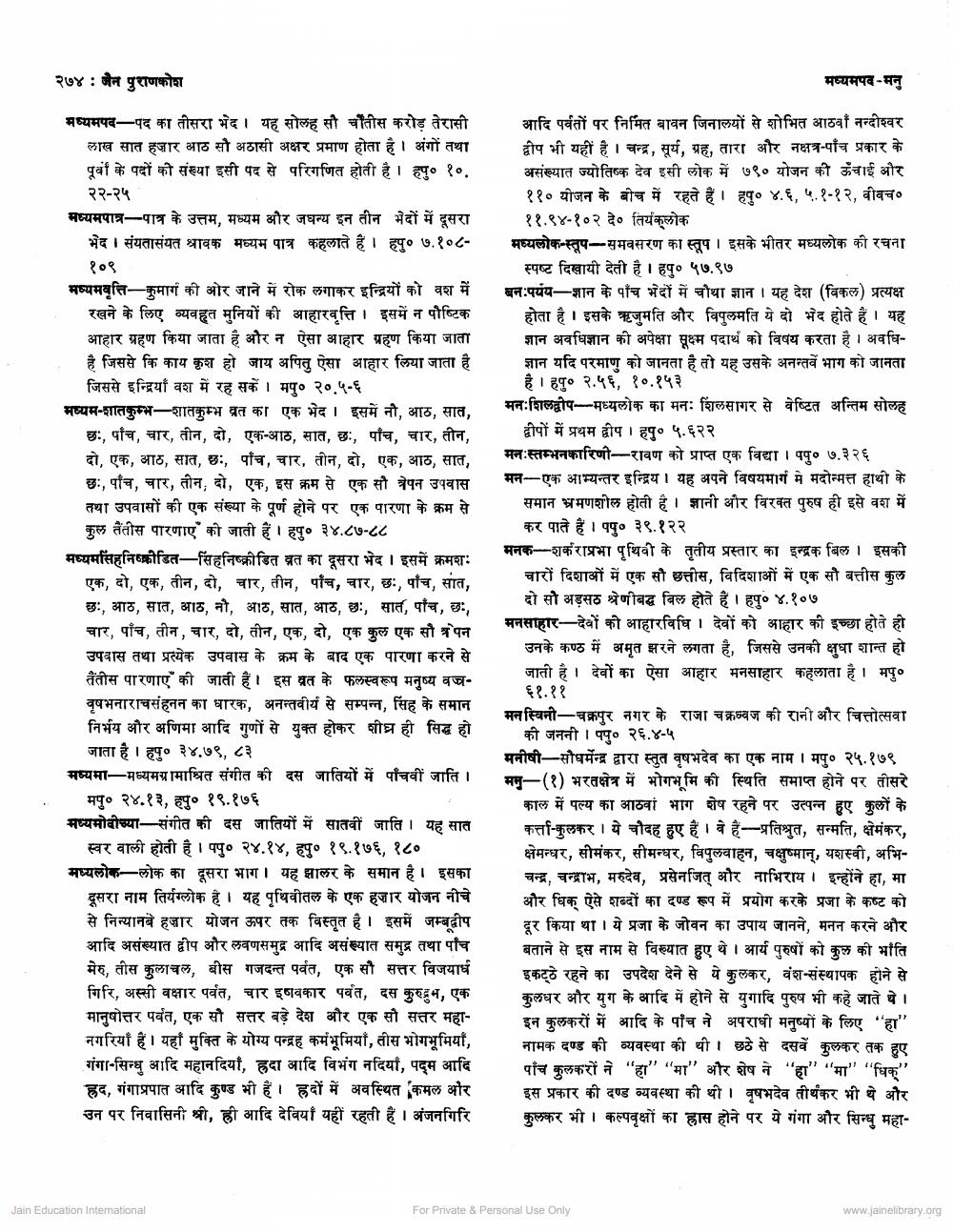________________
२७४ : जैन पुराणकोश
मध्यमपद-मनु
मध्यमपद-पद का तीसरा भेद । यह सोलह सौ चौतीस करोड़ तेरासी
लाख सात हजार आठ सौ अठासी अक्षर प्रमाण होता है। अंगों तथा पूर्वो के पदों की संख्या इसी पद से परिगणित होती है । हपु० १०.
२२-२५ मध्यमपात्र-पात्र के उत्तम, मध्यम और जघन्य इन तीन भेदों में दूसरा
भेद । संयतासंयत श्रावक मध्यम पात्र कहलाते हैं। हपु० ७.१०८
मध्यमवृत्ति-कुमार्ग की ओर जाने में रोक लगाकर इन्द्रियों को वश में रखने के लिए व्यवहृत मुनियों की आहारवृत्ति । इसमें न पौष्टिक आहार ग्रहण किया जाता है और न ऐसा आहार ग्रहण किया जाता है जिससे कि काय कृश हो जाय अपितु ऐसा आहार लिया जाता है जिससे इन्द्रियाँ वश में रह सकें। मपु० २०.५-६ मध्यम-शातकुम्भ-शातकुम्भ व्रत का एक भेद । इसमें नौ, आठ, सात,
छः, पांच, चार, तीन, दो, एक-आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, इस क्रम से एक सौ वेपन उपवास तथा उपवासों की एक संख्या के पूर्ण होने पर एक पारणा के क्रम से
कुल तैंतीस पारणाएं की जाती हैं । हपु० ३४.८७-८८ मध्यमसिंहनिष्क्रीडित-सिंहनिष्क्रीडित व्रत का दूसरा भेद । इसमें क्रमशः
एक, दो, एक, तीन, दो, चार, तीन, पाँच, चार, छः, पाँच, सात, छः, आठ, सात, आठ, नौ, आठ, सात, आठ, छ:, सात, पाँच, छः, चार, पाँच, तीन, चार, दो, तीन, एक, दो, एक कुल एक सौ पन उपवास तथा प्रत्येक उपवास के क्रम के बाद एक पारणा करने से तैंतीस पारणाएं की जाती है। इस व्रत के फलस्वरूप मनुष्य वजवृषभनाराचसंहनन का धारक, अनन्तवीर्य से सम्पन्न, सिंह के समान निर्भय और अणिमा आदि गुणों से युक्त होकर शीघ्र ही सिद्ध हो
जाता है । हपु० ३४.७९, ८३ मध्यमा-मध्यमग्रामाश्रित संगीत की दस जातियों में पांचवीं जाति ।
मपु० २४.१३, हपु० १९.१७६ मध्यमोबीच्या-संगीत की दस जातियों में सातवीं जाति । यह सात
स्वर वाली होती है । पपु० २४.१४, हपु० १९.१७६, १८० मध्यलोक-लोक का दूसरा भाग। यह झालर के समान है। इसका
दूसरा नाम तिर्यग्लोक है। यह पृथिवीतल के एक हजार योजन नीचे से निन्यानबे हजार योजन ऊपर तक विस्तृत है। इसमें जम्बूद्वीप आदि असंख्यात द्वीप और लवणसमुद्र आदि असंख्यात समुद्र तथा पांच मेरु, तीस कुलाचल, बीस गजदन्त पर्वत, एक सौ सत्तर विजया गिरि, अस्सी वक्षार पर्वत, चार इषवकार पर्वत, दस कुरुद्रुभ, एक मानुषोत्तर पर्वत, एक सौ सत्तर बड़े देश और एक सौ सत्तर महानगरियाँ हैं। यहाँ मुक्ति के योग्य पन्द्रह कर्मभूमियाँ, तीस भोगभूमियाँ, गंगा-सिन्धु आदि महानदियाँ, ह्रदा आदि विभंग नदियाँ, पद्म आदि ह्रद, गंगाप्रपात आदि कुण्ड भी हैं। ह्रदों में अवस्थित कमल और उन पर निवासिनी श्री, ह्री आदि देवियाँ यहीं रहती हैं । अंजनगिरि
आदि पर्वतों पर निर्मित बावन जिनालयों से शोभित आठवाँ नन्दीश्वर द्वीप भी यहीं है । चन्द्र, सूर्य, ग्रह, तारा और नक्षत्र-पाँच प्रकार के असंख्यात ज्योतिष्क देव इसी लोक में ७९० योजन की ऊँचाई और ११० योजन के बीच में रहते हैं। हपु० ४.६, ५.१-१२, वीवच० ११.९४-१०२ दे० तिर्यक्लोक मध्यलोक-स्तूप-समवसरण का स्तूप । इसके भीतर मध्यलोक की रचना
स्पष्ट दिखायी देती है । हपु० ५७.९७ बनःपर्यय-ज्ञान के पाँच भेदों में चौथा ज्ञान । यह देश (विकल) प्रत्यक्ष होता है । इसके ऋजुमति और विपुलमति ये दो भेद होते हैं। यह ज्ञान अवधिज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म पदार्थ को विषय करता है । अवधिज्ञान यदि परमाणु को जानता है तो यह उसके अनन्तवें भाग को जानता
है । हपु० २.५६, १०.१५३ मनःशिलद्वीप-मध्यलोक का मनः शिलसागर से वेष्टित अन्तिम सोलह
द्वीपों में प्रथम द्वीप । हपु० ५.६२२ मनःस्तम्भनकारिणी-रावण को प्राप्त एक विद्या । पपु० ७.३२६ मन-एक आभ्यन्तर इन्द्रिय । यह अपने विषयमार्ग मे मदोन्मत्त हाथी के
समान भ्रमणशील होती है। ज्ञानी और विरक्त पुरुष ही इसे वश में
कर पाते हैं । पपु० ३९.१२२ । मनक-शर्कराप्रभा पृथिवी के तृतीय प्रस्तार का इन्द्रक बिल । इसकी
चारों दिशाओं में एक सौ छत्तीस, विदिशाओं में एक सौ बत्तीस कुल
दो सौ अड़सठ श्रेणीबद्ध बिल होते हैं । हपु० ४.१०७ मनसाहार-देवों को आहारविधि । देवों को आहार की इच्छा होते ही
उनके कण्ठ में अमृत झरने लगता है, जिससे उनकी क्षुधा शान्त हो जाती है। देवों का ऐसा आहार मनसाहार कहलाता है। मपु.
६१.११ मनस्विनी-चक्रपुर नगर के राजा चक्रध्वज की रानी और चित्तोत्सवा ___की जननी । पपु० २६.४-५ मनीषी-सौधर्मेन्द्र द्वारा स्तुत वृषभदेव का एक नाम । मपु० २५.१७९ मनु-(१) भरतक्षेत्र में भोगभूमि की स्थिति समाप्त होने पर तीसरे
काल में पल्य का आठवां भाग शेष रहने पर उत्पन्न हुए कुलों के कर्ता-कुलकर । ये चौदह हुए हैं । वे हैं-प्रतिश्रुत, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमन्धर, सीमंकर, सीमन्धर, विपुलवाहन, चक्षुष्मान्, यशस्वी, अभिचन्द्र, चन्द्राभ, मरुदेव, प्रसेनजित् और नाभिराय । इन्होंने हा, मा और धिक् ऐसे शब्दों का दण्ड रूप में प्रयोग करके प्रजा के कष्ट को दूर किया था। ये प्रजा के जीवन का उपाय जानने, मनन करने और बताने से इस नाम से विख्यात हुए थे। आर्य पुरुषों को कुल की भांति इकट्ठे रहने का उपदेश देने से ये कुलकर, वंश-संस्थापक होने से कुलधर और युग के आदि में होने से युगादि पुरुष भी कहे जाते थे। इन कुलकरों में आदि के पांच ने अपराधी मनुष्यों के लिए "हा" नामक दण्ड की व्यवस्था की थी। छठे से दसवें कुलकर तक हुए पाँच कुलकरों ने "हा" "मा" और शेष ने "हा" "मा" "धिक" इस प्रकार की दण्ड व्यवस्था की थी। वृषभदेव तीर्थंकर भी थे और कुलकर भी। कल्पवृक्षों का ह्रास होने पर ये गंगा और सिन्धु महा
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org