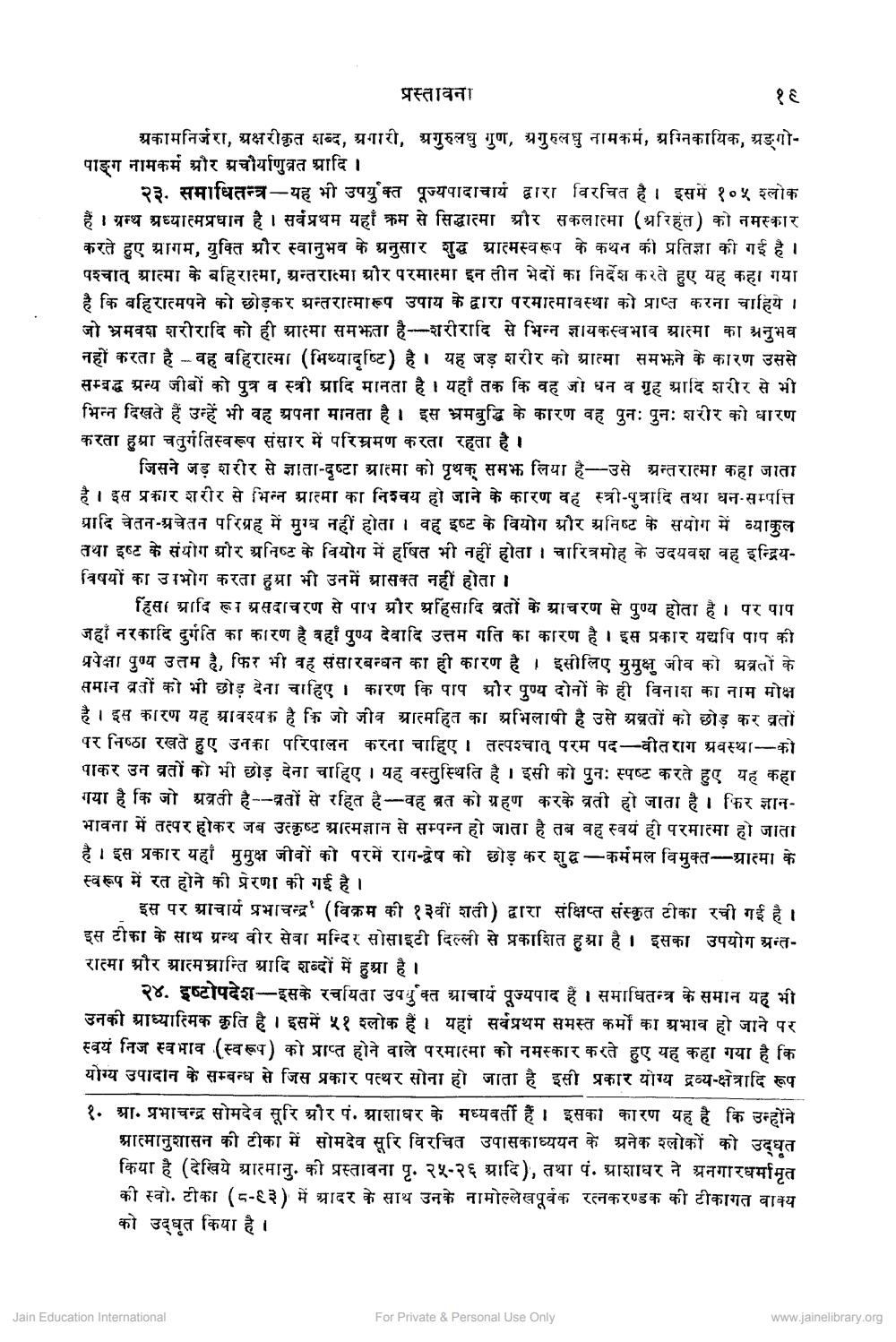________________
प्रस्तावना
१६
अकामनिर्जरा, अक्षरीकृत शब्द, अगारी, अगुरुलघु गुण, अगुरुलघु नामकर्म, अग्निकायिक, अङ्गोपाङ्ग नामकर्म और अचोर्याणुव्रत प्रादि ।
२३. समाधितन्त्र-यह भी उपयुक्त पूज्यपादाचार्य द्वारा विरचित है। इसमें १०५ श्लोक हैं । ग्रन्थ अध्यात्मप्रधान है। सर्वप्रथम यहाँ क्रम से सिद्धात्मा और सकलात्मा (अरिहंत) को नमस्कार करते हुए पागम, युक्ति और स्वानुभव के अनुसार शुद्ध प्रात्मस्वरूप के कथन की प्रतिज्ञा की गई है। पश्चात् आत्मा के बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन तीन भेदों का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि बहिरात्मपने को छोड़कर अन्तरात्मारूप उपाय के द्वारा परमात्मावस्था को प्राप्त करना चाहिये । जो भ्रमवश शरीरादि को ही प्रात्मा समझता है-शरीरादि से भिन्न ज्ञायकस्वभाव प्रात्मा का अनुभव नहीं करता है - वह बहिरात्मा (मिथ्याष्टि) है। यह जड़ शरीर को प्रात्मा समझने के कारण उससे सम्बद्ध अन्य जीबों को पुत्र व स्त्री आदि मानता है। यहाँ तक कि वह जो धन व गृह आदि शरीर से भी भिन्न दिखते हैं उन्हें भी वह अपना मानता है। इस भ्रमबुद्धि के कारण वह पुनः पुनः शरीर को धारण करता हुमा चतुर्गतिस्वरूप संसार में परिम्रमण करता रहता है।
जिसने जड़ शरीर से ज्ञाता-दृष्टा आत्मा को पृथक् समझ लिया है-उसे अन्तरात्मा कहा जाता है। इस प्रकार शरीर से भिन्न प्रात्मा का निश्चय हो जाने के कारण वह स्त्री-पुत्रादि तथा धन-सम्पत्ति प्रादि चेतन-अचेतन परिग्रह में मुग्ध नहीं होता। वह इष्ट के वियोग और अनिष्ट के सयोग में व्याकुल तथा इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग में हर्षित भी नहीं होता। चारित्रमोह के उदयवश वह इन्द्रियविषयों का उपभोग करता हना भी उनमें प्रासक्त नहीं होता।
हिंसा आदि रूप असदाचरण से पाप और अहिंसादि व्रतों के आचरण से पुण्य होता है। पर पाप जहाँ नरकादि दुर्गति का कारण है वहाँ पुण्य देवादि उत्तम गति का कारण है । इस प्रकार यद्यपि पाप की प्रपेक्षा पुण्य उत्तम है, फिर भी वह संसारबन्धन का ही कारण है । इसीलिए मुमुक्षु जीव को अव्रतों के समान व्रतों को भी छोड़ देना चाहिए। कारण कि पाप और पुण्य दोनों के ही विनाश का नाम मोक्ष है। इस कारण यह प्रावश्यक है कि जो जीव आत्महित का अभिलाषी है उसे अव्रतों को छोड़ कर व्रतों पर निष्ठा रखते हुए उनका परिपालन करना चाहिए। तत्पश्चात् परम पद-वीतराग अवस्था-को पाकर उन व्रतों को भी छोड़ देना चाहिए। यह वस्तुस्थिति है । इसी को पुनः स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि जो अव्रती है--व्रतों से रहित है-वह ब्रत को ग्रहण करके व्रती हो जाता है। फिर ज्ञानभावना में तत्पर होकर जब उत्कृष्ट आत्मज्ञान से सम्पन्न हो जाता है तब वह स्वयं ही परमात्मा हो जाता है। इस प्रकार यहाँ मुमुक्ष जीवों को परमें राग-द्वेष को छोड़ कर शुद्ध-कर्ममल विमुक्त-प्रात्मा के स्वरूप में रत होने की प्रेरणा की गई है।
इस पर प्राचार्य प्रभाचन्द्र' (विक्रम की १३वीं शती) द्वारा संक्षिप्त संस्कृत टीका रची गई है। इस टीका के साथ ग्रन्थ वीर सेवा मन्दिर सोसाइटी दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग अन्तरात्मा और आत्मम्रान्ति आदि शब्दों में हमा है।
२४. इष्टोपदेश-इसके रचयिता उपर्युक्त आचार्य पूज्यपाद हैं । समाधितन्त्र के समान यह भी उनकी आध्यात्मिक कृति है। इसमें ५१ श्लोक हैं। यहां सर्वप्रथम समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर स्वयं निज स्वभाव (स्वरूप) को प्राप्त होने वाले परमात्मा को नमस्कार करते हुए यह कहा गया है कि योग्य उपादान के सम्बन्ध से जिस प्रकार पत्थर सोना हो जाता है इसी प्रकार योग्य द्रव्य-क्षेत्रादि रूप १. प्रा. प्रभाचन्द्र सोमदेव सूरि और पं. पाशाघर के मध्यवर्ती हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने
आत्मानुशासन की टीका में सोमदेव सूरि विरचित उपासकाध्ययन के अनेक श्लोकों को उदधत किया है (देखिये प्रात्मानु. की प्रस्तावना पृ. २५-२६ आदि), तथा पं. प्राशाधर ने अनगारधर्मामृत की स्वो. टीका (८-६३) में प्रादर के साथ उनके नामोल्लेखपूर्वक रत्नकरण्डक की टीकागत वाक्य को उद्धृत किया है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org