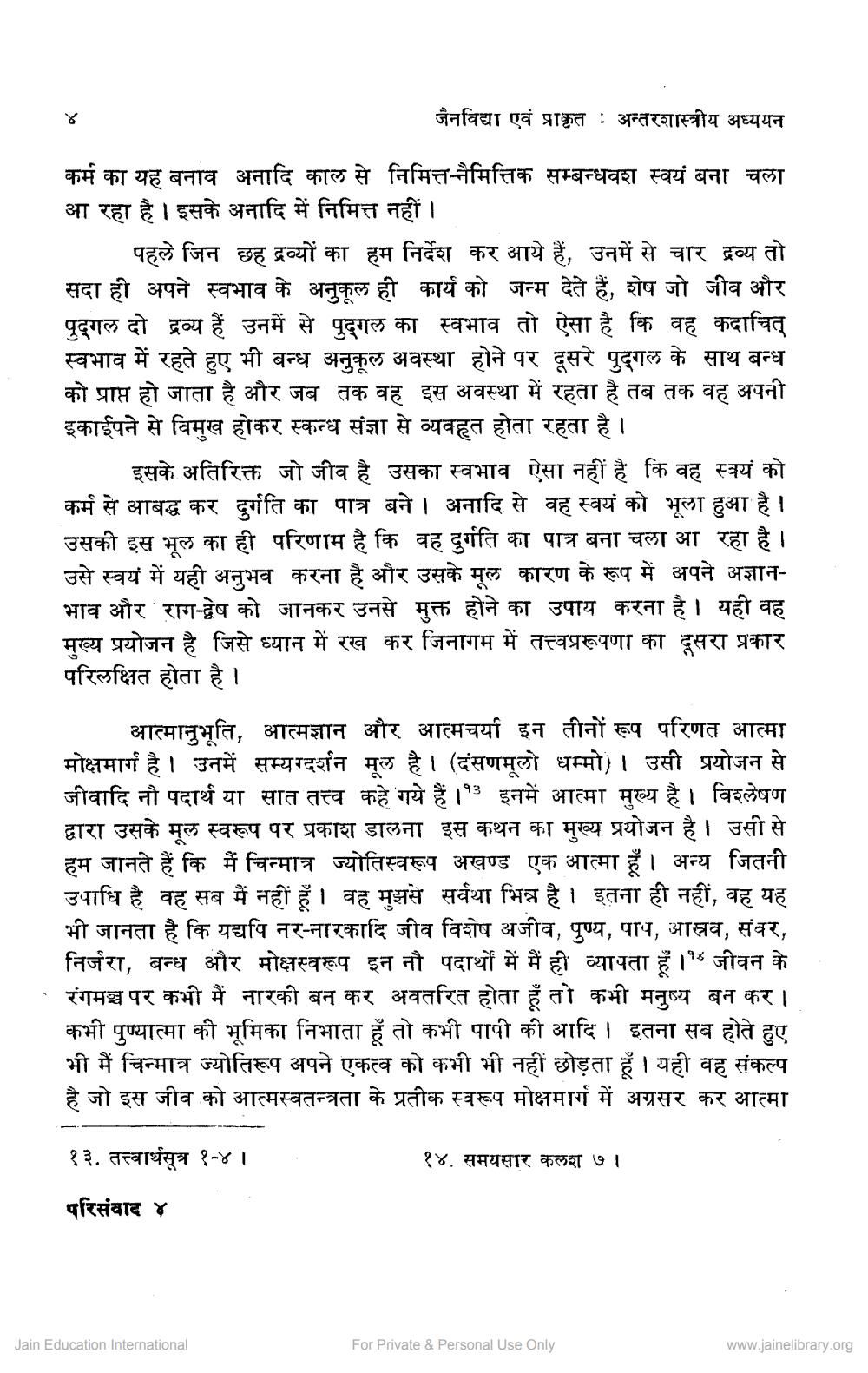________________
जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन
कर्म का यह बनाव अनादि काल से निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धवश स्वयं बना चला आ रहा है । इसके अनादि में निमित्त नहीं।
पहले जिन छह द्रव्यों का हम निर्देश कर आये हैं, उनमें से चार द्रव्य तो सदा ही अपने स्वभाव के अनुकूल ही कार्य को जन्म देते हैं, शेष जो जीव और पुद्गल दो द्रव्य हैं उनमें से पुद्गल का स्वभाव तो ऐसा है कि वह कदाचित् स्वभाव में रहते हुए भी बन्ध अनुकूल अवस्था होने पर दूसरे पुद्गल के साथ बन्ध को प्राप्त हो जाता है और जब तक वह इस अवस्था में रहता है तब तक वह अपनी इकाईपने से विमुख होकर स्कन्ध संज्ञा से व्यवहृत होता रहता है ।
इसके अतिरिक्त जो जीव है उसका स्वभाव ऐसा नहीं है कि वह स्वयं को कर्म से आबद्ध कर दुर्गति का पात्र बने। अनादि से वह स्वयं को भूला हुआ है। उसकी इस भूल का ही परिणाम है कि वह दुर्गति का पात्र बना चला आ रहा है। उसे स्वयं में यही अनुभव करना है और उसके मूल कारण के रूप में अपने अज्ञानभाव और राग-द्वेष को जानकर उनसे मुक्त होने का उपाय करना है। यही वह मुख्य प्रयोजन है जिसे ध्यान में रख कर जिनागम में तत्त्वप्ररूपणा का दूसरा प्रकार परिलक्षित होता है।
आत्मानुभूति, आत्मज्ञान और आत्मचर्या इन तीनों रूप परिणत आत्मा मोक्षमार्ग है। उनमें सम्यग्दर्शन मूल है। (दसणमूलो धम्मो)। उसी प्रयोजन से जीवादि नौ पदार्थ या सात तत्त्व कहे गये हैं। इनमें आत्मा मुख्य है। विश्लेषण द्वारा उसके मूल स्वरूप पर प्रकाश डालना इस कथन का मुख्य प्रयोजन है। उसी से हम जानते हैं कि मैं चिन्मात्र ज्योतिस्वरूप अखण्ड एक आत्मा हूँ। अन्य जितनी उपाधि है वह सब मैं नहीं हूँ। वह मुझसे सर्वथा भिन्न है। इतना ही नहीं, वह यह भी जानता है कि यद्यपि नर-नारकादि जीव विशेष अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्षस्वरूप इन नौ पदार्थों में मैं ही व्यापता हूँ। जीवन के रंगमञ्च पर कभी मैं नारकी बन कर अवतरित होता हूँ तो कभी मनुष्य बन कर । कभी पुण्यात्मा की भूमिका निभाता हूँ तो कभी पापी की आदि। इतना सब होते हुए भी मैं चिन्मात्र ज्योतिरूप अपने एकत्व को कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। यही वह संकल्प है जो इस जीव को आत्मस्वतन्त्रता के प्रतीक स्वरूप मोक्षमार्ग में अग्रसर कर आत्मा
१४. समयसार कलश ७ ।
१३. तत्त्वार्थसूत्र १-४ । परिसंवाद ४
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org