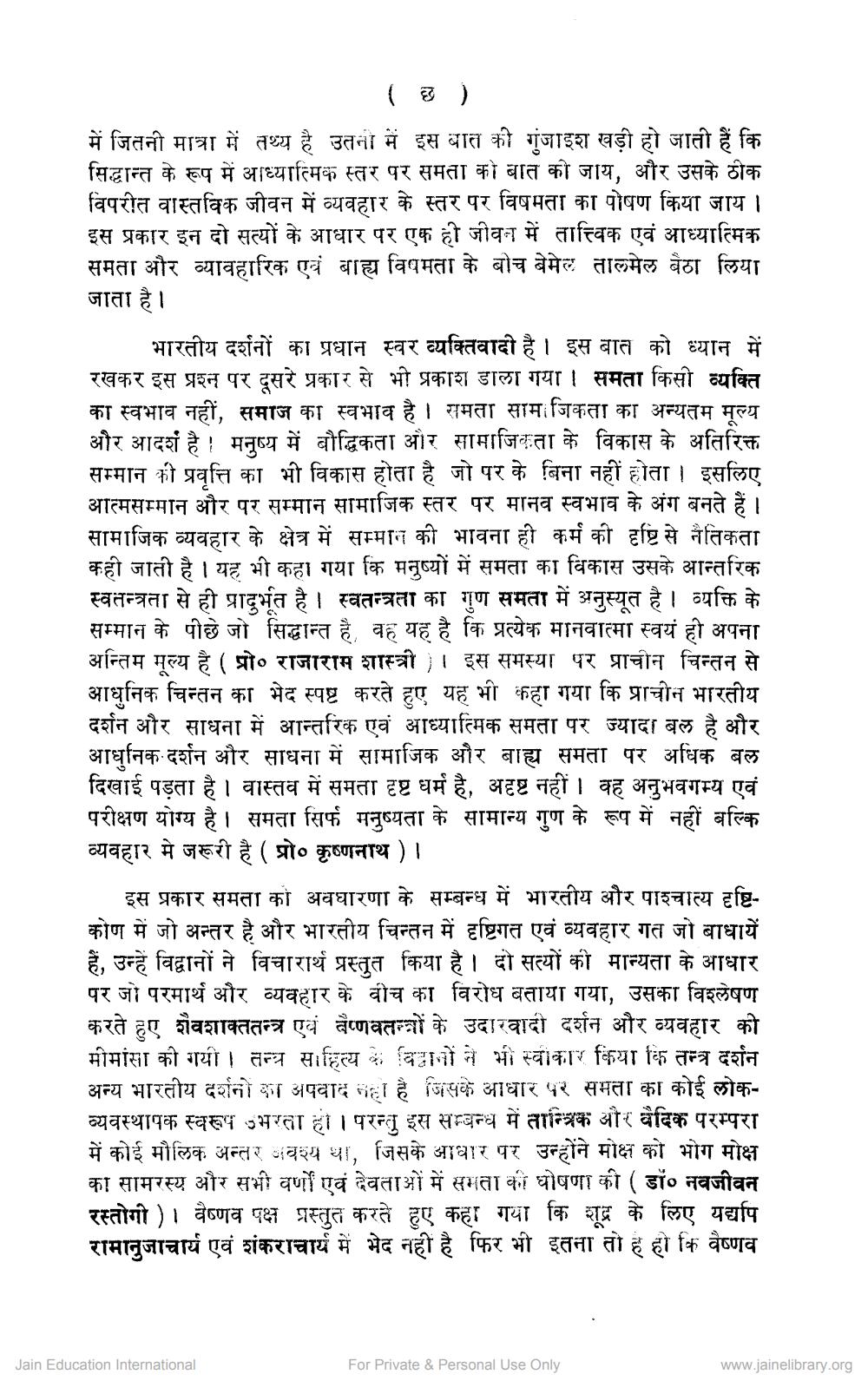________________
में जितनी मात्रा में तथ्य है उतना में इस बात की गुंजाइश खड़ी हो जाती हैं कि सिद्धान्त के रूप में आध्यात्मिक स्तर पर समता को बात को जाय, और उसके ठीक विपरीत वास्तविक जीवन में व्यवहार के स्तर पर विषमता का पोषण किया जाय । इस प्रकार इन दो सत्यों के आधार पर एक ही जीवन में तात्त्विक एवं आध्यात्मिक समता और व्यावहारिक एवं बाह्य विषमता के बीच बेमेल तालमेल बैठा लिया जाता है।
भारतीय दर्शनों का प्रधान स्वर व्यक्तिवादी है। इस बात को ध्यान में रखकर इस प्रश्न पर दूसरे प्रकार से भी प्रकाश डाला गया। समता किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं, समाज का स्वभाव है। समता सामाजिकता का अन्यतम मूल्य और आदर्श है। मनुष्य में बौद्धिकता और सामाजिकता के विकास के अतिरिक्त सम्मान की प्रवृत्ति का भी विकास होता है जो पर के बिना नहीं होता। इसलिए आत्मसम्मान और पर सम्मान सामाजिक स्तर पर मानव स्वभाव के अंग बनते हैं । सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र में सम्मान की भावना ही कर्म की दृष्टि से नैतिकता कही जाती है । यह भी कहा गया कि मनुष्यों में समता का विकास उसके आन्तरिक स्वतन्त्रता से ही प्रादुर्भूत है। स्वतन्त्रता का गुण समता में अनुस्यूत है। व्यक्ति के सम्मान के पीछे जो सिद्धान्त है, वह यह है कि प्रत्येक मानवात्मा स्वयं ही अपना अन्तिम मूल्य है (प्रो० राजाराम शास्त्री । इस समस्या पर प्राचीन चिन्तन से आधुनिक चिन्तन का भेद स्पष्ट करते हुए यह भी कहा गया कि प्राचीन भारतीय दर्शन और साधना में आन्तरिक एवं आध्यात्मिक समता पर ज्यादा बल है और आधुनिक दर्शन और साधना में सामाजिक और बाह्य समता पर अधिक बल दिखाई पड़ता है। वास्तव में समता दृष्ट धर्म है, अदृष्ट नहीं। वह अनुभवगम्य एवं परीक्षण योग्य है। समता सिर्फ मनुष्यता के सामान्य गुण के रूप में नहीं बल्कि व्यवहार में जरूरी है (प्रो० कृष्णनाथ )।
इस प्रकार समता को अवधारणा के सम्बन्ध में भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण में जो अन्तर है और भारतीय चिन्तन में दृष्टिगत एवं व्यवहार गत जो बाधायें हैं, उन्हें विद्वानों ने विचारार्थ प्रस्तुत किया है। दो सत्यों की मान्यता के आधार पर जो परमार्थ और व्यवहार के बीच का विरोध बताया गया, उसका विश्लेषण करते हुए शैवशाक्ततन्त्र एवं वैष्णवतन्त्रों के उदारवादी दर्शन और व्यवहार को मीमांसा की गयी। तन्त्र साहित्य के विद्वानों ने भी स्वाकार किया कि तन्त्र दर्शन अन्य भारतीय दर्शनों का अपवाद नहा है जिसके आधार पर समता का कोई लोकव्यवस्थापक स्वरूप उभरता हो । परन्तु इस सम्बन्ध में तान्त्रिक और वैदिक परम्परा में कोई मौलिक अन्त र अवश्य था, जिसके आधार पर उन्होंने मोक्ष को भोग मोक्ष का सामरस्य और सभी वर्गों एवं देवताओं में समता की घोषणा की ( डॉ० नवजीवन रस्तोगी)। वैष्णव पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि शूद्र के लिए यद्यपि रामानुजाचार्य एवं शंकराचार्य में भेद नहीं है फिर भी इतना तो है हो कि वैष्णव
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org