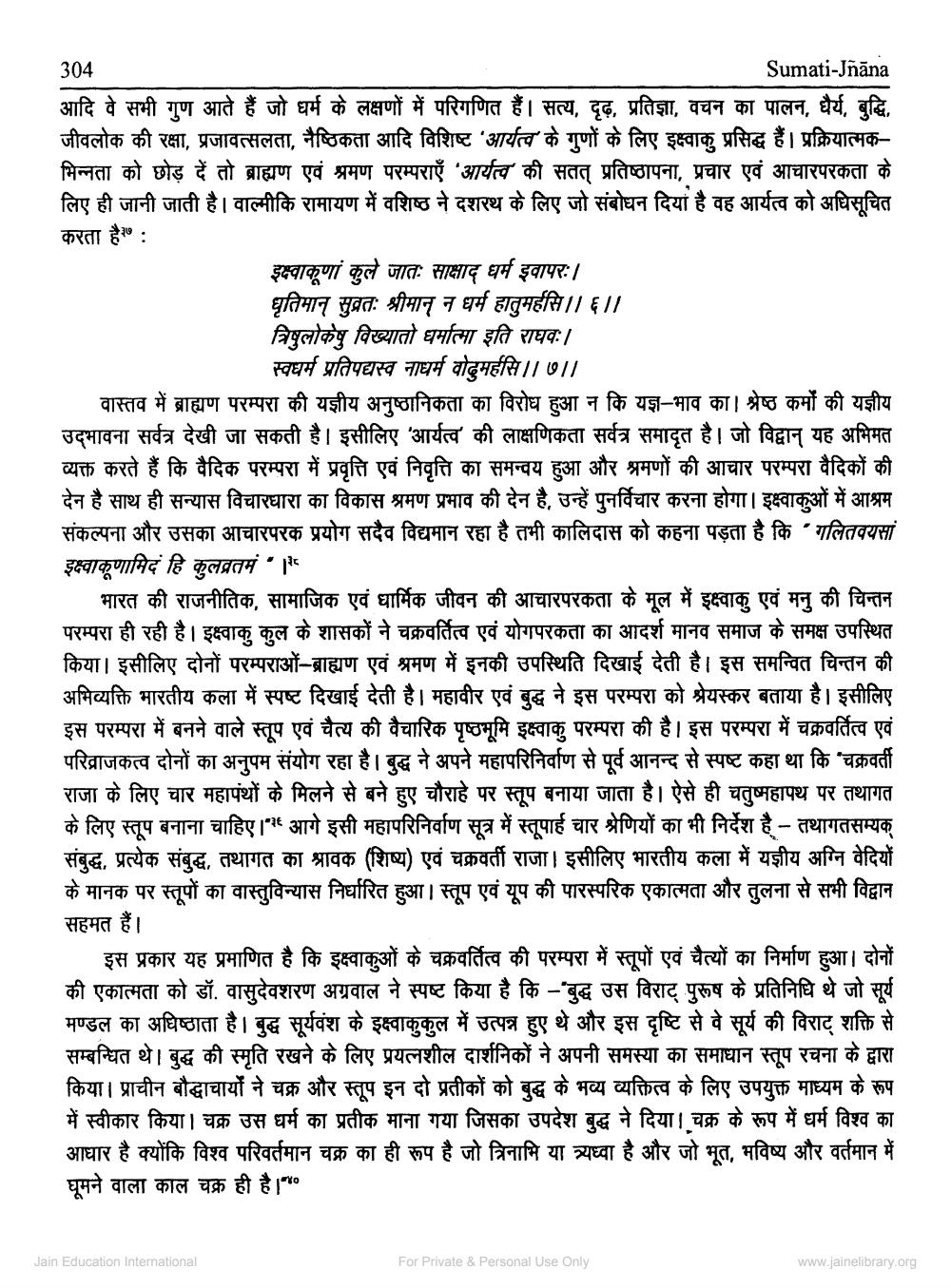________________
304
Sumati-Jnana आदि वे सभी गुण आते हैं जो धर्म के लक्षणों में परिगणित हैं। सत्य, दृढ़, प्रतिज्ञा, वचन का पालन, धैर्य, बुद्धि, जीवलोक की रक्षा, प्रजावत्सलता, नैष्ठिकता आदि विशिष्ट 'आर्यत्व के गुणों के लिए इक्ष्वाकु प्रसिद्ध हैं। प्रक्रियात्मकभिन्नता को छोड़ दें तो ब्राह्मण एवं श्रमण परम्पराएँ 'आर्यत्व की सतत् प्रतिष्ठापना, प्रचार एवं आचारपरकता के लिए ही जानी जाती है। वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ ने दशरथ के लिए जो संबोधन दिया है वह आर्यत्व को अधिसूचित करता है३७ :
इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद् धर्म इवापरः। धृतिमान सुव्रतः श्रीमान् न धर्म हातुमर्हसि।। ६ ।। त्रिषुलोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः ।
स्वधर्म प्रतिपद्यस्व नाधर्म वोढुमर्हसि।। ७।। वास्तव में ब्राह्यण परम्परा की यज्ञीय अनुष्ठानिकता का विरोध हुआ न कि यज्ञ-भाव का। श्रेष्ठ कमों की यज्ञीय उद्भावना सर्वत्र देखी जा सकती है। इसीलिए 'आर्यत्व' की लाक्षणिकता सर्वत्र समादृत है। जो विद्वान यह अभिमत व्यक्त करते हैं कि वैदिक परम्परा में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का समन्वय हुआ और श्रमणों की आचार परम्परा वैदिकों की देन है साथ ही सन्यास विचारधारा का विकास श्रमण प्रभाव की देन है, उन्हें पुनर्विचार करना होगा। इक्ष्वाकुओं में आश्रम संकल्पना और उसका आचारपरक प्रयोग सदैव विद्यमान रहा है तभी कालिदास को कहना पड़ता है कि “गलितवयसां इक्ष्वाकूणामिदं हि कुलव्रतमं । ____भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की आचारपरकता के मूल में इक्ष्वाकु एवं मनु की चिन्तन परम्परा ही रही है। इक्ष्वाकु कुल के शासकों ने चक्रवर्तित्व एवं योगपरकता का आदर्श मानव समाज के समक्ष उपस्थित किया। इसीलिए दोनों परम्पराओं-ब्राह्मण एवं श्रमण में इनकी उपस्थिति दिखाई देती है। इस समन्वित चिन्तन की अभिव्यक्ति भारतीय कला में स्पष्ट दिखाई देती है। महावीर एवं बुद्ध ने इस परम्परा को श्रेयस्कर बताया है। इसीलिए इस परम्परा में बनने वाले स्तूप एवं चैत्य की वैचारिक पृष्ठभूमि इक्ष्वाकु परम्परा की है। इस परम्परा में चक्रवर्तित्व एवं परिव्राजकत्व दोनों का अनुपम संयोग रहा है। बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व आनन्द से स्पष्ट कहा था कि 'चक्रवर्ती राजा के लिए चार महापंथों के मिलने से बने हुए चौराहे पर स्तूप बनाया जाता है। ऐसे ही चतुष्महापथ पर तथागत के लिए स्तूप बनाना चाहिए। आगे इसी महापरिनिर्वाण सूत्र में स्तूपार्ह चार श्रेणियों का भी निर्देश है - तथागतसम्यक् संबुद्ध, प्रत्येक संबुद्ध, तथागत का श्रावक (शिष्य) एवं चक्रवर्ती राजा। इसीलिए भारतीय कला में यज्ञीय अग्नि वेदियों के मानक पर स्तूपों का वास्तुविन्यास निर्धारित हुआ। स्तूप एवं यूप की पारस्परिक एकात्मता और तुलना से सभी विद्वान सहमत हैं। ___ इस प्रकार यह प्रमाणित है कि इक्ष्वाकुओं के चक्रवर्तित्व की परम्परा में स्तूपों एवं चैत्यों का निर्माण हुआ। दोनों की एकात्मता को डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि –'बुद्ध उस विराट् पुरूष के प्रतिनिधि थे जो सूर्य मण्डल का अधिष्ठाता है। बुद्ध सूर्यवंश के इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न हुए थे और इस दृष्टि से वे सूर्य की विराट् शक्ति से सम्बन्धित थे। बुद्ध की स्मृति रखने के लिए प्रयत्नशील दार्शनिकों ने अपनी समस्या का समाधान स्तूप रचना के द्वारा किया। प्राचीन बौद्धाचार्यों ने चक्र और स्तूप इन दो प्रतीकों को बुद्ध के भव्य व्यक्तित्व के लिए उपयुक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया। चक्र उस धर्म का प्रतीक माना गया जिसका उपदेश बुद्ध ने दिया। चक्र के रूप में धर्म विश्व का आधार है क्योंकि विश्व परिवर्तमान चक्र का ही रूप है जो त्रिनामि या त्र्यध्वा है और जो भूत, भविष्य और वर्तमान में घूमने वाला काल चक्र ही है।"०
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org