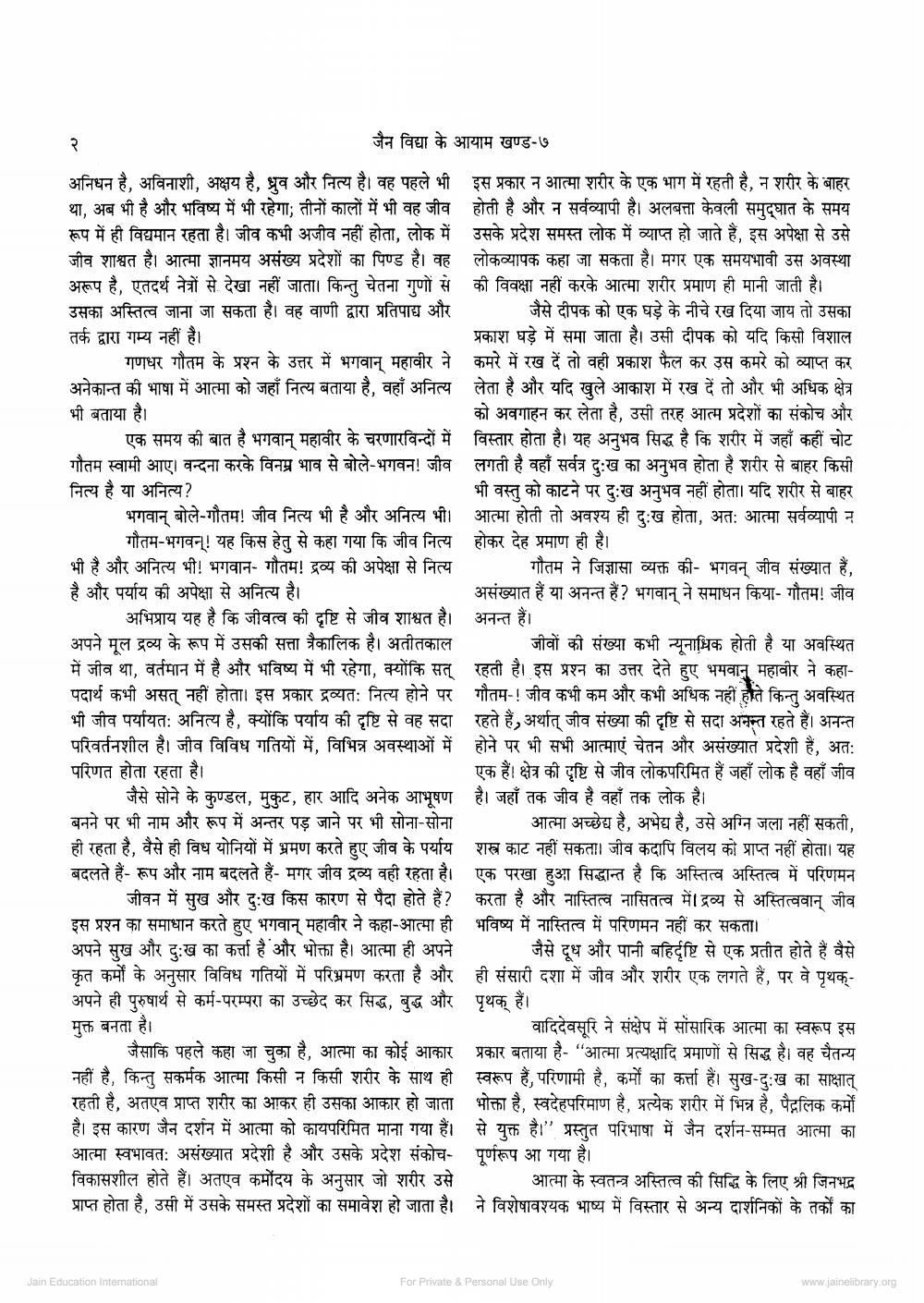________________
जैन विद्या के आयाम खण्ड-७
अनिधन है, अविनाशी, अक्षय है, ध्रुव और नित्य है। वह पहले भी इस प्रकार न आत्मा शरीर के एक भाग में रहती है, न शरीर के बाहर था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा; तीनों कालों में भी वह जीव होती है और न सर्वव्यापी है। अलबत्ता केवली समुद्घात के समय रूप में ही विद्यमान रहता है। जीव कभी अजीव नहीं होता, लोक में उसके प्रदेश समस्त लोक में व्याप्त हो जाते हैं, इस अपेक्षा से उसे जीव शाश्वत है। आत्मा ज्ञानमय असंख्य प्रदेशों का पिण्ड है। वह लोकव्यापक कहा जा सकता है। मगर एक समयभावी उस अवस्था अरूप है, एतदर्थ नेत्रों से देखा नहीं जाता। किन्तु चेतना गुणों से की विवक्षा नहीं करके आत्मा शरीर प्रमाण ही मानी जाती है। उसका अस्तित्व जाना जा सकता है। वह वाणी द्वारा प्रतिपाद्य और जैसे दीपक को एक घड़े के नीचे रख दिया जाय तो उसका तर्क द्वारा गम्य नहीं है।
प्रकाश घड़े में समा जाता है। उसी दीपक को यदि किसी विशाल गणधर गौतम के प्रश्न के उत्तर में भगवान् महावीर ने कमरे में रख दें तो वही प्रकाश फैल कर उस कमरे को व्याप्त कर अनेकान्त की भाषा में आत्मा को जहाँ नित्य बताया है, वहाँ अनित्य लेता है और यदि खुले आकाश में रख दें तो और भी अधिक क्षेत्र भी बताया है।
को अवगाहन कर लेता है, उसी तरह आत्म प्रदेशों का संकोच और एक समय की बात है भगवान् महावीर के चरणारविन्दों में विस्तार होता है। यह अनुभव सिद्ध है कि शरीर में जहाँ कहीं चोट गौतम स्वामी आए। वन्दना करके विनम्र भाव से बोले-भगवन! जीव लगती है वहाँ सर्वत्र दु:ख का अनुभव होता है शरीर से बाहर किसी नित्य है या अनित्य?
भी वस्तु को काटने पर दु:ख अनुभव नहीं होता। यदि शरीर से बाहर भगवान् बोले-गौतम! जीव नित्य भी है और अनित्य भी। आत्मा होती तो अवश्य ही दुःख होता, अत: आत्मा सर्वव्यापी न
गौतम-भगवन्! यह किस हेतु से कहा गया कि जीव नित्य होकर देह प्रमाण ही है। भी है और अनित्य भी! भगवान- गौतम! द्रव्य की अपेक्षा से नित्य गौतम ने जिज्ञासा व्यक्त की- भगवन् जीव संख्यात हैं, है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है।
असंख्यात हैं या अनन्त हैं? भगवान् ने समाधन किया- गौतम! जीव अभिप्राय यह है कि जीवत्व की दृष्टि से जीव शाश्वत है। अनन्त हैं। अपने मूल द्रव्य के रूप में उसकी सत्ता त्रैकालिक है। अतीतकाल जीवों की संख्या कभी न्यूनाधिक होती है या अवस्थित में जीव था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि सत् रहती है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने कहापदार्थ कभी असत् नहीं होता। इस प्रकार द्रव्यतः नित्य होने पर गौतम-! जीव कभी कम और कभी अधिक नहीं होते किन्तु अवस्थित भी जीव पर्यायतः अनित्य है, क्योंकि पर्याय की दृष्टि से वह सदा रहते हैं, अर्थात् जीव संख्या की दृष्टि से सदा अनन्त रहते हैं। अनन्त परिवर्तनशील है। जीव विविध गतियों में, विभिन्न अवस्थाओं में होने पर भी सभी आत्माएं चेतन और असंख्यात प्रदेशी हैं, अत: परिणत होता रहता है।
एक हैं। क्षेत्र की दृष्टि से जीव लोकपरिमित हैं जहाँ लोक है वहाँ जीव जैसे सोने के कुण्डल, मुकुट, हार आदि अनेक आभूषण है। जहाँ तक जीव है वहाँ तक लोक है। बनने पर भी नाम और रूप में अन्तर पड़ जाने पर भी सोना-सोना आत्मा अच्छेद्य है, अभेद्य है, उसे अग्नि जला नहीं सकती, ही रहता है, वैसे ही विध योनियों में भ्रमण करते हुए जीव के पर्याय शस्त्र काट नहीं सकता। जीव कदापि विलय को प्राप्त नहीं होता। यह बदलते हैं- रूप और नाम बदलते हैं- मगर जीव द्रव्य वही रहता है। एक परखा हुआ सिद्धान्त है कि अस्तित्व अस्तित्व में परिणमन
जीवन में सुख और दुःख किस कारण से पैदा होते हैं? करता है और नास्तित्व नासितत्व में। द्रव्य से अस्तित्ववान् जीव इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् महावीर ने कहा-आत्मा ही भविष्य में नास्तित्व में परिणमन नहीं कर सकता। अपने सुख और दुःख का कर्ता है और भोक्ता है। आत्मा ही अपने जैसे दूध और पानी बहिर्दष्टि से एक प्रतीत होते हैं वैसे कृत कर्मों के अनुसार विविध गतियों में परिभ्रमण करता है और ही संसारी दशा में जीव और शरीर एक लगते हैं, पर वे पृथकअपने ही पुरुषार्थ से कर्म-परम्परा का उच्छेद कर सिद्ध, बुद्ध और पृथक् हैं। मुक्त बनता है।
वादिदेवसूरि ने संक्षेप में सांसारिक आत्मा का स्वरूप इस जैसाकि पहले कहा जा चुका है, आत्मा का कोई आकार प्रकार बताया है- “आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है। वह चैतन्य नहीं है, किन्तु सकर्मक आत्मा किसी न किसी शरीर के साथ ही स्वरूप हैं, परिणामी है, कर्मों का कर्ता हैं। सुख-दुःख का साक्षात् रहती है, अतएव प्राप्त शरीर का आकर ही उसका आकार हो जाता भोक्ता है, स्वदेहपरिमाण है, प्रत्येक शरीर में भिन्न है, पैगलिक कर्मों है। इस कारण जैन दर्शन में आत्मा को कायपरिमित माना गया हैं। से युक्त है।'' प्रस्तुत परिभाषा में जैन दर्शन-सम्मत आत्मा का आत्मा स्वभावत: असंख्यात प्रदेशी है और उसके प्रदेश संकोच- पूर्णरूप आ गया है। विकासशील होते हैं। अतएव कर्मोदय के अनुसार जो शरीर उसे
आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व की सिद्धि के लिए श्री जिनभद्र प्राप्त होता है, उसी में उसके समस्त प्रदेशों का समावेश हो जाता है। ने विशेषावश्यक भाष्य में विस्तार से अन्य दार्शनिकों के तर्कों का
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org